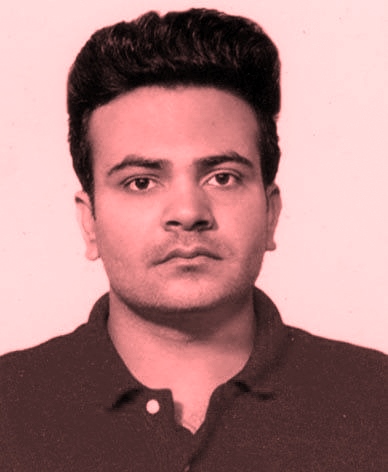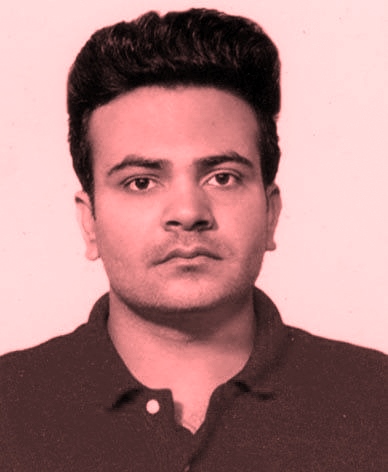
शोधार्थी। पीएच.डी. (हिंदी), दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। कुछ पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएँ आदि प्रकाशित। आई.सी.एस.एस. आर. डॉक्टर फेलो २०२३।
मनुष्य की विकास-यात्रा में स्त्री का संघर्ष शुरुआत से ही समाज में अवस्थित रहा है। देशकाल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप इस संघर्ष का केवल बाहरी रूप बदलता रहा है, जबकि आंतरिक स्तर पर यह संघर्ष अपने अस्तित्व व अधिकार के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। आदिम युग से लेकर वर्तमान युग तक स्त्री किसी-न-किसी रूप में उपेक्षित ही रही है। कभी रीति-रिवाज के नाम पर, कभी भावनात्मक एकता के नाम पर, कभी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण तो कभी केवल उपभोग की वस्तु समझे जाने के कारण। स्त्री को सदैव हर पग पर शोषण का शिकार होना पड़ा है। इस संघर्ष की परंपरा अति-दीर्घ है, जो अपने निजी संघर्षों की करुण कहानी को बुनती है। स्त्री का यह संघर्ष केवल बाह्य समाज के कारण ही नहीं अपितु पारिवारिक व निजी भी होता है। इस संबंध में सिमोन द बउआर ने अपनी पुस्तक ‘द सेकंड सेक्स’ में लिखा है कि ‘स्त्री पैदा नहीं होती, उसे बना दिया जाता है।’
सिमोन द बउवार का यह कथन किसी विशिष्ट समुदाय की स्त्री को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की स्त्रियों के संघर्ष को बयाँ करता है। भारतीय समाज में स्त्री को कभी दासी तो कभी वस्तु के रूप में देखा जाता है। स्त्री मुक्ति का संघर्ष इसी बंधन एवं मानसिकता को तोड़कर समाज में समानता का अधिकार चाहता है, जिसके संबंध में रेखा कास्तकार ने लिखा है—“स्त्री विमर्श का सरोकार जीवन और साहित्य में स्त्री मुक्ति के प्रयासों से है। स्त्री की स्थिति की पड़ताल उसके संघर्ष एवं उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ-साथ बदलते सामजिक संदर्भों में उसकी भूमिका, तलाशे गए रास्तों के कारण जनमे नए प्रश्नों के टकराने के साथ-साथ आज भी स्त्री की मुक्ति का मूल उसके मनुष्य के रूप में स्वीकारे जाने का प्रश्न है।”
स्त्रियों की मानवीय चेतना को तलाश करते हुए प्रभा खेतान ने लिखा है—“हम भारतीय कई तहों में जीते हैं। यदि हम मन की सलवटों को समझते हैं, तो जरूर यह स्वीकारेंगे कि औरत का मानवीय रूप सहोदरा कही जाने के बावजूद स्वीकृत नहीं है। लोगों को उससे उम्मीदें बहुत होती हैं। वह अपनी सारी भूमिकाओं को बिना किसी शिकायत के निभाए...स्पष्टवादिता उसका गुनाह समझा जाता है।”
साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से उन व्यक्तिगत अनुभव और कल्पना को नया रूप देता है, जो समाज का प्रतिबिंब होती है। एक रचनाकार का हृदय कोमल होता है और वह सामाजिक परिस्थितियों से अतिशीघ्र प्रभावित होता है। परिवेशगत अनुभूतियाँ ही एक रचनाकार संवेदनशीलता प्रदान करती है। यद्यपि समकालीन साहित्य की लगभग हर विधा स्त्री संघर्ष की चुनातियों को स्वर प्रदान करने लगी है, लेकिन फिर भी स्त्री का संघर्ष किसी से बराबरी न करके केवल अपनी अस्मिता की तलाश के लिए है।
अस्मिता शब्द अपने में अत्यंत व्यापक अर्थ ग्रहण किए हुए है, जो व्यक्ति की पहचान को एक नए धरातल पर प्रस्तुत करता है। इस शब्द को परिभाषित करते हुए डॉ. सुरेशचंद्र गुप्त लिखते हैं—“अस्मिता को परिभाषित करना कठिन है, फिर भी ‘मैं हूँ’ से लेकर ‘मैं किस लिए हूँ’ तक की अंतर्यात्रा कई पड़ावों से होकर अंततः अस्मिता के गंतव्य पर पहुँचकर ही पूरी होती है।”
सही अर्थों में कहा जाए तो स्त्री अस्मिता स्त्री की उस पहचान को स्थापित करने का कार्य करता है, जो परंपरा से हो रहे स्त्री-संघर्ष की परत-दर-परत को अनुभव करता है। स्त्री विमर्श यही स्थापित करना चाहता है कि वह भी पुरुषों के समान समाज और प्रकृति का हिस्सा है। वह अपनी पहचान के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि अधिकारों को प्राप्त करना चाहती है। यह संघर्ष केवल देह का नहीं, बल्कि रूढ़ हो चुकी मान्यताओं, परंपराओं और मानसिक विषमताओं के विरुद्ध मुक्ति का स्वर है।
कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आरंभ में स्त्री रचनाकारों ने उपदेश-प्रधान साहित्य को आधार बनाया। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने नारी संघर्ष को तो उजागर किया, लेकिन इसे रोकने के लिए वह क्रांतिकारी कदम उठाने में अक्षम महसूस कर रही थी। यही कारण है कि आरंभ में महिलाओं ने समाज-सुधार आंदोलन से जुड़कर स्वयं को आधार प्रदान किया और बाद में अपने संघर्ष का एक निश्चित पथ तैयार किया। डॉ. रस्तोगी का मानना है कि “साहित्य के विकास में नारी का योग उसके भावनात्मक जगत् के अस्तित्व की कहानी है।”
स्त्री-मुक्ति के इस पथ को बाद की महिला रचनाकारों ने अधिक प्रभावशाली आधार प्रदान किया और स्त्री विमर्श के नए आयामों को प्रस्तुत किया। पहले वह सबकुछ सहती थीं, लेकिन अब उसने आवाज उठाना सीखा और अपने अधिकारों को न्यायसंगत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही चरणगत विकास महिला लेखन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए सुदर्शन लिखते हैं—“आज की शिक्षित नारी की प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका है, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, कला, कविता, साहित्य-सृजन, पर्वतारोहण, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहाँ नारी ने प्रवेश न किया हो।”
समकालीन लेखिकाओं में कृष्णा सोबती, चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, जिन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, विद्रूपताओं, भेदभाव आदि को अपने साहित्य का माध्यम बनाया तथा समाज की अन्य स्त्रियों को आगे आने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान समय में मृदुला सिन्हा भी उन महिला रचनाकारों में से एक मानी जाती है, जिन्होंने अपने उपन्यासों व कथा साहित्य के माध्यम से स्त्री मुक्ति के प्रश्न को सायास प्रस्तुत किया है। हालाँकि वे अपने साहित्य में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर नहीं, अपितु उनसे श्रेष्ठ मानती है।
मृदुला सिन्हा उस रचनाधर्मिता की प्रतीक हैं, जो अपने गाँव, देश की माटी से जुड़कर अपनी सृजनात्मकता के बीज पल्लवित पोषित करती हैं। अपने जीवन और सृजन को माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से जोड़कर विविध आयाम देती हैं। समाज, साहित्य और राजनीति तीनों क्षेत्रों से अनायास जुड़कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा और चिंतन-शैली से भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार और लोक विश्वासों को जन-जन तक पहुँचाती हैं। वे अपनी जीवन-यात्रा के पड़ावों को एक ओर साहित्यिक सृजन में ढालती हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी से करती हैं।
असल में व्यक्तित्व और कृतित्व (सृजन) का संबंध परस्पर पूरक और अन्योन्याश्रित होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यक्ति की संवेदना, भाव उसके स्वभावगत संस्कार-विशेषताएँ, परिवेशगत जीवन अनुभव, किसी प्रसंग से उसके मन-मस्तिष्क पर पड़ने वाली क्रिया-प्रक्रियाएँ आदि समाहित रहती हैं। एक साहित्यकार या रचना के कृतित्व या सृजन का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने हेतु उसके व्यक्तित्व से अवगत होना समीचीन होता है। डॉ. नगेंद्र की मान्यता है कि “मैं यह मानता हूँ कि प्रत्येक साहित्यिक कृति का संबंध कृतिकार के व्यक्तित्व से है। कृतिकार का अपना रागात्मक जीवन और उसके आधार पर निर्मित जीवन दर्शन कृति में अनिवार्यतः प्रतिफलित-प्रदर्शित होता है। यह प्रतिफलन प्रत्यक्ष हो यह आवश्यक नहीं है। प्राय: यह अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न ही होता है।”
मृदुलाजी का समकालीन समय में भारत के गाँवों, विशेषकर बिहार के गाँवों से जुड़कर साहित्य रचना करना इनकी एक अलग और न्यारी विशेषता है। वे कहती भी हैं—“मैं लोकगीतों, लोकोक्तियों, लोक-कहावतों में ही सोचती हूँ। मानव मन, उसकी विशेषताओं, हास-परिहास, संस्कार और व्यथा को समझने के लिए लोक-साहित्य के ही पन्ने पलटती हैं।”
मृदुलाजी के लेखन के प्रति भाव तो मन में गहरे समाए हुए थे ही, पर वे जागरूक हुए अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूकता और अपने पति की सकारात्मकता भाव दृष्टिकोण से। अपनी शादी के बाद उन्होंने पहली कहानी लिखी—‘भ्रम की व्यथा’। इसी कहानी के जरिए उनका पदार्पण होता है, हिंदी के साहित्यिक जगत् में। अगस्त २०१५ में डी.डी. न्यूज पर उनके ‘तेजस्विनी’ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनकी इस साहित्य सृजना के पीछे प्रेरणास्रोत कौन हैं तो उन्होंने कहा कि “मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल का मुँह दिखाया और अपने पति के सहयोग-समर्थन और प्रेरणा से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ।”
एक पौराणिक और जागरूक आधुनिक भारतीय नारी की दृष्टि से इन्होंने आज की महिलाओं के पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के समसामयिक जटिल प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक मंथन किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके नारी चिंतन में पौराणिक और आधुनिक नारी चिंतन का गठजोड़ विद्यमान है। तभी तो इन्होंने ‘हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी है’ जैसे उत्तेजक एवं संघर्षशील नारों को संशोधित कर ‘हम भारत की नारी हैं, फूल और चिनगारी हैं’ के रूप में आम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अर्थात् नारी फूल सदृश्य कोमल तो होती है; परंतु दुर्बल नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्मीबाई का रूप भी धारण कर सकती है।
इस प्रकार मृदुलाजी अपनी पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह में हुए अनुभवों के संचित कोश द्वारा साहित्य को नई दृष्टि और दिशा दे रही हैं। इनका चिंतन अनजानी भावुकता, छद्म बौद्धिकता और कोरी कल्पना से दूर हटकर अनुभवजन्य सत्य के आधार पर निर्मित है, वहीं आज इनका उदीयमान व्यक्तित्व स्वयं को और दूसरों को दुनिया की धारा में बहने की बजाय उसे सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील और सृजनरत है। इस दृष्टि से मृदुलाजी के व्यक्तित्व मूल्यपरक होना भारतीय परंपरा में दृढ़ विश्वास को जताता है। वे अपनी शक्ति और समृद्ध पुरानी नींव को नए निर्माण से जोड़कर राष्ट्र निर्माण की बात कहती हैं।
मृदुला सिन्हा लोकधर्मी साहित्यकार हैं। वे लोकचेतना में संपृक्त होकर लेखन कार्य करती हैं। उनकी लेखनी ने आधुनिक हिंदी कथा संसार में एक नया स्तंभ स्थापित किया है। विशेषकर महिला कथा लेखन को एक दिशा-बोध प्रदान करने का प्रयास किया है। उनके उपन्यास साहित्य की दृष्टि डाले तो यह बात बेहतर तरीके से स्पष्ट की जा सकती है कि मृदुलाजी की उपन्यास सर्जन-यात्रा स्वानुभूति से प्रारंभ होकर लोकानुभूति तक जाती है।
महिला कथा-लेखन परंपरा में मृदुला सिन्हा पौराणिक स्त्री पात्रों के आत्मकथात्मक उपन्यास सृजित कर स्त्री विमर्श का भारतीय चिंतन प्रस्तुत किया है। सीता माँ की आत्मकथा के रूप में ‘सीता पुनि बोली’, सती सावित्री की आत्मकथा के रूप में ‘विजयिनी’ और मंदोदरी की आत्मकथा के रूप में ‘परितप्त लंकेश्वरी’ लिखकर मृदुलाजी ने पौराणिक स्त्री पात्रों से आधुनिक भारतीय नारी को संबल प्रदान करने का अनुकरणीय प्रयास किया है।
१. ‘ज्यों मेहँदी को रंग’, मुदुला सिन्हा का पहला उपन्यास विकलांगों के जीवन पर आधारित है। इसमें विकलांगों के प्रति समाज और सामाजिक संस्थाओं का नजरिया वास्तविकता के साथ चित्रित किया गया है।
२. ‘घरवास’ १९९२ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लोकार्पित उपन्यास बिहार के एक गाँव के घात-प्रतिघात, उत्थान-पतन, सामाजिक व राजनीतिक उथल-पुथल पर आधारित बिहार के गाँव में एकता के बीज ढूँढ़ता है। इस उपन्यास में बिहार से बाहर पंजाब गए मजदूरों के जीवन में आए परिवर्तन और उस परिवर्तन को गाँव द्वारा स्वीकार्य को बड़ी सजीवता के साथ उकेरा गया है।
३. ‘अतिशय’ भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, ऐसी ही स्थितियों को बड़े प्रभावी ढंग से उकेरा गया है इस उपन्यास में। इसमें तीन पीढ़ियों की आर्थिक, पारिवारिक संघर्ष की कहानी को रचा-बुना गया है। एक प्रकार से यह रचना वर्तमान परिवेश की विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उठाती है और उनका समाधान भी ढूँढ़ती है, जिसमें भोग की जगह संयम को स्थापित किया गया है। औद्योगिककरण एवं सूचना क्रांति के बंद होने की कगार पर खड़े वस्त्र उद्योगों को पुनर्जीवन प्रदान करने की कहानी को प्रस्तुत करता है यह उपन्यास।
४. ‘सीता पुनि बोली’ रामायण की ‘रामकथा’ को आधार बनाकर आत्मकथा शैली में सीतामाता के मन के भावों को अपनी भाषा से शब्दबद्ध करता ‘सीता पुनि बोली’ उपन्यास अत्यंत मार्मिक, कारुणिक एवं हृदयस्पर्शी बन पड़ा है। इसमें सीता माँ के ‘मन’ की थाह ली गई है, सीता माँ से जुड़े सभी प्रश्नों को उठाया गया है, नारी की आत्मिक शक्ति के साथ मातृत्व की प्रतिष्ठा की गई है, भारतीय नारी की आचरणशीलता और पतिव्रता धर्म को सीता माँ के शक्ति संपन्ना रूप के साथ संजोया गया है। सीता के अंतर्मन में उमड़-घुमड़ कई अनुत्तरित प्रश्नों को मृदुला सिन्हा ने लोकमन के साथ उठाया है—उनका हल भी ढूँढ़ा है, स्वयं- सीता माँ की पीड़ा में डुबकी लगाकर, सीता माँ की ‘आत्मकथा' लिखकर। इस आत्मकथा में हमारे सनातन भारतीय जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा स्थापित हुई है। भारतीय संस्कारशीलता की कहानी आस्थावादी और जीवन-मूल्यपरक दृष्टि लिए प्रस्तुत हुई है।
५. ‘विजयिनी’ उपन्यास सती सावित्री की आत्मकथा के रूप में है, जिसमें आधुनिक भारतीय नारियों के लिए आत्मसंबल खोजने की कोशिश की गई है। भारतीय नारी का आत्मस्वाभिमान, आत्मनिर्णय, स्वावलंबन, अस्मिता की पहचान आदि बिंदुओं को इस उपन्यास के द्वारा उकेरा गया है।
भारतीय नारी का आदर्श कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप लिखा गया है विजयिनी उपन्यास। लेखिका ने इसकी भूमिका में कहा है कि “सावित्री हमारा इतिहास है। भारतीय नारी की तेजस्विता का इतिहास। नारी विकास की दशा निर्धारण के समय तो और भी आवश्यक है, सावित्री की निर्णय-स्वतंत्रता के पहलुओं को जानना, समझना और आत्मसात् करना।”
६. ‘परितप्त लंकेश्वरी’ एक ऐतिहासिक कथा की सशक्त महिला पात्र मंदोदरी की वीरता, विद्वत्ता और व्यावहारिकता आधारित जीवन के संघर्ष को उकेरकर आज जल, थल, नभ पर कदम रखती युवतियों के लिए आदर्श गढ़ती संवेदनशील लेखनी का प्रयास है—‘परितप्त लंकेश्वरी’।
७. ‘अहल्या उवाच’ उपन्यास मिथकीय कथा के माध्यम से आधुनिक भारत की नारी के संघर्ष को दरशाता है। उपन्यास में दांपत्य जीवन में आने वाले दबावों और उनके कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को बहुत ही सहजता से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में यह समस्या प्रासंगिक बनी हुई है, जिसमें परिवार छोटे होते जा रहे हैं और पति-पत्नी के रिश्तों में दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं को उपन्यास में मिथकीय कथा के माध्यम से दरशाया गया है। यही कारण है कि प्रो. कुमुद शर्मा ने इस उपन्यास को ‘दांपत्य जीवन की पाठशाला’ कहा है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मृदुला सिन्हा उस रचनाधर्मिता की प्रतीक हैं, जो अपने गाँव, देश की माटी से जुड़कर अपनी सृजनात्मकता के बीज पल्लवित पोषित करती है। अपने जीवन और सृजन को माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से जोड़कर विविध आयाम देती है। समाज, साहित्य और राजनीति तीनों क्षेत्रों से अनायास जुड़कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा और चिंतन शैली से भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार और लोकविश्वासों को जन-जन तक पहुँचाती हैं। वे अपनी जीवन-यात्रा के पड़ावों को एक ओर साहित्यिक सृजन में ढालती हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी करती रही हैं।
बी-४३, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट,
यूनिवर्सिटी एन्क्लेव, दिल्ली-११०००७
दूरभाष : ९५६०५४६४७४