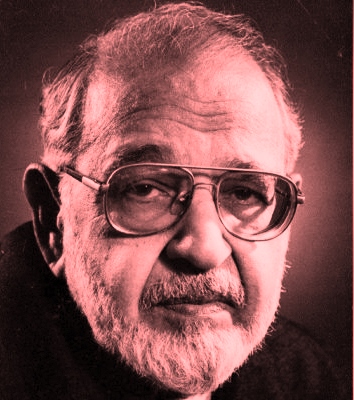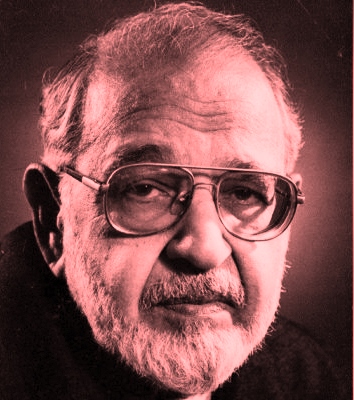
हिंदी के सुपरिचित कवि, आलोचक एवं भाषाविद्। शब्द सक्रिय हैं (कविता-संग्रह), खुली हथेली और तुलसीगंध (संस्मरण) व कविता का स्थापत्य, कविता की अष्टाध्यायी एवं शब्दों से गपशप सहित समीक्षा व आलोचना की कई पुस्तकें। कई ख्यात कवियों की कृतियों का संपादन। तत्सम, शब्दकोश के सहयोगी संपादक एवं बैंकिंग वाङ्मय सीरीज (पाँच खंड) के रचयिता। उ.प्र. हिंदी संस्थान से ‘आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार’ सहित अन्य सम्मानों से विभूषित।
ज्ञेय साहित्यिक प्रतिभा के शिखर पुरुष थे। हिंदी की एक बड़ी विभूति, जिसने हिंदी को आत्मगौरव दिया, नए शिल्प और नए प्रयोगों से उसे जोड़ा। ‘तारसप्तक’ के प्रकाशन से हिंदी में प्रयोगवाद के जनक कहलाए। अनेक विधाओं में श्रेष्ठ रचनाओं का उपहार हिंदी समाज को दिया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं, हिंदी के सुधी कवि-समालोचक डॉ. ओम निश्चल।
अज्ञेय की प्रतिभा का कहना क्या! उनसे मेरी मुलाकातें थीं। उन्होंने अपनी कविताओं, उपन्यासों, कहानियों, यायावरी के वृत्तांतों, निबंधों से एक अलग दुनिया रची। उनका वैदुष्य अप्रतिम था, उनकी शख्सियत में एक सम्मोहन था, जिसमें अव्यक्त उदात्तता थी। उनके जीवन, उनके कामकाज में एक सलीका था—शिष्टता की एक अनूठी आभा, जिसके प्रभामंडल में शब्द विश्रांति का अनुभव करते थे। हिंदी रचनाशीलता की एक बड़ी सत्ता के रूप में अज्ञेय को याद करना आज भी प्रसन्नता और गर्व से भर देता है। वे जितना भीतर-भीतर बंद रहने वाले इनसान थे, उतना ही अपनी रचनाओं में भरे-भरे। उनकी पैदाइश पुरातात्त्विक उत्खनन के शिविर में हुई तो बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनारा में उनका बचपन बीता। पिता के साथ अनेक उत्खनन स्थलों पर उनका प्रवास होता रहा। जिसका बचपन ही बुद्ध की ऐसी स्मृति-छाया में गुजरा हो, वह आगे चलकर ऐसी ही प्रतिभा से निमज्जित क्यों न होता। अज्ञेय धीरे-धीरे प्रबुद्ध और बुद्ध होते गए। ऐसे अज्ञेय जब एक बार वत्सल निधि शिविर के बहाने लखनऊ आए तो मिलने का बानक बहुत विलक्षण तरीके से बना। गँवई गाँव से आया हुआ मैं, उन दिनों यों तो सूचना विभाग की पत्रिका ‘उत्तर प्रदेश’ मासिक से संबद्ध था, पर वह गँवई आभा मेरे भीतर थी, जो संकोच की मारी थी। किसी लेखक से मिलना और उससे बातचीत करना अनेक प्रासंगिक सवालों के साथ यह संकोच से भरने वाला था। लेकिन उनके व्यक्तित्व की दुंदुभि ऐसी थी कि मिलने का रोमांच उत्तरोत्तर गहराता रहा।
वे उन दिनों लखनऊ आए थे वत्सल निधि शिविर के एक आयोजन में, जो कृष्णानगर, आलमबाग में साक्षरता निकेतन में आयोजित था। मुझे पता था कि उन्होंने कुछ साल पहले ही एक उपक्रम ‘वत्सल निधि’ गठित किया है, जिसकी गोष्ठियाँ वे लेखकों-कवियों के मध्य सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थलों पर किया करते हैं। देश के जाने-माने व युवा लेखक सभी इन गोष्ठियों में आते हैं। चर्चाएँ होती हैं। काव्यपाठ आदि होता है। शुद्ध साहित्यिक आयोजन की सुगंध ऐसे ही कार्यक्रमों में होती है। उन दिनों साक्षरता निकेतन के निदेशक थे, भगवतीशरण मिश्र। वे सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशक रह चुके थे। आई.ए.एस. थे। स्वयं लेखक भी थे। अज्ञेय के लिए उनके मन में बहुत स्नेह था। साक्षरता निकेतन इससे पहले जा चुका था। कभी यहाँ बच्चों के सुप्रसिद्ध कवि द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरीजी निदेशक हुआ करते थे। उपशिक्षा निदेशक पद से सेवानिवृत्ति के बाद वे साक्षरता की इस महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था में नियुक्त हुए थे। सच कहें तो साक्षरता, बाल शिक्षण, प्रौढ़ शिक्षण इन सब में द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी की दक्षता थी। वे माध्यमिक शिक्षा परिषद् में लंबे अरसे तक रहे थे, पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य रह चुके थे। उन्हें शिक्षा विभाग में काम करने का सुदीर्घ अनुभव था। उसी जगह पर उन दिनों भगवतीशरण सिंह थे। सुपरिचित लेखक। अत: स्पष्ट था कि अज्ञेय को एक ऐसा वातावरण स्वत: ही उपलब्ध हो गया था, जहाँ लखनऊ के बाहरी सुरम्य वातावरण में लेखक आ सकें, बातचीत कर सकें, ठहर सकें। अज्ञेय का वत्सल निधि उपक्रम उन दिनों चर्चा में रहा करता था।
वत्सल निधि क्या है, यह अज्ञेय को जानने के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि भारतीय ज्ञानपीठ से उन्हें जो पुरस्कार मिला था, उसमें कुछ निधि अपनी मिलाकर उन्होंने १९८० में ‘वत्सल निधि’ की स्थापना की थी, जिसका एक लक्ष्य रखा गया कि भारत के सांस्कृतिक महत्त्व के स्थलों पर वत्सल निधि के शिविर आयोजित किए जाएँ, जहाँ हिंदी के वरेण्य और कुछ युवा कवि, कथाकार, लेखक, आलोचक शामिल हो सकें और साहित्य पर महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ हो सकें। वत्सल निधि के लेखकीय शिविर प्राय: रमणीय स्थलों पर आयोजित होते। लखनऊ, बोधगया, बरगी नगर, नर्मदा तट जैसी जगहों पर हुए शिविर आज भी लोगों के ध्यान में हैं। वे आज के अर्थों में साहित्य महोत्सव कहे जा सकते हैं, जो आज लकदक सभागारों में हुआ करते हैं, पर अज्ञेय ने अपने शिविर को कुदरत के साहचर्य से जोड़ा था। वे प्रकृति के सुकुमार पर्यवेक्षक थे। हर शिविर में साहित्य का कोई-न-कोई बहसतलब विषय हुआ करता था। सर्जन और संप्रेषण, साहित्य का परिवेश, साहित्य और समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया, सामाजिक यथार्थ और कथाभाषा तथा समकालीन कविता में छंद आदि विषयों पर उन्होंने गोष्ठियाँ आयोजित कीं। ऐसी पहली गोष्ठी उन्होंने साक्षरता निकेतन के सहयोग से लखनऊ में साक्षरता निकेतन के परिसर में रखी, जो लखनऊ से दूर एक प्राकृतिक वातावरण में है। इन गोष्ठियों में बीस-पच्चीस युवा लेखक आमंत्रित होते थे। युवाओं पर अधिक बल रहता था अज्ञेय का, जो वरिष्ठ लेखकों के सान्निध्य में लेखन के सांप्रतिक विषयों पर बेबाक बातचीत कर सकें। अपने पर्चे पढ़ सकें। वत्सल निधि द्वारा समय-समय पर लेखक शिविर, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ, परिसंवाद, सभाएँ, संदर्भ सामग्री और दस्तावेजों का संग्रह आदि गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित होती रहीं। इसके अलावा अज्ञेय द्वारा दो व्याख्यान-मालाएँ भी वत्सल निधि द्वारा संचालित होती रहीं—राय कृष्णदास व्याख्यान माला और हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला। पर दुर्भाग्य है कि आज वत्सल निधि को कोई सक्षम व्यक्ति चलाने वाला नहीं है।
ऐसे अज्ञेय, जिनकी उस जमाने में तूती बोल रही थी, से कैसे मिला जाए, यह समस्या थी। १९८१ के वे जाड़े के दिन थे। कोहरे में डूबी सुबहें और हम फिदाए लखनऊ का झीना-झीना वातावरण। उनसे मुलाकात की चर्चा मैंने अपने मित्र चंद्रपाल सिंह से की, जो उस समय शायद दैनिक जागरण में कार्यरत थे या उससे संबद्ध थे। उन्हें यह प्रस्ताव अच्छा लगा, पर समस्या यह थी कि उनसे पूछने के लिए कुछ सवाल हमारे पास चाहिए। दूसरे यह कि हमारे पास उनसे मुलाकात का पूर्व अपॉइंटमेंट तो था नहीं। वे उपलब्ध न हुए तो क्या होगा। बहरहाल हम पुस्तकालयों के नियमित विजिटर थे। उनकी बहुत सी पुस्तकें जुटाईं तथा उनसे पूछे जाने वाले सवाल भी। उन दिनों अज्ञेय का बहुत विरोध था। वामपंथियों में उन्हें लेकर एक चिढ़-सी थी, जो आज भी है। सो हम लोग भी उन बातों से एक हद तक परिचालित थे। हमें अज्ञेय का व्यक्तित्व तो प्रिय था, पर हम ऐसे सवालों से बच न सके, जो उन्हें असुविधाजनक जान पड़ते। बहरहाल सवाल बन गए। किताबें जुट गईं। पर बातचीत को रिकाॅर्ड कैसे किया जाए, यह समस्या थी। हम दोनों इस मामले में विपन्न थे। हमारे पास तो ढंग का कलम तक न होता था, टेप रिकाॅर्डर कहाँ से आता और किसी लेखक से इमला शैली में बातचीत करना हमें अशोभन व समयलेवा भी जान पड़ता था, सो टेप रिकॉर्डर की खोज शुरू हुई। संयोग से चंद्रपाल सिंह यानी सी.पी. सिंह एक रिसोर्स पर्सन भी थे। पत्रकारिता में होने के कारण निर्भीक भी थे, पढ़ाकू थे, अध्यापकों के प्रिय थे, सो उन्होंने तत्कालीन प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा से संपर्क किया। उन्होंने अपना रिकॉर्डर सी.पी. को दिया तथा हम लोग उसे चलाना सीख बैटरी आदि की व्यवस्था कर बातचीत के लिए प्रस्तुत हो गए।
और एक दिन शाम को लगभग तीन बजे हम साक्षरता निकेतन की ओर चल पड़े। हम दोनों के पास साइकिल ही थी। किताबें कॅरियर पर दाबे, झोले में टेप रिकॉर्डर टाँगे और मन में अज्ञेय से बातचीत का हौसला लिए हम एक घंटे में कृष्णानगर पहुँच गए। साक्षरता निकेतन रोड पर ही है। उसी से कुछ आगे। वहाँ पहुँचकर इस शिविर के बारे में जानकारी की तथा किसी व्यक्ति से पूछा कि अज्ञेयजी कहाँ ठहरे हैं। हम थोड़ी देर में उनके कमरे के बाहर पहुँच गए। आहिस्ता घंटी बजाने पर एक स्त्री ने दरवाजा खोला। सुदर्शना। मुझे याद हो आई उनकी कविता—‘अमराई महक उठी हिय की गहराई में, पहचानें लहक उठीं तितली के पंख खुले, यादों के देवल के उढ़के दो द्वार खुले।’ द्वार खोलने वाली इला डालमिया थीं, जो अज्ञेय की सहचरी कही जाती थीं। उनके बारे में हमें कुछ पता भी था कि वे अपनी किसी मित्र के साथ रहते हैं। उन्होंने उस सुइट के आगे वाले रूम में आत्मीयता से बिठाया और भीतर जाकर अज्ञेयजी को जानकारी दी। तब तक हम टेबल पर टेप रिकॉर्डर रख चुके थे। थोड़ी देर में दुग्धधवल कुरते-पायजामे में अज्ञेयजी कमरे के बाहर आए। देखा, हम दो युवा लगभग २० साल के उनकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। उनकी कुछ पुस्तकें टेबल पर रख दी थीं व कुछ चंद्रपाल व मेरे हाथ में थीं। हमें देखकर ही मालूम हो सकता था कि हम अदब के दीवाने हैं, अज्ञेय के दीवाने हैं तथा उनसे मिलने की अपार उत्कंठा से भरे हैं। अज्ञेय ने बाँकी स्मिति के साथ पूछा, बोलिए। हमने अपना उद्देश्य बताया तो वे असमंजस में पड़ गए। वे लोग थोड़ी ही देर में लेखकों के साथ नगर दर्शन के लिए निकलने वाले थे। लेकिन हमें देखकर अज्ञेयजी थोड़ा सदय हुए तथा नगर दर्शन के व्यवस्थापक को कहलवाया कि मैं लेखकों के साथ नगर दर्शन के लिए न जा सकूँगा। दो लड़के बातचीत के लिए आए हैं। ये जरूरी जान पड़ते हैं। इला डालमिया को कहा कि वे चली जाएँ। हम यहीं रहेंगे। इनसे बातचीत करेंगे। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में परिसर में बस वे थे और हम थे।
इस तरह हम थोड़ी ही देर में उनके सम्मुख थे। एक तेजस्विता हमारे मासूम चेहरे निहार रही थी कि ये युवा भला क्या पूछेंगे। हमने प्रश्नों की काॅपी दिखा दी। वे बोले, कैसे लिख सकोगे। हमने कहा, रिकॉर्डर पास है, जिससे सुविधा होगी। हम बाद में ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे। मेरा उनके गीतों से बड़ा लगाव रहा है। उनकी भाषा में जहाँ अभिजात गुण झलकते हैं, वहीं गँवईगाँव के कुदरत के अनेक देशज बिंब भी आ धमकते हैं कि वे सप्रयोजन ले आते हैं, यह नहीं पता, पर वे भले लगते हैं। वे भाषा के ठाठ को संवेद्य और स्मरणीय बना देते हैं। लिहाजा उनका एक पुराना गीत मेरे ध्यान में कहीं अटका था। पहुँच क्या तुम तक सकेंगे, काँपते ये गीत मेरे, दूरवासी मीत मेरे। यहीं से शुरू किया और कई सवाल पूछे, जो कविता पर कविता की संप्रेषणीयता को छूते हुए थे। उन्हें व्यक्तिवादी वैशिष्ट्य का कवि मानकर नेपथ्य में डालने की बहुतेरी कोशिशें हुईं, पर उनकी कविता इस एक विशेषण में बाँधी न जा सकती थी। उनका यायावर मन भारतीय संस्कृति और चिंतन के अनेक आयामों से टकराता हुआ लगता था।
अज्ञेय का प्रभामंडल विराट् था। वे काल और समय की अखंडता पर भी बोल सकते थे और साहित्य की जनवादी सीमाओं पर भी। सामाजिक यथार्थ और कथाभाषा, संप्रेषणीयता, छंद और कविता, श्रुति की ओर लौटती कविता, कविता के वाचिक संप्रेषण, नई कविता में छंद के अभिनव प्रयोगों तथा कविता में छंद की सार्थकता पर वे बहुधा विचार कर चुके थे। जितना उनका सम्मान हिंदी साहित्य में था, उतना उनका विरोध भी हुआ करता था। कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम से सहबद्ध होने के कारण उन्हें वामपंथियों की निंदा भी सहनी पड़ी। कहा जाता है, इसे सी.आई.ए. की फंडिंग उपलब्ध थी। किंतु अज्ञेय अपने मौन की कारा में बंद एक ऐसे लेखक थे, जो बहुत जरूरत होने पर ही बोलते थे। उनका लेखन, संपादन और व्यक्तित्व सब व्यवस्थित था। उनका पांडुलिपि तैयार करने का ढंग बेहतरीन था। वे ही थे, जिन्होंने कभी कंटेंट्स के लिए अनुक्रम नहीं लिखा। कभी निबंध क्रम, कभी कविता क्रम, कभी क्रमसूची यही दिया। क्योंकि कंटेंट्स का अनुवाद अनुक्रम हो ही नहीं सकता। वह तो अपेंडिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जो बाद में आता है, पहले नहीं। और पहले नहीं आता तो अनुक्रम कैसे हो जाएगा। हिंदी में कुछ लेखकों को छोड़कर यह इल्म बहुधा कम लोगों को होगा।
इस तरह अज्ञेय अपनी भाषा, अपने भाषाई व्यवहार में इतने चुस्त-दुरुस्त थे। पर यह जानते हुए भी सबकुछ हमारे लिए अनजाना सा था। अज्ञेय का ऊपर-ऊपर दिखने वाला व्यक्तित्व जितना मोहक था, क्या पता वे भीतर से वैसे न निकले तो। किसी बात के लिए डाँट दिया तो। पर हम अपनी मासूमियत में सौ प्रतिशत ईमानदार थे। अज्ञेय-अज्ञेय थे, तभी तो हम उन्हें जानने निकले थे, कुछ मुट्ठीभर सवालों के साथ। चंद्रपाल हमारे साथ थे ही। वे भी बहुत शार्प थे। अनुवाद उनका बहुत मँजा हुआ करता था। जब मैं पत्रकारिता के उपाधि के लिए अपना शोध-पत्र (Pressures on the Press) हिंदी में तैयार कर रहा था, उन्होंने चंचल सरकार की पुस्तक ‘द चेंजिंग प्रेस’ और अन्य अंग्रेजी के ग्रंथों के संदर्भित अंशों के अनुवाद में मेरी सहायता की थी। वे इस बात से प्रसन्न थे कि अब अज्ञेयजी मान चुके हैं तो किला तो फतेह है, पर मैं उठने वाले सवालों से जरा मुतमइन न था। उनमें से एकाध तो अज्ञेय जैसी महान् शख्सियत को मुँह चिढ़ाते हुए से लगते थे। तथापि यह वार्त्ता हुई और खूब हुई। यह बातचीत टेप रिकॉर्डर के साथ काफी दिनों पड़ी रही। जितने उत्साह से बातचीत हुई, उतने उत्साह से इसका ट्रांस्क्रिप्शन में तत्परता न दिखती थी। दिन बीतते गए। पर इसे बाद में मैंने ट्रांस्क्राइव किया। एक काॅपी पर उतारा। उनकी आवाज बहुत स्पष्ट थी। सबकुछ समझ में आने योग्य था। बहुत दिनों तक यह वार्त्ता हमारे पास पड़ी रही। १९८४ फरवरी में मैं दिल्ली आ चुका था। जब सूचना विभाग की पत्रिका ‘उत्तर प्रदेश’ की संपादकीय कमान विजय राय ने सँभाली तो बात-ही-बात में उन्होंने एक दिन पूछा—ओमजी, वह अज्ञेयजी वाली बातचीत कहाँ है? दीजिए, उसे ‘उत्तर प्रदेश’ में दे दें। उनके अनेक मनुहार और दबाव पर उसे संपादित कर छपने को दिया। बाद में वह बातचीत दिल्ली आने पर उनकी जन्मशती के मौके पर ‘आलोचना’ में छपी। बेव दुनिया में भी उसके कुछ अंश प्रसारित हुए।
उनसे मिलकर वापस आते हुए हम अभिभूत थे। असुविधाजनक सवालों के उत्तर भी उन्होंने ढंग से दिए थे। हमारे सवालों को बहुत कुशलता से नकारते हुए हमारे भीतर की तथाकथित धुंध को छाँटते हुए समझाने के अंदाज में भी थे। वे जानते रहे होंगे कि ये लड़के भी उनके बारे में हिंदी समाज में फैलाई गई भ्रांतियों से परिचालित होंगे, तभी ऐसा पूछ रहे हैं। पर ऐसा कोई आभास उन्होंने बातचीत के दौरान नहीं होने दिया। बातचीत समाप्त होने पर मैंने उनसे कहा कि कोई कविता सुनाएँ तो हमें अच्छा लगेगा। पर हमारी इस मनुहार को उन्होंने ठुकरा दिया। बल्कि यह कहें कि मुसकराकर टाल दिया। पर आॅटोग्राफ के लिए डायरी बढ़ाने पर बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखकर दिया—
‘जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है।’
मुझे तब तक यह पता न था कि यह उनकी कोई मशहूर काव्यपंक्ति है। मैंने तो यही समझा कि उन्होंने तत्काल यह पदावली निर्मित की है। वे इतने मेधावान तो थे ही कि ऐसी अनेक पंक्ति मनचाहे बना सकते थे। बाद में जब उनकी जन्मशती २०११ में आई तो मन हुआ कि उस आॅटोग्राफ के शीर्षक को कहीं इस्तेमाल करें और निर्णय हुआ कि इस नाम से उनकी प्रेम कविताओं का चयन निकाला जाए। कई प्रकाशकों ने उस दौरान उनके साहित्य पर और उनकी लिखी रचनाओं के चयन प्रकाशित किए। मैंने एक दिन किताबघर प्रकाशन के श्री सत्यव्रत शर्माजी से बात की। वे अज्ञेय शती पर कुछ पुस्तकें छाप रहे थे, जिनमें एक प्रो. विश्वनाथप्रसाद तिवारीजी की भी थी। पर उसमें उन पर अनेक लेखकों के आलेख थे। मैंने कहा, शताब्दी पर तो उनकी कोई मौलिक पुस्तक छापिए, जिसकी शाश्वत माँग बनी रहे। तब उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे बहुत अच्छे आकल्पन के साथ छापा तथा उसकी पीठ पर उनकी ही हस्तलिपि में उनकी वह पदावली लगाई, जो आज भी उनके सुरुचिपूर्ण हस्तलेख का परिचायक है। मैं उन दिनों वाराणसी में पदस्थ था। पुस्तक छपने पर एक प्रति श्री अशोक वाजपेयीजी को और एक प्रति जनसत्ता के संपादक श्री ओम थानवीजी को भेजी। उन्हें इससे पहले इस पुस्तक के प्रकाशन की सूचना न थी।
ओम थानवीजी ने पुस्तक मिलते ही लंबी बातचीत की। मुझे अच्छा लगा कि वे वास्तव में एक सुधी अज्ञेय प्रेमी हैं। इस पर जो अज्ञेय की हँसती हुई तसवीर लगी है, उसके बारे में वाग्देवी के प्रकाशक दीपचंद सांखला से ज्ञात हुआ कि वह उनकी खींची हुई है। अशोक वाजपेयीजी को भी यह स्लिमकाय पुस्तक पसंद आई। उनके ही सुझाए विषय ‘प्रेम के संसार में अज्ञेय’ पर इसमें एक प्राक्कथन भी था। उन्होंने जनसत्ता के अपने स्तंभ ‘कभी-कभार’ में इसकी संक्षिप्त पर आत्मीय चर्चा की। अशोक वाजपेयीजी के आग्रह एवं आयोजना के अधीन राजकमल प्रकाशन के लिए अज्ञेय आलोचना संचयन संपादित किया था, जो शताब्दी वर्ष में ही प्रकाशित हुआ। इन प्रसंगों का उल्लेख इसलिए कि जाने-अनजाने आप ऐसे लेखकों से जुड़ जाते हैं, जो आपकी स्मृति में चिरस्थायी जगह बना लेते हैं। हम जानते हैं कि अज्ञेय के रहते हुए उनका बहुत विरोध हुआ। अनेक शिविरों से उन पर सवाल उठाए गए। लेकिन वे बहुत ही धीरज से सबकुछ देखते हुए प्राय: मौन ही रहते। जरूरत पड़ने पर उनके उत्तर उन्होंने अपने आलोचनात्मक निबंधों में दिए हैं।
’८० में हुई वह मुलाकात आज भी जेहन में ताजा है। जैसे अज्ञेयजी सम्मुख बैठे हों अपनी तेजस्वी आभा से चकित करते हुए। अज्ञेय हिंदी कविता के एक ऐसे गौरव पुरुष हैं, जिनकी जड़ें हिंदी कविता में गहरे समाई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि लेखक परंपरा तोड़ता है, जैसे किसान भूमि तोड़ता है। मैंने अचेत या मुग्धभाव से नहीं लिखा, “जब परंपरा तोड़ी है तब यह जाना है कि परंपरा तोड़ने के मेरे निर्णय का प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा।”
इस भेंट में मैंने उनसे पूछा कि अकसर यह सुनने को मिलता है कि कविता आम आदमी की समझ से बाहर होती जा रही है। यह कुछ थोड़े से बुद्धिजीवियों की समझ की चीज रह गई है। आज की कविता में आम आदमी कहाँ है। उसके संघर्ष को आज की कविता कहाँ तक संप्रेषित कर पा रही है? यह सुनकर वे बोले, क्या आपका यह प्रश्न कुछ-एक नारों की आवृत्ति नहीं कर रहा है। अनुकूल भाव से या प्रतिकूल भाव से। वह बोले, आम आदमी कौन होता है। आम आदमी आज का एक नारा है। कविता आम आदमी के लिए लिखी जाती है, वह एक और नारा है। उन्होंने कहा कि कविता लिखना एक असाधारण कर्म है और हमेशा कविता दो तरह की रही है, ‘एक सीमित समाज के लिए, एक बड़े समाज के लिए’। पूरे-के-पूरे समाज की एक कविता कभी नहीं रही। कविता और सामाजिक परिवर्तन की बात बहुधा की जाती रही है। अज्ञेय के शिविरों में भी और उनके निबंधों में भी इस ओर ध्यानाकर्षण मिलता है। क्या समाज के परिवर्तन में साहित्य कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका अदा करता है, मेरे इस अगले सवाल पर वे पुन: बोले, “यह भी एक नारा है कि साहित्य समाज को बदलने में कोई भूमिका अदा करता है। यह माँग भी साहित्य से कभी नहीं की गई, इधर की जा रही है—और यह भी राजनीतिक दबाव का ही परिणाम है।” वे बोले, “साहित्य समाज बदलने के लिए नहीं लिखा जाता। हाँ, वह पाठक के संवेदन का विकास करता है। उस संवर्धित संवेदना के कारण उसका कोई प्रभाव समाज पर पड़ता हो तो यह बात और है। अव्वल जो साहित्य समाज बदलने के लिए लिखा जाता है, वह उतना समर्थ नहीं होता और टिकाऊ भी नहीं होता।” ये कुछ प्रश्न उन्हें उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त थे। समाज के बदलाव को लेकर दो प्रश्न और किए, तब भी उनकी राय वही रही। उन्होंने विस्तार से समझाने की चेष्टा की कि ‘ऐसा साहित्य जो सामंती युग में कभी लिखा गया, वह जरूर सैनिकों को लड़ाई के लिए प्रेरित करने वाला हुआ करता था, पर आज हम उसे पढ़कर लड़ने को उद्यत नहीं होते। लेकिन ऐसे काव्य की आगे चलकर कोई उपयोगिता काव्य की दृष्टि से होगी, ऐसा मैं नहीं मानता।’
अब हम थोड़ा-थोड़ा सम पर आ रहे थे। वे हाल ही में ‘कितनी नावों में कितनी बार’ संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, सो जानना चाहा कि अकसर लोगों को उनकी कमतर कृतियों पर पुरस्कार दिए गए हैं। इस अर्थ में इस पुरस्कार को लेकर आपका क्या मानना है तो इसके उत्तर में उन्होंने माना कि वह उनकी श्रेष्ठ कृति नहीं है। उन्होंने बताया कि जहाँ तक उन्हें मालूम है, एक दूसरी रचना संभवत: ‘शेखर : एक जीवनी’ का अनुमोदन पुरस्कार समिति ने किया था, पर कदाचित् वह निर्णय उनके अनुकूल नहीं हुआ। फिर बाद में जो उस अवधि में उन्हें विचारणीय लगी, उसे पुरस्कृत किया। फिर हमारी बातचीत युवा पीढ़ी के रचनात्मक कर्म, विदेशी पठन पाठन के प्रभावों से होकर समाज में पनपती अलगाव की प्रवृत्ति से होकर उनकी कविताओं की दुरूहता पर आ टिकी। इस प्रश्न के उत्तर में जो एक बात हमें उन्होंने बताई, वह ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि ‘कवि कंठाभरण’ में आचार्य क्षेमेंद्र ने कहा है कि हर किसी से सीखो, हर वर्ग के व्यक्ति के पास जाओ, गँवार-से-गँवार आदमी से कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन दो आदमियों से बचो। एक व्याकरण से, दूसरे तार्किक से। इस अर्थ में उनका कहना था, आज का अध्यापक काव्य का व्याकरण तो पढ़ना-पढ़ाना जानता है, पर कविता से उसका प्रयोजन कम ही है। अंत में बात शोध प्रबंधों की भरमार को लेकर हुई। बोले कि इस दिशा में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, यह सच है। क्योंकि ये समझ का विकास नहीं कर रहे, नई जानकारी भी बहुत कम देते हैं। गतानुगतिकता ज्यादा है।
लगभग एक घंटे की बातचीत में वे थक से गए थे। हम दोनों सजग थे कि हमारे सवाल से वे हमें किसी मुहिम से प्रेरित न मान बैठें। क्योंकि हमारे सवाल कुछ तीखे जरूर थे, लेकिन हम पहली बार एक विराट् लेखक से मिल रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा, उन दिनों अज्ञेय का विरोध हवा में था। तारसप्तक और सप्तक सीरीज व प्रयोगवाद के मान्यता पा जाने से उनके प्रतिद्वंद्वी लेखक दु:खी थे, दूसरे बाम पक्ष के विचारकों के लिए अज्ञेय सदैव प्रश्नों के घेरे में रहते थे। उनके वैचारिक निबंधों को देखें तो बहुधा अपने निबंधों में तब के सवालों या अनर्गल प्रलापों पर उनके सफाई भरे निबंध पढ़ने को मिलते हैं। उनका जीवन रचनात्मक लेखन के अलावा ऐसे अप्रत्याशित सवालों का उत्तर देते हुए भी बीता। इस बात का भान मुझे तब हुआ, जब एक बाद कोलकता में अशोक सेकसरिया के यहाँ गिरधर राठी मिले तो अज्ञेय की चर्चा चलने पर उन्होंने कहा कि अज्ञेय के इसी चौतरफा विरोध के चलते उनके मन में उनसे मिलने की प्रेरणा ही नहीं जागी। हमें लग रहा था कि वैमत्य अलग है, किंतु मिलनसारिता में अज्ञेय का कोई सानी नहीं है। वे भले व्यक्तिवादी प्रस्तावनाओं के कवि रहे हों, पर समय-समय पर उनके विचारों में पर्याप्त प्रगतिशीलता नजर आती है।
संयोग यह कि बाद में भी अज्ञेय के बारे में जानने का अवसर मिलता रहा। नजदीक से उन्हें देखने का। उन पर लिखने-लिखाने के अवसर भी मिलते रहे। पर यह कैशोर्य की हम दोनों मित्रों की अज्ञेय से मुलाकात हमारे लिए एक दुस्साहस ही कही जाएगी। यह संवाद देर से लिप्यंतरित और प्रकाशित होने के कारण इसे अज्ञेय जीवनकाल में न देख सके। पर यह आज भी उनके कुछ चुनिंदा साक्षात्कारों में एक है। साहित्य में एक बड़ी शख्सियत को पास से देखने का यह पहला मौका था। हमारे भीतर कौतूहल और विस्मय दोनों थे। हम उनके पार्थिव सौंदर्य पर मुग्ध थे तो उत्तर देने की उनकी चातुरी पर भी कि अनुकूल सवाल न होने के बावजूद उनकी त्योरियाँ नहीं चढ़ीं। वे हल्की स्मिति के साथ ही बोलते रहे। आज भी जब अज्ञेय की बात चलती है तो गर्व होता है कि हमने उन्हें देखा है, उनसे बात की है। यद्यपि अब तो बहुतेरे बड़े कवियों, लेखकों से भेंट है, कइयों से बातचीत भी, लेकिन अज्ञेय से बातचीत के वे क्षण नहीं भूलते। न मुझे, न चंद्रपाल सिंह को। तेहि नो दिवसा गता:। आज वे नहीं हैं, पर उनके शब्द छूते हैं। उनकी याद भर से आती हुई स्मृति-सुगंध जैसे आतप में तपे हुए व्यक्ति को छाया देती हो।
जी-१/५०६ ए, उत्तम नगर,
नई दिल्ली-११००५९
दूरभाष ः ९८१००४२७७०