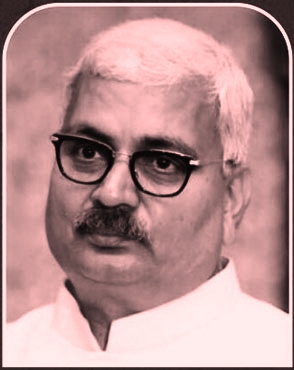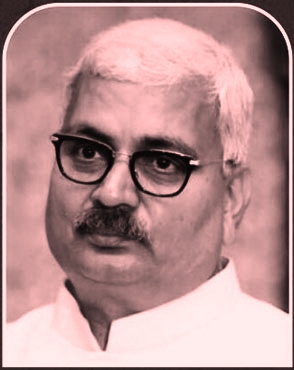
लेखन में पत्रकारीय छवि सर्वनिहित है। उनके लेख, रिपोर्ट और इतिहासबद्ध पुस्तकें इसकी प्रमाण हैं। पत्रकारीय लेखन में हेमंतजी ठोस और तथ्यपरक लिक्खाड़ माने जाते हैं। लेकिन पत्रकारिता से इतर उनका लेखन संवाद और बिंबों का एक कमाल का कोलाज है। वह निबंधात्मक लेखन में प्रवीण हैं, लेकिन उस लेखन और लेखक की स्याही बनारसी है, इसीलिए उसमें लालित्य है। ललित निबंध लिखने वाले हेमंतजी कथेतर गद्य के माहिर हैं। संवाद की शैली, दृष्टांतों का रेशम, छोटे-छोटे कथानकों से उकेरे गए बिंब और इन सबकी प्रतिस्थापना में इतिहास तथा परंपरा के प्रमाण, यही ताना-बाना और रचना हेमंतजी के कथेतर गद्य को रोचक और ललित बनाते हैं।
आह्लादित हूँ। किताबों के दिन अब लौट रहे हैं। दिल्ली में लगे विश्व पुस्तक मेले में उमड़ी भीड़ तो यही उद्घोष कर रही है। खासकर हिंदी किताबों की बिक्री से बड़ी तसल्ली हुई। हिंदी में किताब खरीदकर पढ़ने की आदत नहीं है। और पुस्तकें उपहार में देने की तो कभी प्रथा ही नहीं रही है। १९८० से पुस्तक मेले में जा रहा हूँ, पर इस दफा मेले के निकास गेट का नजारा बदला-बदला सा था। लोगों के कंधों पर टँगे थैले किताबों से भरे थे। प्रकाशक भी बम-बम थे। एक आकलन के मुताबिक दस रोज के मेले में कोई बीस लाख लोग आए। ज्ञान के इस महाकुंभ में ५० से ज्यादा देशों के दो हजार से ज्यादा प्रकाशकों ने अपनी किताबों की नुमाइश की। कोई सात से आठ करोड़ की ब्रिकी भी हुई। पर एक बात खटकी, यह काहे का विश्व पुस्तक मेला? यहाँ तो बांग्ला, तमिल, तेलगु, कन्नड़, गुजराती, असमिया का स्टॉल तक नहीं था। जिनका साहित्य सचमुच में काफी समृद्ध है। भारतीय भाषाओं की उपस्थिति मेले में न होना चिंता का कारण है। इस लिहाज से राष्ट्रीय ही नहीं था तो विश्व पुस्तक मेला कैसा? इसे दिल्ली पुस्तक मेला कहना चाहिए।
आईपैड, किंडल और स्मार्ट फोन ने किताबों को ज्ञान और मेधा के अखाड़े से बाहर कर दिया था। मेले को देखकर लगा कि किताबें अब उपेक्षा के इस दायरे से बाहर आ रही हैं, वरना बुकसेल्फ से झाँकती लाचार किताबें कंप्यूटर की सौतन लगने लगी थीं। इसलिए किताबों की बिक्री दिन-ब-दिन घट रही थी। हिंदी में किताबों के मुफ्तखोर बहुत हैं या फिर चोर हैं। मेरी पचास प्रतिशत पुस्तकें यह बिरादरी पार कर देती है। मेरा मानना है कि किताबों की जगह दुनिया का कोई गैजेट नहीं ले सकता। एआई भी नहीं। किताबों के पुराने पड़ते कागज की गमक और उस पर जमी धूल की जो सोंधी महक उठती है, उसकी जगह क्या कोई कंप्यूटर ले सकता है? और पुरानी यादें किताबों के सफों में कैद रहती हैं। उनको छूते ही न जाने कितनी आहटें आप सुन सकते हैं।
इस सिलसिले पर गुलजार कहते हैं, “जबाँ पर जाइक़ा आता था जो सफ़्हे पलटने का/अब उँगली क्लिक करने से बस इक झपकी गुजरती है/बहुत-कुछ तह-ब-तह खुलता चला जाता है परदे पर/किताबों से जो जाती राब्ता था, कट गया है/कभी सीने पे रख के लेट जाते थे/कभी गोदी में लेते थे/कभी घुटनों को अपने रेहल की सूरत बनाकर/नीम सज्दे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से/वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी/मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुकए/किताबें माँगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे/उन का क्या होगा...? वो शायद अब नहीं होंगे!”
इसलिए गुलजार साहब ‘नर हो, न निराश करो मन को’, किताबों का जमाना लौट रहा है। हमारे धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा में किताबें प्रासंगिक बनी रहेंगी। इस नश्वर संसार में अगर वह सुरक्षित है तो मान लीजिए कि अभी कुछ नष्ट नहीं हुआ है। मैंने जब से होश सँभाला है, इसी संपदा को जीता, महसूस करता रहा हूँ। आज भी घर में मेरी पसंदीदा जगह लाइब्रेरी ही है, जहाँ एक चिर-परिचित सुकून हमेशा मिलता है। दुनिया भर की दौड़-भाग और उथल-पुथल के बीच मैं उसी लाइब्रेरी में जाकर ठहर जाता हूँ। यह वक्त का एक ऐसा ठहराव होता है, जो मन को नई ऊर्जा, दृष्टि और संभावनाओं से भर देता है। इसलिए लगता है किताबें अनमोल हैं।
कल मुंबई जा रहा था। एयरपोर्ट पर किताबों की दुकान में ‘वेद’, ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के अंग्रेजी अनुवाद देखे। हिंदी की कोई किताब वहाँ नहीं थी। एक साथ अपनी परंपरागत ज्ञान-संपदा अंग्रेजी में देख खुशी भी हुई और एक आशंका भी। अगर कहीं ये सब नष्ट हो जाते, तो हमारी संस्कृति और ज्ञान-परंपरा का क्या होता? किसी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना हो तो वहाँ की परंपरा और ज्ञान-भंडार नष्ट कीजिए। ईसाइयत और इसलाम ने यही तो किया। अपनी ज्ञान-परंपरा से कटा व्यक्ति प्राणविहीन हो जाता है। वह समाज अपनी जड़ों से कट जाता है। दुनियाभर के तानाशाह ऐसा ही मानते हैं। इसलिए वे नस्लों के खात्मे के लिए उनकी लाइब्रेरियों को जरूर नष्ट करते थे। नालंदा, तक्षशिला, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी पर हमले इसी खातिर हुए। वरना लाइब्रेरी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आक्रांता तो देश जीत ही चुके थे। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर भी इसलिए नहीं तोड़ा गया कि वह शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर था, बल्कि इसलिए टूटा कि औरंगजेब की नजरों में वहाँ दुष्ट विद्या पढ़ाई जाती थी। वहाँ बड़ी भारी लाइब्रेरी थी। डॉ. मोतीचंद्र के ‘काशी का इतिहास’ में मंदिर तोड़े जाने के लिए औरंगजेब का जो फरमान छपा है, उसमें यही लिखा है कि मंदिर परिसर में दुष्ट विद्या की शिक्षा दे काफिर बनाए जाते थे। औरंगजेब का भाई दाराशिकोह वहीं संस्कृत पढ़ता था। औरंगजेब इस कारण इस मंदिर को और बुरा मानता था। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी, कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तइद खाँ की किताब ‘मआसिर-ए-आलमगीरी’ में इस ध्वंस और उसके कारण का वर्णन है। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने के मूल में वहाँ धर्म, दर्शन की किताबें थीं।
इन आततायियों और आक्रांताओं को यह भरोसा था कि अगर शहर नष्ट होंगे तो फिर बन सकते हैं। आबादी दोबारा बस जाती है। संपत्ति की भी भरपाई हो जाती है, पर सांस्कृतिक केंद्र जब नष्ट होते हैं, तो फिर नहीं बनते और यदि बनते भी हैं, तब वे वह नहीं रहते, जो थे। क्या नालंदा अब फिर बन सकता है? पुराना तक्षशिला क्या स्वप्न में भी आ सकता है? एक पागल शासक ने सिकंदरिया (अलेक्जेंड्रिया) की पूरी लाइब्रेरी जला डाली। उसका तर्क था, अगर केवल एक कुरान में ही सबकुछ है, तो इन पुस्तकों की क्या जरूरत? फिर जो कुरान में है, यदि वही इन पुस्तकों में है तो भी ये सब किताबें बेकार हैं, जलने के काबिल हैं। यदि कुरान में जो नहीं है, वह इन पुस्तकों में है, तब तो इन्हें बिल्कुल जला देना चाहिए। इसलिए उस सनकी ने कुरान को छोड़ बाकी सारी पुस्तकें जलवा दीं। क्या वह लाइब्रेरी फिर कहीं से लाई जा सकती है?
अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे प्राचीन और विशालतम मानी जाती थी। मिस्र में टॉलमई राजवंश के संरक्षण में ईसा पूर्व तीसरी सदी में बना यह पुस्तकालय ४८ ईसा पूर्व में जलाकर नष्ट कर दिया गया। पुस्तकों का वह संग्रहालय दोबारा नहीं बनाया जा सका। लगभग तीन शताब्दियों तक यह लाइब्रेरी मिस्र में ज्ञान-विज्ञान का प्रमुख केंद्र रही। मिस्र दुनिया में किताबों का जनक रहा है। जब हम लिखने के लिए भोज-पत्र का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने पेड़ की छाल से कागज बना लिया था।
दुनिया की अनगिनत पुस्तकें युद्ध की भेंट चढ़ाई जाती रहीं। युद्ध कितना विनाशक होता है, इसका सही अनुमान सामान्य दृष्टि से नहीं होता है। हमारा आकलन बस भौतिक विनाश तक ही सीमित रहता है, पर किताबों को स्वाहा करने वाली इस आग में हमारा कितना सांस्कृतिक अंश भस्म होता है, यह उसके अनुमान से परे रह जाता है। हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और पहुँचती भी है तो हमारा ज्ञान सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। मनुष्य की विनाशक महत्त्वाकांक्षा, धार्मिक अंधविश्वास और ईर्ष्या जबरन सांस्कृतिक माध्यमों और केंद्रों को चबा जाती है।
इराक के हमले से कुवैत के सिर्फ तेल के कुएँ ही नहीं जले, वरन् उसका वह संग्रहालय भी जल गया, जो बहुत मेहनत से बना था। कुवैत का विश्वप्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय, जहाँ कभी इसलामिक कला-जगत् का सबसे विशाल संग्रह प्रदर्शित था, युद्ध में खँडहर बन गया। संग्रहालय की दुर्लभ वस्तुएँ लूटकर इमारत जला दी गई। इसमें इसलामिक कला तथा पुरातत्त्व दीर्घाएँ थीं। इन दीर्घाओं में किताबों के अलावा खाड़ी से इकट्ठा किए गए अद्भुत शंख, सीप, डाक टिकट, मुहरें, नक्काशीदार पत्थर, सिक्के तथा कुवैती कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्र थे। यह संग्रहालय इसलामिक कला का विश्व में सबसे बड़ा संग्रह था, जो अब राख हो चुका है। संग्रह में सातवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक की सात हजार कलाकृतियाँ थीं। सब नष्ट हो गईं।
ग्रीक सभ्यता के साथ अंग्रेजों ने भी यही किया। उनकी लाइब्रेरी और मूर्तियाँ लूट ले गए। हाँ, पुस्तकें उन्होंने जलाई नहीं, लंदन के म्यूजियम में रखीं। और यह सब कला में नग्नता की आड़ में किया गया। कुछ ऐसा ही नालंदा के महान् विश्वविद्यालय के साथ हुआ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकाल के शासक कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा संस्कृत शब्द नालम्+दा से बना है। संस्कृत में ‘नालम्’ का अर्थ ‘कमल’ होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालम्+दा यानी कमल देने वाला या फिर ज्ञान देने वाला। इस विश्वविद्यालय के नाम में ही ज्ञान की जड़ें समाई थीं। यहाँ इतनी पुस्तकें रखी थीं कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की पुस्तकें इस विश्वविद्यालय में थीं। यहाँ बौद्ध और जैन धर्म की मूल्यवान पुस्तकों के साथ ही वेद, विज्ञान, खगोलशास्त्र, सांख्य, वास्तुकला, शिल्प, मूर्तिकला, व्याकरण, दर्शन, शल्यविद्या, ज्योतिष, योगशास्त्र और चिकित्साशास्त्र की दुर्लभ पुस्तकें मौजूद थीं। इसमें कुल तीन पुस्तकालय थे—रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। एक पुस्तकालय भवन तो ९ तलों का था। इन पुस्तकालयों में हस्तलिखित हजारों पुस्तकें और छपी हुई लाखों पुस्तकें थीं। यहाँ कई दुर्लभ पुस्तकों का भंडार था। मगर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने ११९९ ई. में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकें जलकर राख हो गईं। हमारे इतिहास के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद भी ३ महीने तक पुस्तकें धू-धू करके जलती रहीं। बताते हैं कि कई अध्यापक और बौद्ध भिक्षु अपने कपड़ों में छुपाकर कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों को बचा तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इसी ज्ञान-संपदा ने तिब्बत को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में बदल दिया, बाद में जिन्हें चीनी आक्रमणकारियों ने जला दिया। दलाई लामा जरूर भागते वक्त कुछ पांडुलिपियाँ खच्चर पर लादकर भारत लाए थे। तिब्बत से कुछ पुस्तकें राहुल सांकृत्यायन भी खच्चरों पर लादकर ले आए थे।
ऐसे कितने ही विनाशक युद्धों में, लूट में, आधिपत्य की लालसा में ज्ञान का कितना अमृत नष्ट हो गया, पता नहीं। पर यह अमृत हमारी पीढ़ियों के जीवन-आँगन का कल्पतरु जरूर था। जो नष्ट हो गया, उसका क्या रोना? असल चुनौती तो यह है कि जो संरक्षित है, जो उपलब्ध है, जो पहुँच के दायरे में है, उसे कैसे ग्रहण किया जाए? पढ़ने-लिखने की आदत मानव को इनसान बनाने का सबसे सटीक साँचा होती है। यह कैसे बनी रहे? इसलिए पुस्तक मेले जरूरी हैं। इनके मायने हैं। ज्ञान का अमृत इसी ‘कुंभ’ में मिलेगा।
आज भी लिखते-लिखते कोई दुविधा होती हो तो मुझे किताबों की शरण में जाना पड़ता है। उनसे संदर्भ लेने पड़ते हैं। और मित्र कहते हैं, बड़ा लंबा लिख देते हो यार, पढ़त-पढ़त...फट जाला। पिछले दिनों कथक नृत्य की उम्र को लेकर मन में सवाल उठा। किसी ने एक कतरन दिखाते हुए कहा कि यह नृत्य ईसा पूर्व का है। मैं अपने अध्ययन कक्ष में जा यह ढूँढ़ने लगा कि इसका उल्लेख सबसे पहले कब और कहाँ मिलता है? कुछ पुस्तकें खँगाली। संगीत और नृत्य के इतिहास पर एक किताब हाथ लगी पर यह क्या? कथक तक आते-आते आगे के पन्ने गायब थे। बहुत क्षोभ हुआ। अगर आपकी किसी किताब से कुछ पन्ने गायब हों तो लगता है, आपका शरीर विकलांग है।
मुझे फौरन याद आई काशी हिंदू विश्वविद्यालय की केंद्रीय लाइब्रेरी, जो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बनवाई थी। बड़ी समृद्ध और खूबसूरत लाइब्रेरी। दुनिया के बड़े-से-बड़े विश्वविद्यालयों से टक्कर लेती। मेरे विश्वविद्यालयी जीवन के ज्यादा दिन इसी में बीते। उन दिनों वहाँ ‘स्टैक’ में जाने की इजाजत छात्रों को थी। मैंने कई बार देखा, कुछ छात्र स्टैक में जाते, जरूरत की पुस्तकें निकालते। किनारे जाकर जरूरी अध्याय फाड़कर अपनी कमीज के भीतर खोंस लेते। कुछ लोग ब्लेड से पुस्तक की हत्या करते। उस वक्त तो यह इतना बड़ा अपराध नहीं लगता था, पर अब लगता है कि दरअसल वे छात्र नहीं, पुस्तकों के हत्यारे थे।
अंग्रेज लेखक फ्रांसिस बेकन, दार्शनिक और राजनेता थे। उनके विचार से कुछ पुस्तकें चखी जाती हैं, कुछ निगली जाती हैं और कुछ चबा-चबाकर खाई और पचाई जाती हैं। पता नहीं इन पन्नों को पचाया गया या नहीं, पर किसी की स्वार्थपरता उन्हें चबा अवश्य गई। किताब फाड़ने की हमारी इस जघन्य प्रवृत्ति ने ज्ञान के इस सागर को खारा कर दिया है। सोच ही रहा था, तभी यकायक मेरे सामने एक धुँधली सी आकृति उभरती है। संगीत के इतिहास की उस पुस्तक से उभरकर एक चित्र मेरे मानस से टकराता है, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी का चित्र। धीरे-धीरे वह मुखर होने लगता है। उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। “आज से लगभग साढ़े तेरह सौ वर्ष पहले मैं नालंदा का छात्र था। उत्तर भारत का यह विश्वविद्यालय अपनी ज्ञान-गरिमा के कारण विश्व में प्रसिद्ध था। देश-विदेश से विद्यार्थी यहाँ विद्यार्जन के लिए आते थे। उन दिनों विख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया। नालंदा को देखकर वह चमत्कृत हो गया। इतना विशाल विद्या का केंद्र और इतना विशाल पुस्तकालय उसने अपने जीवन में नहीं देखा था”।
‘अतिथि देवो भव’ का मंत्रोच्चार करने वाली हमारी संस्कृति ने ह्वेनसांग की खूब आवभगत की। उसे सम्मान दिया। हमारे आचार्यों ने उसकी जिज्ञासाएँ शांत कीं। और जब ह्वेनसांग लौटने लगे, तो उन्हें ढेर सारे ग्रंथ भेंट में दिए गए। कुछ ग्रंथों को वह स्वयं माँगकर ले गए। उनकी पुस्तक-पिपासा अद्भुत थी। पुस्तकें गाड़ी पर लादी गईं। ब्रह्मचारी बोलता रहा, चातुर्मास बीत चुका था। फिर भी आकाश में उस दिन अचानक बादल छाए थे। जब ह्वेनसांग हमारे विश्वविद्यालय से विदा होने लगे, तो आसमान पसीजने लगा। आचार्य ने मुझे बुलाकर कहा, “वत्स, देखो, यह हमारे मान्य अतिथि हैं, इनकी सेवा देवता की सेवा है। वर्षा शुरू हो गई है। उन्हें नदी के उस पार तक सकुशल पहुँचा दो। और हाँ, इसका ध्यान रखना कि इन पुस्तकों में से एक भी नष्ट न होने पाए। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।” मैं उनके साथ-साथ चल पड़ा। नाव पर किताबें लादी गईं। बाढ़ की नदी फुफकार रही थी। मध्य धारा में आते-आते नाव डगमगाने लगी। नाविक चिल्लाया, “बोझ कम कीजिए, वरना नाव डूब जाएगी।” लोग घबरा गए। ह्वेनसांग बड़ी दुविधा में पड़ा। वह किस ग्रंथ को फेंके, किसे न फेंके। मेरे कान में आचार्य की ध्वनि पुनः गूँजी, ‘देखना, इन पुस्तकों में से एक भी नष्ट न होने पाए। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।’
“मैं एकदम खड़ा हो गया और विनीत भाव से बोला, “आप घबराएँ नहीं। मैं अभी बोझ हलका किए देता हूँ...और मैं ‘झम’ से नदी में कूद पड़ा। तबसे आज तक हमारी आत्मा बड़े-बड़े पुस्तकालयों में ही घूमा करती है। तब से जब भी मैं किसी पुस्तक को नष्ट होते या किसी विद्यार्थी को इसके पन्ने फाड़ते देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि कोई हमारी इन सांस्कृतिक धरोहरों को घायल कर रहा है। मैं चीख पड़ता हूँ। मुझे लगता है कि इस सांस्कृतिक संदर्भ में अधिकांश बहरे हो गए हैं। भगवान्, इन बहरों को सद्बुद्धि दो।” मेरे हाथ से छूटकर संगीत की वह किताब गिर गई। मैं पसीने-पसीने था। अध्ययन-कक्ष में और कोई नहीं था। सिर्फ मैं, मेरी पुस्तक और अवचेतन में वह कथा।
हमारी इन मूल्यवान धरोहरों का इतिहास भी रोचक है। दुनिया को पहला ग्रंथ ऋग्वेद की शक्ल में हमने दिया। पर छपे हुए हर्फ रोम ने दिए। पहली शताब्दी ईसवी में रोम लिखित शब्दों से भरा पड़ा था। मूर्तियों, स्मारकों और कब्रों पर आलीशान बड़े अक्षरों में लिखा जाता था। नागरिक मोम से ढकी लकड़ी की लेखन पिट्टयों पर नोट लिखते और संदेश भेजते थे। और धनी लोगों के पुस्तकालयों में इतिहास, दर्शन और कला की किताबें भरी होती थीं। लेकिन ये किताबें वैसी नहीं थीं, जैसी हम जानते हैं—ये मिस्र के पपीरस की चादरों से बनी स्क्रॉल थीं, जिन्हें ४.५ से १६ मीटर (१४.७६ फीट से ५२.४९ फीट) की लंबाई के रोल में चिपकाया जाता था। उनकी सर्वव्यापकता के बावजूद उनमें खामियाँ भी थीं।
कई इतिहासकार पुस्तकों की उत्पत्ति का श्रेय मिस्र को देते हैं, जिनके पपीरस स्क्रॉल (papyrus scrolls) आज की पुस्तकों से बहुत अलग दिखते थे। हजारों बरस पहले जब उन्होंने पहली बार लिखित लिपि विकसित की थी, तब से मिस्र के लोग धातु, चमड़े, मिट्टी, पत्थर और हड्डी सहित कई अलग-अलग सतहों पर लिखते थे। पपीरस स्क्रॉल पर लिखने के लिए रीड पेन (ईख की कलम) का इस्तेमाल होता था। स्क्रॉल बनाने के लिए पपीरस की अलग-अलग शीट को एक साथ चिपकाया या सिल दिया जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पपीरस लेखन के लिए सबसे आम सतह थी और इसका इस्तेमाल यूनानियों और रोमनों द्वारा किया जाता था। अलेक्जेंड्रिया की रॉयल लाइब्रेरी के संग्रह में ऐसे लगभग पाँच लाख स्क्रॉल थे।
इसके बाद आया कोडेक्स (Codex)। यानी एक तरह का चर्मपत्र। यह चर्मपत्र जानवरों की खाल से बनाया जाता था, जिसे एक लचीली, समतल सतह बनाने के लिए खुरचकर पतला किया जाता था। पपीरस की तुलना में चर्मपत्र के कई फायदे थे। यह अधिक टिकाऊ था, इस पर दोनों तरफ लिखा जा सकता था। कोडेक्स पद्धति की संरचना आज की पुस्तकों जैसी ही है। कोडेक्स पपीरस स्क्रॉल की तुलना में इस्तेमाल करने वालों के लिए ज्यादा फ्रेंडली था। अधिक पोर्टेबल, स्टोर करने और सँभालने में आसान तथा उत्पादन में कम खर्चीला। यह पाठकों के बीच जल्दी लोकप्रिय हो गया। प्रारंभिक ईसाई ग्रंथों के लिए कोडेक्स को ही प्राथमिकता दी गई थी। छठीं शताब्दी तक इसने स्क्रॉल की जगह ले ली।
किताबों की विकास-यात्रा का अगला पड़ाव था कागज। किताबों के इतिहास में बड़ा इनोवेशन कागज बना। चीन में तांग राजवंश के दौरान कागज का आविष्कार हुआ। हान राजवंश (१०५ ई.) के दौरान एक चीनी अधिकारी, जिसका नाम कै लुन (Cai Lun) था, उसने कागज का आविष्कार किया। कागज पर छपे पाठ के पहले ज्ञात उदाहरण ७६४ ई. में जापान की महारानी शोतोकू द्वारा कमीशन किए गए बौद्ध प्रार्थनाओं के छोटे, २.५ इंच चौड़े स्क्रॉल, जो वाशी (कागज) स्याही के मिलते हैं। ७वीं शताब्दी तक कागज कोरियाई प्रायद्वीप के जरिए चीन से जापान में आ चुका था और जापानियों ने हीनयानकाल में कागज बनाने की विधि में सुधार कर वाशी (washi) का विकास किया।
दुनिया में छपी हुई किताब का सबसे पहला उदाहरण डायमंड सूत्र (८६८ ई.) नामक एक बौद्ध ग्रंथ है। डायमंड सूत्र का संस्कृत शीर्षक ‘वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र’ (ज्ञान की पूर्णता) एक महायान बौद्ध सूत्र है। डायमंड सूत्र के तांग राजवंश-चीनी संस्करण की एक प्रति १९०० में डुनहुआंग पांडुलिपियों के बीच दाओवादी भिक्षु वांग युआनलू द्वारा पाई गई और १९०७ में ऑरेल स्टीन (हंगरी में जनमे ब्रिटिश पुरातत्त्वविद्) को बेची गई थी। डायमंड सूत्र को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित तिथिबद्ध मुद्रित पुस्तक माना जाता है।
टाइप फॉण्ट (movable metal type) से मुद्रित पहली किताब थी जिक्जी (Jikji)। यह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है, जिसे १३७७ में गोरियो (Goryeo) राजवंश के दौरान छापा गया था। यह दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, जो चल धातु प्रकार (movable metal type) से मुद्रित है। हालाँकि यह प्रिंटिंग-मशीन पर छपी पुस्तक नहीं थी। यूनेस्को ने सितंबर २००१ में जिक्जी को दुनिया के सबसे पुराने मेटलॉइड प्रकार के रूप में पुष्टि की और इसे ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम’ में शामिल किया।
लेकिन प्रिंटिंग प्रेस बनाने में जर्मनों ने बाजी मारी। जर्मन आविष्कारक जोहांस गुटनबर्ग (१४००-३ फरवरी, १४६८) ने दुनिया का पहला यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस १४४० ई. में विकसित किया। मानव इतिहास में यह एक मील का पत्थर था। प्रिंटिंग प्रेस ने पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और ज्ञानोदय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन एक ‘मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन’ थी। इस प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। किताबों की छपाई होने लगी। लोगों के बीच किताबों की माँग बढ़ने लगी। गुटनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन में सबसे पहले जर्मन भाषा में एक कविता छापी गई। इसके बाद लैटिन ग्रामर की एक किताब छपी। लेकिन गुटनबर्ग प्रेस को पहचान बाइबिल की छपाई के बाद ही मिली। गुटनबर्ग बाइबिल के नाम से जानी जाने वाली यह ४२ पंक्ति वाली बाइबिल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे पुरानी मशीन से मुद्रित किताब के रूप में सूचीबद्ध है। गुटनबर्ग ने पहलेपहल बाइबिल की १८० प्रतियाँ छापीं थी इस मूवेबल प्रिंटिंग मशीन से छपाई का काम ब्लॉक में अक्षर खोदकर किया जाता था। इस मशीन की खास बात यह थी कि इसकी छपाई में लकड़ी की जगह मेटल ब्लॉक का इस्तेमाल होता था। इस मशीन के ईजाद होने से किसी भी तरह के पेपर पर छपाई करना आसान हो गया। ये प्रिंटिंग मशीन रोजाना एक हजार से ज्यादा पेज छाप सकती थी। इसके पहले छपाई की जो तकनीक थी, उससे दिनभर में सिर्फ ४० से ५० पेज ही छप पाते थे।
गुटनबर्ग प्रेस के आने से पहले बाइबिल की हस्तलिखित प्रतियाँ ही मौजूद थीं। हाथ से लिखने में पादरी को एक साल का समय लगता था, छपाई ने यह मुश्किल कम कर दी। चर्मपत्र की तुलना में कागज का उत्पादन बहुत सस्ता था। प्रिंटिंग प्रेस से पहले पुस्तकों की आमतौर पर प्रतिलिपि बनाई जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस ने इस प्रकिया को रफ्तार दे दी। १५वीं शताब्दी के अंत यानी गुटनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के ५० साल बाद पूरे यूरोप में छपाई की दुकानें खुल गईं, जिनमें अकेले जर्मनी में कोई ३०० प्रिंटिग प्रेस थे। हैरी रैनसम ह्यूमैनिटीज रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले पूरे यूरोप में किताबों की कुल संख्या लगभग ३०,००० थी और सभी हाथ से लिखी हुई थीं।
‘सेल्टिक साल्टर’ को स्कॉटलैंड की बुक ऑफ केल्स के रूप में दर्जा प्राप्त है। भजनों की यह पॉकेट-साइज किताब एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में रखी गई है। इस पुस्तक का निर्माण ११वीं शताब्दी में हुआ था, इसे स्कॉटलैंड की सबसे पुरानी किताब मानते हैं।
इसके बाद कोई पाँच सौ साल पुरानी किताब मिलती है मैड्रिड कोडेक्स। १८६० में स्पेन में इसे खोजा गया। मैड्रिड कोडेक्स, जिसे ट्रू-कोर्टेसियंस कोडेक्स के नाम से भी जाना जाता है—लगभग ९००-१५२१ ई. की प्री-कोलंबियन माया संस्कृति से जुड़ी एकमात्र जीवित पुस्तकों में से एक है। यह किताब युकाटेकन में लिखी गई है, जो मायान भाषाओं का एक समूह है, जिसमें युकाटेक, इट्जा, लैकांडन और मोपन शामिल हैं। मैड्रिड कोडेक्स के निर्माण की सटीक तारीख पर विशेषज्ञ असहमत हैं, यह किताब स्पेन के मैड्रिड में ‘म्यूजियो डि अमेरिका’ में रखी गई है।
‘सिद्दुर' एक यहूदी प्रार्थना पुस्तक है, जो लगभग ८४० ई.पू. की है। पूरी चर्मपत्र पर। अभी भी अपनी मूल बाइंडिंग में मौजूद है। किताब की प्राचीनता इसके बेबीलोनियन स्वर संकेत से सिद्ध होती हैं—जो अंग्रेजी भाषा के लिए पुरानी या मध्य अंग्रेजी के समान है। यूरोप की सबसे पुरानी ज्ञात बची हुई पुस्तक ‘सेंट कथबर्ट गॉस्पेल’ है। यह किताब लगभग ६९८ई में नॉर्थंबरलैंड के पास लिंडिसफर्ने द्वीप पर ब्रिटिश ईसाई नेता सेंट कथबर्ट के साथ दफनाई गई थी। इस किताब को वाइकिंग हमलावरों से बचने के लिए डरहम ले जाया गया, जहाँ यह विनाश से बाल-बाल बच गई।
मिस्र की ‘नाग हम्मादी’ सबसे पुरानी बची और बँधी हुई किताबों में से एक मानी जाती है। ऊपरी मिस्र के नाग हम्मादी शहर में एक स्थानीय व्यक्ति को १९४५ में एक सीलबंद जार के अंदर १३ चमड़े की बँधी हुई पपीरस कोडेक्स की शक्ल में यह किताब मिली। गनोस्टिक ग्रंथों वाली ये किताबें चौथी शताब्दी ईस्वी के पहले भाग की हैं। कॉप्टिक भाषा में लिखी, इन कोडेक्स को ग्रीक से कॉपी किया गया माना जाता है।
‘पिरगी गोल्ड टेबलेट्स’ इटली के प्राचीन पिरगी में एक अभयारण्य की खुदाई में १९६४ में मिली तीन सोने की प्लेटें ५०० ईसा पूर्व की हैं। किनारों के चारों ओर छेद होने के कारण, विद्वानों का मानना है कि वे कभी एक साथ बँधी हुई थीं। दो एट्रस्केन पाठ में लिखी गई हैं, जबकि एक फोनीशियन में लिखी गई है, जिसमें राजा थेफरी वेलियानास द्वारा फोनीशियन देवी एस्टेर्ट को समर्पित एक समर्पण शामिल है। अब ये प्लेटें इटली के रोम में राष्ट्रीय एट्रस्केन संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। सोने की प्लेट पर छपी यह भी एक तरह की किताब थी।
‘एट्रस्केन गोल्ड बुक’ ७० साल पहले बुल्गारिया में स्ट्रोमा नदी के किनारे नहर खोदते समय मिली थी। यह दुनिया की पुरानी किताबों में एक मानी जाती है। यह पुस्तक २४ कैरेट सोने की ६ शीटों से बनी है, जिन्हें छल्लों से बाँधा गया है। इन प्लेटों पर एट्रस्केन अक्षरों में लिखा गया है, और इनमें एक घोड़ा, घुड़सवार, एक सायरन, एक वीणा और सैनिकों को भी दरशाया गया है। यह पुस्तक बुल्गारिया के सोफिया स्थित राष्ट्रीय इतिहास के संग्रहालय में है। एट्रस्केन एक प्राचीन जाति थी, जो लिडिया से पलायन करके मध्य इटली में लगभग ३ हजार साल पहले बस गई थी— जो अब आधुनिक तुर्की है।
‘द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर’ दुनिया में टाइपराइटर पर छपी पहली किताब थी। १६९८ में चार्लस्टन साउथ कैरोलिना में पहली बार कोई पब्लिक लाइब्रेरी खुली। ४.९ करोड़ डॉलर में लियोनार्डो द विंची की लिखी द कोडेक्स लीसेस्टर साल १९९४ में बिकी सबसे महँगी किताब थी। अमेरिका की ‘द लाइब्रेरी आॅफ कांग्रेस’ में २.८ करोड़ किताबें हैं। यह लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। दुनियाभर में हर सेकंड ५७ किताबें बिकती हैं। दुनिया की पहली लाइब्रेरी प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता के राजा अश्शूरबनिपाल ने ६६८-६२७ ई.पू. में बनवाई थी। लाइब्रेरी में ३०,००० से ज्यादा मिट्टी की पियाँ और टुकड़े हैं, जिनमें ७वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर अब तक के सभी तरह के ग्रंथ मौजूद थे।
दुनिया की सबसे बड़ी किताब वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में है। १५०० किलोग्राम की यह किताब भगवान् स्वामीनारायण की शिक्षाओं का संग्रह है। यह किताब १०/७ फीट की है। इस किताब में ८५४ पेज हैं। किताब के पेज खास पेपर से बनाए गए हैं। दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी किताब, जिसका वजन १४२० किग्रा. है, उत्तरी हंगरी के छोटे से गाँव सिनपेत्री के रहने वाले बेला वर्गा ने अपने हाथों से एक किताब बनाई है। उनका दावा है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी किताब है।
दुनिया की सबसे छोटी किताब का नाम ‘Teeny Ted from Turnip Town’ है। यह किताब इतनी छोटी है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के देखना मुश्किल है। इसकी नाप-जोख केवल ०.०७ mm × ०.१ mm है, जो एक मोती के आकार से भी छोटा है। इस किताब को कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने २००७ में बनाया था। यह किताब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अद्भुत उदाहरण है। किताब में एक छोटे से खरगोश ‘टिनी टेड’ की मजेदार और दिलचस्प कहानी है, जो टर्निप टाउन में एक साहसिक यात्रा पर निकलता है। यह किताब कागज के बजाय सिलिकॉन क्रिस्टल पर लिखी गई है, जो इसके आकार और स्थायित्व को बनाए रखने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह किताब दुनिया की सबसे छोटी किताब के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दुनिया की सबसे मोटी किताब अगाथा क्रिस्टी की ‘मिस मारपेल कलेक्शन’ (Miss Marple Collection) है। ४,०३२ पन्ने वाली इस किताब का वजन करीब ८ किलोग्राम है।
हमारे देश में किताब लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगाल से १५५६ में मिशनरियों के साथ एक स्पेनिश जहाज पर एक प्रिंटिंग प्रेस भारत आया। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस १५५६ में ओल्ड गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया। इस प्रेस में छपने वाली पहली और सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक थी ‘कैटेसिमो दा डोट्रिना क्रिस्टा’। इसे फ्रांसिस जेवियर ने खुद लिखा था, लेकिन यह उनकी मृत्यु के पाँच साल बाद तक नहीं छपी थी। भारत में पहली किताब १७९४ में छपी अंग्रेजी की ‘The Travels of Dean Mahomet’ थी। यह किताब डीन महोमेद (Dean Mahomed) ने लिखी थी, जो पटना के थे। हिंदी में छपी पहली किताब १८०३ में ‘प्रेम सागर’ थी। इस पुस्तक के लेखक लालू लाल फारसी और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे।
हालाँकि ‘ऋग्वेद’ को हम अपनी पहली किताब मानते हैं। भारत में अध्यात्म और रहस्यमयी ज्ञान की खोज ऋग्वेद काल से ही हो रही है, जिसके चलते यहाँ ऐसे संत, दार्शनिक और लेखक हुए हैं, जिनके लिखे हुए का तोड़ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने जो लिख दिया, वह अमर हो गया। उनकी ही लिखी हुई बातों को दूसरी और १२वीं शताब्दी के बीच अरब, यूनान, रोम और चीन ले जाया गया, रूपांतरण किया गया और फिर उसे दुनिया के सामने नए सिरे से प्रस्तुत कर दिया गया। ईसा से सैकड़ों वर्ष पूर्व ‘महर्षि लगध’ ने वैदिक ज्योतिषशास्त्र के सबसे पुराने ग्रंथ ‘वेदांग ज्योतिष’ की रचना की थी। ऋग्वेद के आधार पर ही ज्ञान के अनन्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद की रचना हुई। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए हमारे मनीषियों ने ‘वेदांगों’ व ‘उपवेदों’ को लिपिबद्ध किया। वैदिक ज्ञान को सरल बनाने के लिए ‘शंकराचार्य’ ने अपने बाल्यकाल में ही ‘विवेकचूड़ामणि’ ग्रंथ लिख दिया। वेद व उपनिषद् के अध्ययन के बाद हमारे आचार्यों ने अपने ‘दर्शन’ की रचना की। वेदों की २८ हजार पांडुलिपियों को पुणे के ‘भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेटंर’ ने सहेजा है। जिनमें से ३० महत्त्वपूर्ण पांडुलिपियों को यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में भी शामिल किया है। ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ ने वर्ष २००७ में वेदों को संसार के स्मृति रजिस्टर में शामिल करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया था।
‘विलियम जोंस’ ने सन् १७७६ में ‘मनुस्मृति’ तथा १७८९ में कालीदास द्वारा रचित विश्वविख्यात नाटक ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आरटीएच ग्रिफिथ ने बनारस विश्वविद्यालय से संस्कृत में शिक्षा हासिल की तथा सन् १८७० में रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया। दाराशिकोह ने ५० से अधिक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाकर इसे ‘सीर ए अकबर’ (सबसे बड़ा रहस्य) का नाम देकर खाड़ी देशों में पहुँचा दिया था। योग के जनक ‘पतंजलि’ ऋषि द्वारा रचित ८४ अध्यायों के ग्रंथ ‘महाभाष्य व योगसूत्र’, कौटिल्य का ‘अर्थशास्त्र’, ‘विदुर नीति’, भृगुसंहिता व ‘पाणिनि’ द्वारा रचित विश्व की सबसे प्राचीन व्याकरण तथा भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सनातन संस्कृति के इस संस्कार के पुरोधा महर्षि ‘श्वेतकेतु’ थे। आधुनिक विज्ञान के कई सूत्र व सिद्धांत हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व वेदों व अन्य ग्रंथों में अंकित कर दिए थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लेकर पृथ्वी का भार तक वेदों में दर्ज है। वेदों में पृथ्वी को धरती माता कहा गया है। हाल ही में अमरीका की ‘यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर’ ने पृथ्वी पर शोध के बाद ‘अथर्ववेद’ में दर्ज उस पंक्ति को स्वीकार किया है, जिसमें पृथ्वी को एक ‘जीवित वस्तु’ बताया गया है। कुछ वर्ष पहले अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नासा’ ने महर्षि ‘भरद्वाज’ द्वारा रचित ‘यंत्र सर्वस्व’ ग्रंथ के भाग ‘विमान शास्त्र’ का अध्ययन किया था। अणु वैज्ञानिक ‘जॉन डॉल्टन’ ने ‘महर्षि कणाद’ को ही ‘परमाणु सिद्धांत’ का जनक माना था। महर्षि कणाद के ग्रंथ ‘वैशेषिक दर्शन’ तथा ‘बिजली सूत्र’ के जनक ‘अगस्त्य मुनि’ के ‘अगस्त्य संहिता’ ग्रंथ पर कई देशों के वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं। हमारे ऋषि-मुनियों को हजारों वर्ष पूर्व ९ ग्रहों, १२ राशियों व २७ नक्षत्रों के बारे में गहन जानकारी थी। ४ वेद, ४ उपवेद, १८ पुराण, १८ उपपुराण, ६ शास्त्र, ६ दर्शन, ६० नीतियाँ व १०८ उपनिषद् के अलावा वेदों का नेत्र ज्योतिष, खगोल तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की जानकारी से भरपूर लिखित भारतीय साहित्य का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
आठवीं से १२वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए ग्रंथ इनमें से प्रमुख हैं—वाग्भट्ट की ‘अष्टांग हृदय’, गोविंद भगवत्पाद की ‘रस हृदयतंत्र’ एवं ‘रसार्णव’, सोमदेव की ‘रसार्णवकल्प’ एवं ‘रसेंद्र चूणामणि’ तथा गोपालभट्ट की ‘रसेंद्रसार संग्रह’। कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों में—रसकल्प, रसरत्नसमुच्चय, रसजलनिधि, रसप्रकाश सुधाकर, रसेंद्रकल्पद्रुम, रसप्रदीप तथा रसमंगल। अश्वघोष, भास, भवभूति, बाणभट्ट, भारवि, माघ, श्रीहर्ष, शूद्रक और विशाखदत्त की पुस्तकें हैं।
अब कुछ रहस्यमयी किताब। लाल किताब भृगुसंहिता से कहीं अधिक रहस्यमयी ज्ञान है। माना जाता है कि लाल किताब के ज्ञान को सबसे पहले अरुणदेव ने खोजा था, जिसे ‘अरुणसंहिता’ कहा जाता है। फिर इस ज्ञान को रावण ने खोजा और इसके बारे में रावण ने लिखा था। फिर यह ज्ञान खो गया, लेकिन यह ज्ञान लोक-परंपराओं में जीवित रहा। रावण द्वारा रचित ‘रावण संहिता’ के बारे में कहा जाता है कि इसमें ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी हैं, जो कि अचूक मानी गई हैं। हालाँकि असली रावण संहिता के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरह लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती हैं, उसी तरह रावण संहिता के नाम पर नकली रावण संहिता ही आजकल मिलती है।
वैसे रावण ने जिन ग्रंथों की रचना की थी, उनमें ‘शिव तांडव स्तोत्र’ और ‘रावण संहिता’ प्रमुख हैं। रावण ने इसमें सूर्य के सारथी अरुण से यह ज्ञान प्राप्त किया था। रावण ने इस ज्ञान को ‘रावण संहिता’ नाम से लिखा था। पाँच सौ ईसा पूर्व पाणिनि ने दुनिया को पहला व्याकरण ग्रंथ ‘अष्टाध्यायी’ दिया। इसमें आठ अध्याय हैं, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या ३९९६ है। इन सभी सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्त होगी, वह दुनिया की अन्य किसी व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगा। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत ‘वार्तिक ग्रंथ’ है। इसी तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ पर विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा है। पतंजलि का योगसूत्र (१५० ईसा पूर्व) पढ़ने लायक ग्रंथ है, जिसमें योग की चर्चा है। संपूर्ण ग्रंथ योग के रहस्य को उजागर करता है। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा है।
उपनिषदों को वेदों का सार या निचोड़ कहा गया है। उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमयी बातें भी हैं, जिन्हें जान-समझकर आप हैरान रह जाएँगे। उपनिषद् १००८ से भी अधिक हैं। उनमें से भी १०८ महत्त्वपूर्ण हैं और उनमें से भी सबसे महत्त्वपूर्ण हैं—१. ईश, २. केन, ३. कठ, ४. प्रश्न, ५. मांडूक्य, ७. तैत्तिरीय, ८. ऐतरेय, ९. छांदोग्य, १०. वृहदारण्यक, ११. नृसिंह पर्व तापनी।
प्रारंभिक उपनिषदों का रचनाकाल १००० ईस्वी पूर्व से लेकर ३०० ईसा पूर्व तक माना गया है। कुछ परवर्ती उपनिषद्, जिन पर शंकर ने भाष्य किया, बौद्धकाल के पीछे के हैं और उनका रचनाकाल ४०० या ३०० ई.पू. का है। सबसे पुराने उपनिषद् वे हैं, जो गद्य में हैं। संस्कृत में लिखी गई २५ कथाओं का एक संग्रह है ‘वेताल पच्चीसी’। इसे विक्रम वेताल के नाम से जाना जाता है। विक्रम-वेताल की कहानी हम सबने बचपन में सुनी हैं। इसके रचयिता भवभूति ऊर्फ वेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के नौ रत्नों में से एक थे। इस किताब में लेखक ने एक वेताल (भूत समान) के माध्यम से राजा विक्रम की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया है। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है।
एक रहस्यमयी किताब है ‘विमान शास्त्र’। जिसके रचनाकार ऋषि भरद्वाज हैं। उन्होंने अपनी किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है, उसका प्रचलन आधुनिक युग में होने लगा है। ऋषि भरद्वाज ने ‘यंत्र-सर्वस्व’ नामक बृहद् ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने ‘विमान-शास्त्र’ के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है।
कामशास्त्र और कामसूत्र दोनों ही ग्रंथ रहस्य और विवादों से भरे हैं। कहते हैं कि नंदी ने भगवान् शंकर और पार्वती के पवित्र प्रेम के संवादों को सुनकर कामशास्त्र लिखा। नंदी नाम का बैल भगवान् शंकर का वाहन माना जाता है। कामशास्त्र तो प्रारंभ में अर्थशास्त्र और आचार शास्त्र का हिस्सा था। पुराण, स्मृतियों के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों का एक विशालकाय ग्रंथ बनाया। उस ग्रंथ का मंथन कर मनु ने एक पृथक् आचार शास्त्र बनाया, जो मनुसंहिता या धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा के ग्रंथ के आधार पर बृहस्पति ने ब्रार्हस्पत्यम् अर्थशास्त्र की रचना की। ब्रह्मा के ग्रंथ के आधार पर ही भगवान् शंकर के अनुचर नंदी ने एक हजार अध्यायों के कामशास्त्र की रचना की, ऐसा बताया जाता है।
इसके अलावा कामशास्त्र पर संस्कृत में अनंगरंग, कंदर्प चूड़ामणि, कुिनीमत, नागर सर्वस्व, पंचसायक, रतिकेलि कुतूहल, रति मंजरी, रति रहस्य, रतिरत्न प्रदीपिका, स्मरदीपिका, शृंगारमंजरी आदि कई ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्ति कुचिमार मंत्र, कामकलावाद तंत्र, काम प्रकाश, काम प्रदीप, काम कला विधि, काम प्रबोध, कामरत्न, कामसार, काम कौतुक, काम मंजरी, मदन संजीवनी, मदनार्णव, मनोदय, रति सर्वस्व, रतिसार, वाजीकरण तंत्र आदि संबंधित ग्रंथ हैं।
तंत्र शास्त्र पर भारत में हजारों प्राचीन किताबें मिल जाएँगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विज्ञान भैरव तंत्र की होती है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा, यह ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें शिव और पार्वती के बीच हुआ संवाद है, उसी तरह का जिस तरह अष्टावक्र और जनक के बीच हुआ था और जिस तरह श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था।
सामुद्रिक शास्त्र मुख, मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिककाल से ही प्रचलित है। ज्योतिष शास्त्र की भाँति सामुद्रिक शास्त्र का उद्भव भी ५००० वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। पराशर, व्यास, सूर्य, भरद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षियों ने इस विद्या की खोज की गरुड़ पुराण में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन है। यह एक रहस्यमयी शास्त्र है, जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोलकर रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान सामुद्रिक विद्या की एक शाखा मात्र है।
कहते हैं कि ईसापूर्व ४२३ में यूनानी विद्वान् अनेक्सागोरस यह शास्त्र पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों अनुसार हिपांजस को हर्गल की वेदी पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली, जो सिकंदर महान् को भेंट की गई थी। प्लेटो, अरिस्टॉटल, मेगनस, अगस्टस, पैराक्लीज तथा यूनान के अन्य दार्शनिक भारत के ज्योतिष और सामुद्रिक ज्ञान से परिचित थे।
प्राचीन भारत में नागार्जुन नाम के एक महान् रसायनशास्त्री हुए हैं। इनकी जन्मतिथि एवं जन्मस्थान के विषय में अलग-अलग मत हैं। रसायन शास्त्र में उनकी दो पुस्तकें ‘रस रत्नाकर’ और ‘रसेंद्र मंगल’ बहुत प्रसिद्ध है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें ‘कक्षपुटतंत्र’, ‘आरोग्य मंजरी’, ‘योग सार’ और ‘योगाष्टक’ हैं। रसरत्नाकर में इन्होंने रसायन के बारे में बहुत ही गूड़ रहस्यों को उजागर किया है। इसमें उन्होंने अयस्क सिनाबार से पारद को प्राप्त करने की आसवन विधि, रजत के धातुकर्म का वर्णन तथा वनस्पतियों से कई प्रकार के अम्ल और क्षार की प्राप्ति की भी विधियाँ वर्णित की हैं। इसके अतिरिक्त रसरत्नाकर में रस (पारे के योगिक) बनाने के प्रयोग दिए गए हैं। इसमें देश में धातुकर्म और कीमियागरी के स्तर का सर्वेक्षण भी दिया गया था। इस पुस्तक में चाँदी, सोना, टिन और ताँबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह कि इसमें सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐसी पुस्तक है, जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। इसे चाणक्य ने ‘कौटिल्य’ नाम से लिखा था। चाणक्य को तो सभी जानते हैं कि वे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट् अशोक को सिंहासन पर बिठाने वाले थे। चाणक्य के लिखे नीतिशस्त्र और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की आज भी विश्व प्रसिद्धि हैं। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष पर विष्णुगुप्त सिद्धांत और आयुर्वेद पर ‘वैद्य जीवन’ नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। इसी तरह हिमाचल के निरमंड क्षेत्र से २५० वर्ष पुरानी ‘पारद विज्ञान’ पुस्तक मिली है।
छपाई की उपलब्धि से दुनिया बदल गई। आज भारत की पुस्तकें दुनियाभर में छप रही हैं। अलग-अलग भाषाओं में अनूदित हो रही हैं। उन पर शोध हो रहे हैं। भारत के लेखक विश्व के अन्य देशों में रहकर भी अद्भुत लेखन के उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल रहे हैं। उसी प्रकार दुनियाभर का साहित्य, विज्ञान, कला, चिकित्सा या किसी भी विषय की पुस्तक आज भारत में उपलब्ध हैं या मँगाई जा सकती हैं। किताबों ने दुनिया को बदला है। दुनिया ने किताबों के सहारे बहुत कुछ सीखा है और उसके सीखने से नई चीजें तो बनी ही हैं, नई चीजों पर नई पुस्तकें भी बनी हैं। दरअसल किताब वह पद्धति है, जिसकी मदद से मनुष्य सीखता है, समझता है, कुछ नया या विशेष बनाता है और फिर उसे लिपिबद्ध करता है, किताब की शक्ल देता है, ताकि भविष्य में जब उस अनुसंधान से आगे जाना हो तो यह किताब नए सृजन का आधार बने।
किताबों का होना दरअसल मनुष्यता के सतत होने और रहने की कहानी है। इसलिए किताब जरूरी है। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि जिंदगी की किताब को और बेहतर बनाना है, किसी किताब की दुकान पर जाइए, किसी पुस्तक मेले में पहुँचिए, किसी लाइब्रेरी की बेंच को रूमाल से पोंछकर वहाँ बैठिए और इन्हें दोस्तों की तरह अपने घरों में रखिए।
आसावरी, जी-१८०, सेक्टर-४४
नोएडा-२०१०३०१
hemantmanusharma@gmail.com