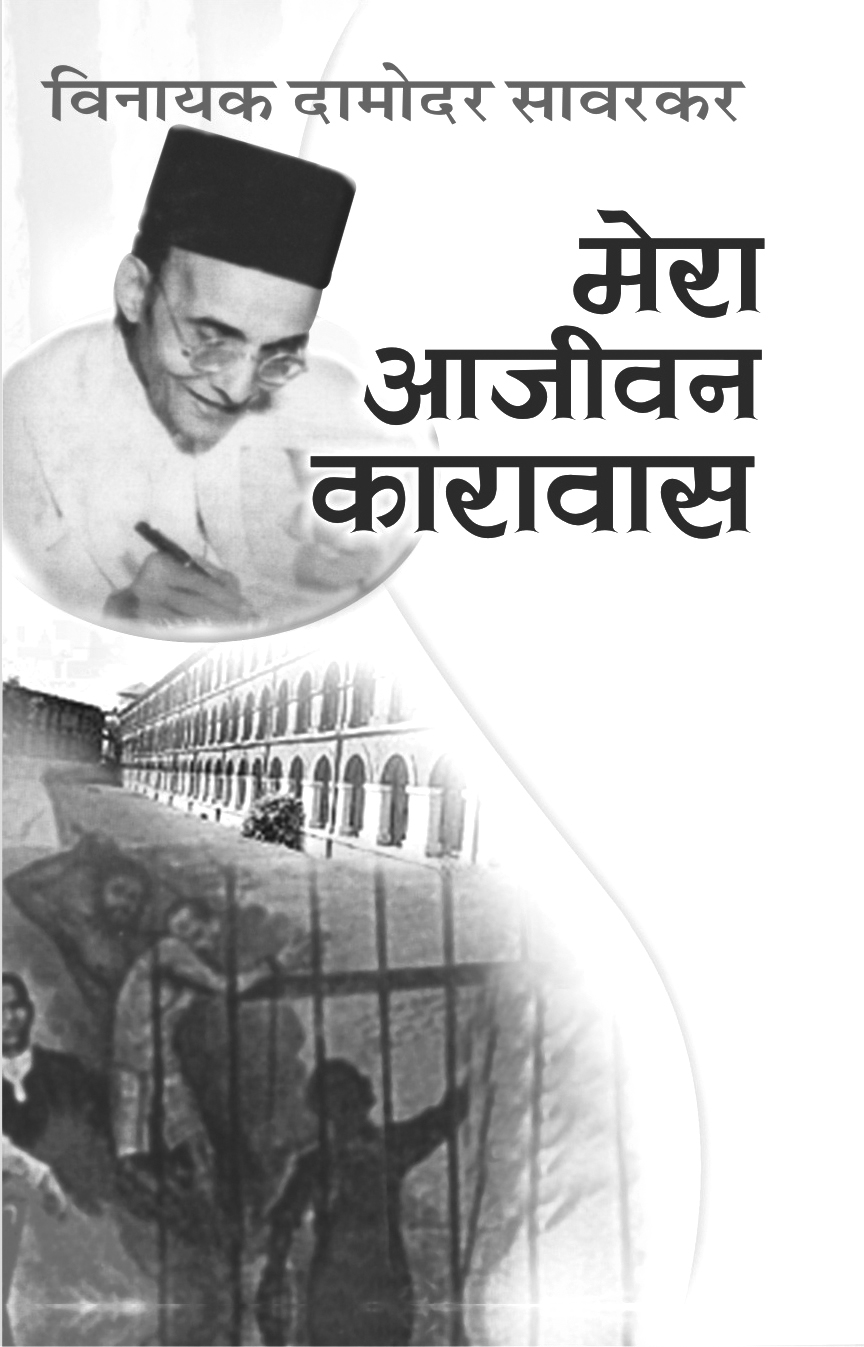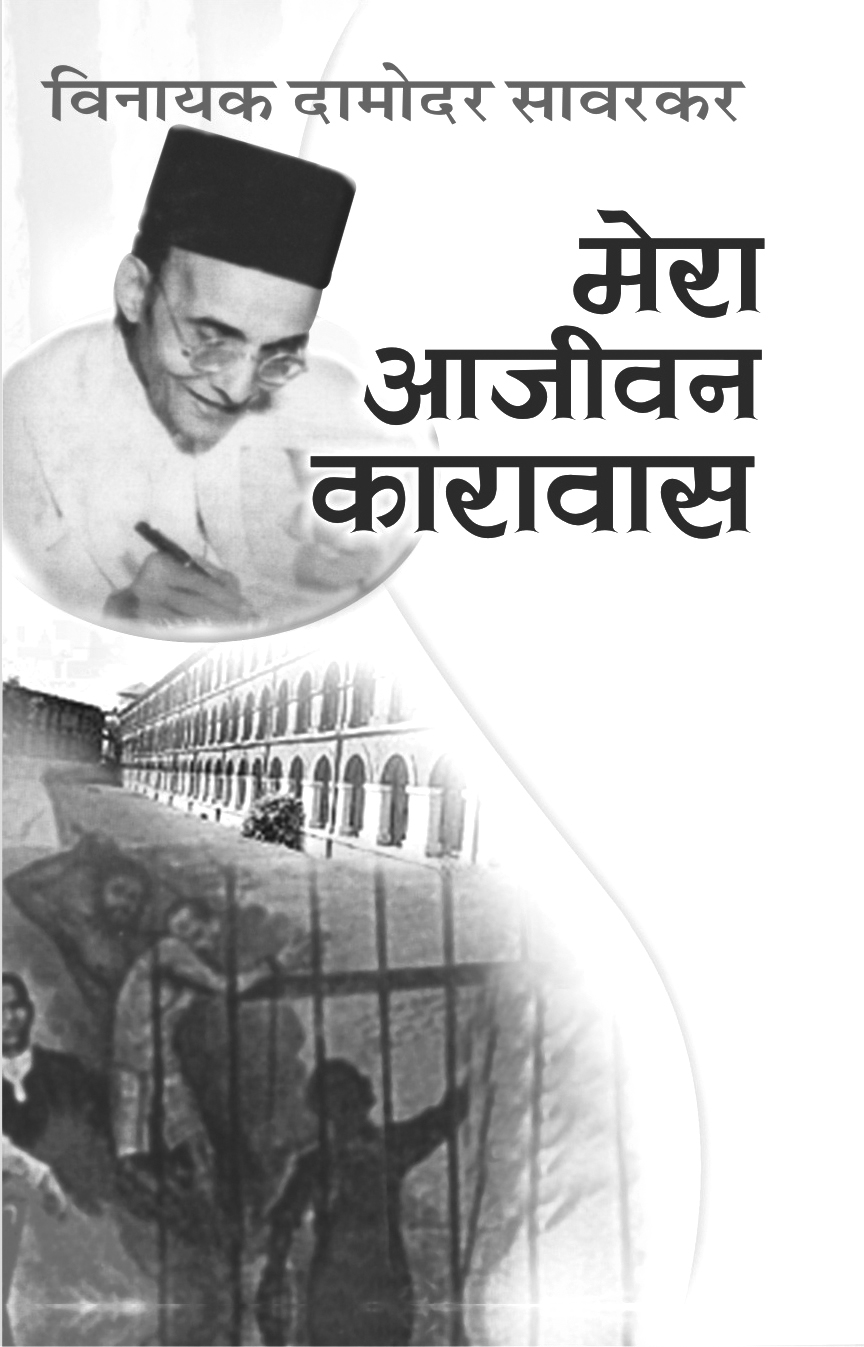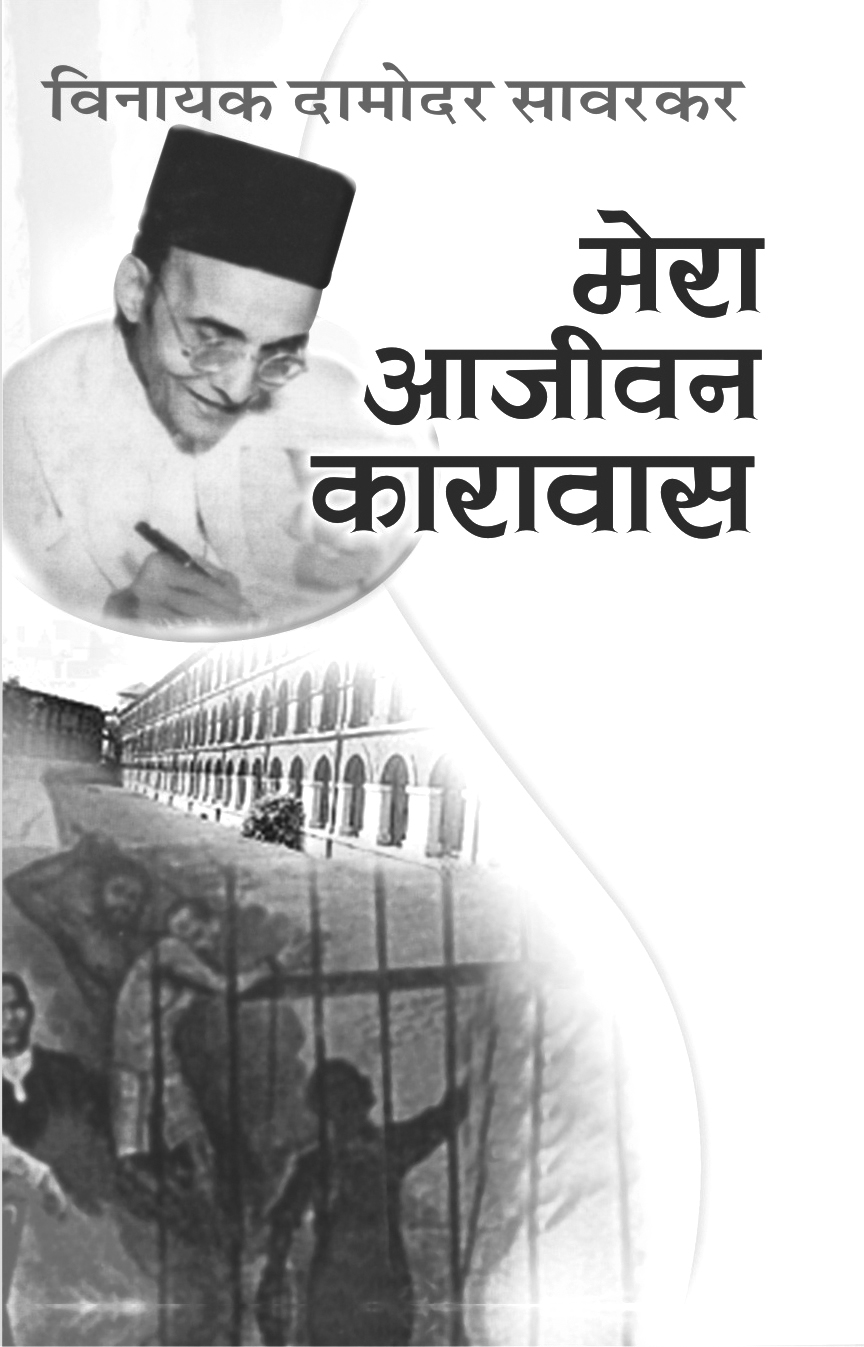
प्रकरण-११
मैंने लगभग एक महीना छिलका कूटने का काम किया। सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि मुझे कोल्हू कैसे नहीं दिया गया। इसपर कुछ आशावादियों ने कहा, ‘‘नहीं जी, बैरिस्टर बाबू को किस मुँह से कोल्हू का काम देंगे?’’ मैं उनसे कहता, ‘‘उसी मुँह से जिससे बैरिस्टर बाबू को कालेपानी भेेजकर, लँगोटी पहनाकर छिलका कुटवाया।’’ आखिर एक दिन सुपङ्क्षरटेंडेंट ने आकर मुझसे कहा, ‘‘कल से आपको कोल्हू पर जाना है। छिलका कूट-कूटकर अब आपके हाथ कठोर बन गए होंगे। अब और अधिक कठोर काम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।’’ बारी साहब ने हँसते हुए कहा, ‘‘अब आप ऊपरी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं।’’ उस दिन शाम के समय बारी साहब ने मुझे कचहरी में बुलाया। मुझसे हुए संभाषण से उन्हें ज्ञात हो चुका था कि राजबंदियों की हड़ताल से मेरी सहानुभूति थी और उस हड़ताल तथा निर्भीक आचरण की उद्ïदंड, अशिष्ट तथा मूर्खता के प्रतीक-रूप में निंदा करते उन राजबंदियों के मुख मेरी नीति के समर्थन से शांत हो गए थे। कुल मिलाकर ये वात्र्ताएँ बारी तक गुप्त रूप में नित्य पहुँच रही थीं, उससे यही संभावना दिख रही थी कि शीघ्र ही मैं उन ‘अशिष्ट बर्बरों’ का शिरोमणि बननेवाला हूँ। इसकी टोह लेने के लिए कि कहीं मैं कोल्हू पेरने के लिए मना तो नहीं कर रहा और ऐसा करने से परावृत्त करने के लिए बारी ने मुझे बुलावा भेजा था। बहुत देर तक गपशप लड़ाने के बाद अंत में उन्होंने कहा, ‘‘मैं क्या करूँ? ऊपर से मिले आदेश का मुझे पालन तो करना ही चाहिए। लिखित ऑर्डर आया है कि आपको कोल्हू ही दिया जाए। फिर भी मैंने इतना किया कि आपकी योग्यता के बारे में बताकर आपको सुपङ्क्षरटेंडेंट द्वारा केवल चौदह दिन ही कोल्हू का काम दिलवाया। अन्य बंदियों जैसा बार-बार नहीं दिलवाऊँगा। हाँ, आप मना मत कीजिए। जाइए, खड़े हो जाइए। मैं यथासंभव आपकी सहायता करूँगा। परंतु दंड मत भुगतिएगा।’’ मैंने कहा, ‘‘पहले ही हमारा जीवन मटियामेट हो चुका है। फिर बिना किसी कारण और अत्याचार सहने का हमें शौक थोड़े ही चढ़ा है? मैं सदैव यथासंभव काम करता ही रहूँगा।’’ बारी ने जैसे दयाभाव से कहा, ‘‘देखो भाई, मैं आपके लिए कहता हूँ। पचास बरस का दंड जो है। मेरा तो दिल फट जाता है। इसीलिए तो कहता हूँ, अन्यों का चाहे जो हो, आप सबसे अलग ही रहना।’’ मेरा मनोधैर्य भंग करने के लिए बारी जैसे-जैसे पचास बरस के दंड का बार-बार स्मरण दिलाता गया, वैसे ही उसकी नीति का विपरीत परिणाम होता गया और उन शब्दों के अर्थ से मैं इतना परिचित हो गया, जैसे तोपखाने के फौजी तोपखाने की आवाज से परिचित हो जाते हैं। उसके गर्जन से काँपना ही बंद हो गया। दूसरे दिन प्रात:काल से ही मुझे कोल्हू के काम पर लगा दिया गया।
तेलघानी में
मैं जिस सात नंबर में रहता था, वहाँ से उस कोल्हू का काम छठवें भाग में था। अत: मुझे प्रात:काल ही उधर ले जाया गया। उस विभाग को बदलने से मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि वे राजबंदी, जो उधर रहते थे, अब मुझे दिखाई देने लगे और कभी-कभी मुझसे बात भी करने लगे। काम पर जाते ही देखा, बर्मा देश के एक राजबंदी को भी मेरे कोल्हू में ही जोता गया था। मुझे कहा गया कि यह आपकी सहायता करेगा, परंतु आपको लगातार कोल्हू घुमाते रहना होगा। तनिक भी बैठना नहीं चाहिए। अन्य राजबंदियों की तुलना में मुझे यह सुविधा मिली थी, तथापि वह कोल्हू के काम की सुविधा थी। सुविधा घटाकर भी शेष जो कष्ट बचा वह उसे, जिसे किसी भी तरह कष्टों का अभ्यास नहीं, सीधा करने के लिए पर्याप्त था। लँगोटी पहनकर प्रात: दस बजे तक काम करो, बिना रुके गोल-गोल घूमने से सिर चकराता था। अंग-प्रत्यंग ढीले पड़ जाते थे, शरीर इतना थक जाता कि रात में तख्ते पर लेटते ही नींद आने के बदले करवट बदलते हुए रात काटनी पड़ती थी। दूसरे दिन प्रात:काल पुन: कोल्हू के सामने जा पहुँचता। इस तरह छह-सात दिन गुजारे। तब तक काम पूरा कहाँ होता था? एक दिन बारी आया और इठलाते हुए कहने लगा, ‘‘यह देखिए, आपके पासवाली कोठरी का बंदी दो बजे पूरा तीस पौंड तेल तौलकर देता है और आप शाम तक कोल्हू चलाकर भी पौंड-दो पौंड ही निकालते हैं, इसपर आपको शर्म आनी चाहिए।’’ मैं बोला, ‘‘शर्म तो तब आती जब मैं भी बचपन से ही उसके समान कुलीगिरी करने का आदी होता। यदि आप उसे एक घंटे के अंदर एक सुनीत (सॉनेट) रचने के लिए कहें तो क्या वह रच सकेगा? मैं आपको आधे घंटे के अंदर रचना करके दिखाता हूँ। परंतु इसलिए आप यदि उस श्रमिक को ताना मारें कि ‘अरे, तुम सॉनेट की रचना शीघ्रतापूर्वक नहीं कर सके, इसके लिए तुम्हें लाज आनी चाहिए’ तब क्या कहेगा वह, ‘बचपन से कविता करना मुझे किसी ने सिखाया नहीं।’ अपने कार्यालय में आप अर्ध शिक्षित किसानादि चोर-डाकुओं को लिखने का काम देते हैं। उन्हें जैसे हमारे सरीखे त्वरित अंग्रेजी नहीं बोल पाने पर लज्जा आने का कोई कारण नहीं, उसी तरह हम उनके जैसा शारीरिक श्रम झेलने में एकदम असमर्थ हैं और इस कारण हमारा लज्जित होना अनावश्यक है। उसे भी लज्जित नहीं होना चाहिए जो सॉनेट की रचना नहीं कर सकता। वास्तव में लज्जित उन्हें होना चाहिए जो बुद्धिजीवी वर्ग को कोल्हू में जोतते हैं, श्रमजीवी अनपढ़ों को क्लर्क की जगहों पर रखते हैं और अपने दोनों काम बिगाड़ते हैं।’’
उदार मित्रों का सहयोग
कोल्हू पेरते समय राजबंदियों में से एक-दो बंदी, जो उधर गुप्त रूप से आ सकते थे, आकर मेरी सहायता करते। इतना ही नहीं, मेरे लगातार ‘ना-नु’ करने के बाद भी और उनके दु:ख, कष्ट, मुझसे अधिक होते हुए भी राजबंदियों में से कई जन मुझे अपने कपड़े भी नहीं धोने देते, न ही अपना थाल-कटोरा माँजने देेते। मेरे कपड़े धोने तथा बरतन माँजने के संबंध में कई बार पेटी अफसर तथा वॉर्डर लोग उनसे धक्का-मुक्की करते, गालियाँ देते; परंतु इस तरह के कष्ट झेलकर भी ये उदार तथा स्नेही लोग मेरे काम करते रहते। उनको रोकने का मैंने बहुत प्रयास किया। कभी-कभी उनके कपड़े गुपचुप धो डाले। जब उन्हें पता चला तब उनके मन को भारी ठेस पहुँची। इतनी कि वे हाथ जोडक़र गिड़गिड़ाते हुए मुझसे प्रार्थना करने लगे। जब मैंने इस बात का अनुभव किया कि यदि मैंने उनकी सहायता अस्वीकार की तो सहायता देने में जितना कष्ट होता, उससे कहीं अधिक उन्हें मन:क्लेश होगा। तब मैंने निश्चय किया कि इन उदार एवं निरपेक्ष मित्रों को अपना काम करने दिया जाए। साधारणतया प्राय: सभी राजबंदियों की मुझपर इसी तरह निश्छल भक्ति और प्रगाढ़ स्नेह है, इसका अनुभव मैंने कर लिया। कभी-कभी तो उनमें मेरे कपड़े धोने तथा मेरी सेवा करने के लिए होड़ लगती और मनमुटाव भी हो जाता। तब मुझे बारी-बारी से अलग-अलग मित्रों को अपने कपड़े धोने के लिए देने पड़ते। उन लोगों की इस महानता तथा स्नेह के लिए मैं आज भी उनका कृतज्ञ हूँ। इसी प्रसंग में उन साधारण बंदियों ने भी, जो राजबंदी नहीं थे, हमें बिन माँगा जो सहयोग आखिरी दम तक दिया और हमारे शब्दों को सर-आँखों पर रखते गए उन्हें भी सार्वजनिक धन्यवाद देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। मनोरंजक होते हुए भी विस्तार भय से यहाँ उन अनेक प्रसंगों का वर्णन करना असंभव है। केवल एक बार और संगठित रूप से उनके प्रति कृतज्ञता ही प्रदर्शित की जा सकती है।
मानसिक विद्रोह
किसी से चर्चा करनी नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, परंतु कोल्हू चलाते-चलाते पसीने से नहाए शरीर पर उड़ रही वह बुकनी (पीसकर निचोड़ा हुआ भूसा) और सारा कचरा चिपका हुआ, गँदला, नंग-धड़ंग शरीर देखकर मन बार-बार विद्रोह कर उठता। अपने आपसे घिन आती। अरे, इस तरह का दु:ख झेल क्यों रहे हो? तुम्हारी इस देह तथा कर्तृत्व का राष्ट्रों के उदयार्थ उपयोग होना चाहिए। वह अब माटीमोल हो गया है। फिर इस अँधेरे में ही इतने सारे कष्ट सहते क्यों सड़ रहे हो? इसका तुम्हारे कार्य के लिए, तुम्हारी मातृभूमि के उद्धारार्थ कौड़ी भर उपयोग नहीं है। उधर तुम पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में एक अक्षर का भी पता नहीं चल रहा होगा, फिर नैतिक परिणाम तो दूर की बात है। इस तरह से तुम न कार्य के लिए और न ही अपने लिए उपयुक्त हो। इतना ही नहीं, वह कष्टप्रद भी हो रहा है। ऐसा जीवन तुम व्यर्थ ही क्यों धारण कर रहे हो। बस जो उपयोग होना था, सो हो चुका। अब चलो उठो, रस्सी के एक ही झटके से कर डालो इस जीवन का अंत! तुम्हारी कर्तृत्व-शक्ति के मेरुदंड का निर्माण इसलिए हुआ था कि उसका समुद्रमंथनार्थ उपयोग हो, उसे इस य:कश्चित्ï बटलोई के चुल्लू भर छाछ मथने के काम में जुटाकर उसका अनादर क्यों कर रहे हो? चित्त पुन:-पुन: कहता, ‘अब जीना व्यर्थ, अब आत्मघात ही आत्मसम्मान सिद्ध होगा।’ नोवालिस आदि कई नीति विशारदों का और ऐतिहासिक उदाहरणों का स्मरण होने लगा, जिन्होंने प्रसंगवश आत्मघात को आत्मकर्तव्य सिद्ध किया था।
एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में कोल्हू चलाते समय मैं हाँफने लगा; ऐसा लगा, चक्कर आ रहा है। मैं धम्म से नीचे बैठ गया। अत्यधिक श्रम के कारण अँतडिय़ाँ ऐंठने लगीं। पेट पकडक़र दीवार से सिर टिकाया, आँखें मूँद लीं और तभी उसी जगह गहरी नींद आ गई। इतनी गहरी कि जब चौंककर आँख खुली तब दिशा-विदिशा, स्थल-काल किसी का भी चार-पाँच मिनट तक भान नहीं हो रहा था। इस तरह शांत, शून्य, निर्विकार, सुखद अवस्था में ऐसे पड़ा रह गया जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मेरी चेतना लौट आई। एक-एक वस्तु दिखाई देने लगी, उसके अर्थ का आकलन होने लगा। अत: पुन: काम में जुट गया। परंतु मन सतत एकतारा छेडऩे लगा, यह अंतिम कार्य संपन्न क्यों नहीं होने देता? थोड़ी देर पहले जो शून्यवत्ï हो गया था, वही मृत्यु है। रस्सी के एक टुकड़े से, जिसके सहारे रातों में सैकड़ों बंदी पोर्ट ब्लेअर में मृत्यु को पार करके गए, उस डोर का गले में फंदा डालो और कर डालो इस यंत्रणा का अंत।
आत्महत्या का आकर्षण
उस आत्महत्या का आकर्षण मुझे सतत खींच रहा था। थोड़ी देर पहले जो शून्यावस्था थी, वही है मृत्यु—मरण। वह तो निस्संदेह इस जीवन से मधुर है। मुझे दो-चार बार अपनी निर्वासन की यातनाएँ असहनीय लगीं और आत्महत्या आकर्षक प्रतीत होने लगी थी। एक बार तब, जब मैं मार्सेलिस से पुन: पकड़े जाने के बाद एडऩ के आस-पास भयानक गरमी में तथा यंत्रणाओं में बंद किया गया था। दूसरी बार तब, जब इस कोल्हू पेरने में चक्कर आ गया था। दोनों बार मन तथा बुद्धि का प्रबल टकराव होते-होते बुद्धि के लगभग चारों खाने चित होने की स्थिति बन गई थी और एक-दो बार तो वह प्रसंग पुन: आनेवाला था। उस रात कोठरी की जिन सलाखों से लटककर प्राय: बंदी स्वयं फाँसी लगा लेते थे, उस खिडक़ी की ओर लुभावनी दृष्टि से मैंने चार-पाँच बार तो देखा ही होगा। बुद्धि और मन का संवाद मैं तटस्थतापूर्वक सुन रहा था, जिसे आगे चलकर मैंने एक कविता में ग्रंथित किया है। बार-बार मन के इस तर्क को विवेक उत्तर देता, ‘बावले, यह तुम्हारा अहंकार है। मान लो, तुम्हारा कर्तृत्व, कर्तव्य, पराक्रम एक यंत्र है, जो ऐसी प्रचंड गति प्रदान करने की क्षमता रखता है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र का उद्धार होगा, हो सकता है, भला अब उसका क्या? उसका उचित तथा यथाप्रमाण उपयोग नहीं होता, यह एक तरह से सत्य है। परंतु इस तरह जहाँ अन्य भारी-भरकम यंत्र चकनाचूर हो जाते हैं वहाँ इसलिए कि गुप्त, अज्ञात यातनाओं की मार सहने के लिए उपयुक्त हो, इस कार्य को करवाने के लिए यह कर्तृत्व शक्ति का यंत्र नहीं बनाया, यह कैसे कह सकते हैं? राष्ट्रोद्धार की मुठभेड़ों में सैकड़ों महत्त्वपूर्ण चौकियों पर लडऩा पड़ता है और उसमें बंदीगृह का मोर्चा सबसे कठिन परंतु अत्यावश्यक होता है। फिर वह लडऩे की तुम्हारी योजना बनी है, यह क्या उस कर्तव्य का कम गौरव है?’
‘और किस पराक्रम की बात कर रहे हो? तेरा, इस अखिल मनुष्यजाति का ही नहीं अपितु इस सूर्य का भी इस प्रचंड विश्व की उथल-पुथल में वास्तव में अणुमात्र भी महत्त्व है क्या? साबुन के झाग के गुब्बारे सदृश वह अब अपनी ही महत्ता के अभिमान से फूला उड़ता दिखाई दे रहा है। परंतु एक क्षणार्ध में विश्व की मूल शक्ति कोई दूसरा हँसता-खेलता गुब्बारा दे मारे तो वह पहला फुस से नष्ट हो जाएगा, तथापि विश्व उसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। अत: विवेक से काम लो। सापेक्ष रूप में जो कर्तृत्व है, उसकी खरी कसौटी यहीं पर है। वही सच्चा देशसेवक है जो इस कारागृह में देशसेवा करेगा। जो देशोद्धार मूल्य दिए बिना होगा ही नहीं, वह कारापीडऩ का मूल्य चुकाना है, जीवन अकारथ जाना नहीं है। कीर्ति का, लौकिक मन का लालच उसमें नहीं है। परंतु इसीलिए वह अधिक अव्यर्थ है और...’
यदि मरना है तो
‘तो फिर ऐसे क्यों मर रहे हो? तुम्हारे द्वारा सही गई यातनाओं का परिणाम देश के लिए होगा ही होगा। परंतु यदि तुम्हारा इसपर विश्वास न हो तो यह समाचार भी देश तक नहीं पहुँचेगा। फिर उसका नैतिक परिणाम भला कहाँ से होगा? फिर व्यर्थ कष्ट किसलिए? उनके लिए अपने हाथों से अपने पक्ष की हानि तथा पराजय क्यों बढ़ा रहे हो? यदि मरना ही है तो उस सेना का कुछ कार्य करके मरो जिसके तुम एक सैनिक हो। फाँसी पर लटककर नहीं...अपनी एक जान के लिए...इस तरह मरो।
बुद्धि का यह अंतिम कारण जान हथेली पर लिये उस अवस्था में स्वीकार किया। मन स्थिर हो गया। यही ठाणे के कारागार में भी किया था। उसका स्मरण हो आया। उस दिन से पुन: मैं एक बार आत्महत्या के कगार पर जाकर खड़ा हो गया था, रत्नागिरि की जेल में। परंतु वह आगे की बात है।
मरेंगे तो वैसे ही मरेंगे
इस तरह के कृत-निश्चय में रात व्यतीत हो गई। इतना ही नहीं, उपर्युक्त तर्क का उपयोग करके और इस तरह उपदेश करते हुए कि यदि किसी को भी मरना है तो...इसी तरह मरे, यही अंगीकृत व्रतार्थ कर्तव्य है। मैंने अंदमान के उस कारागार के उन सैकड़ों सहभागी राजबंदियों में से अनेक को कई बार आत्महत्या के कगार से हाथ पकडक़र वापस लौटाया है।
कोल्हू पर काम करते समय भारी शारीरिक एवं मानसिक श्रम होते हुए इसकी थोड़ी सी भरपाई करनेवाली एक संधि मिलती थी। वह थी उन राजबंदियों से थोड़ी सी बोलचाल की सुविधा, जो इस कोल्हू पर काम करते थे। आते-जाते अधिकारियों की दृष्टि बचाकर अथवा किसी समझदार या दयालु पहरेदार या सिपाही की कृपा से वे राजबंदी मेरे पास आते। यथासंभव मुझसे बतियाते। प्राय: सायंकाल पाँच बजे के आस-पास भोजन की धाँधली में जब सभी व्यस्त होते तब उस क्रमांक के हौज की ओट में हमारा अड्ïडा जमता। एक पहरा देता, शेष जन बातें करते। उस समय जिस कार्य के अनवरत चिंतनवश चित्त ने सभी ऐहिक सुखों को लात मारी थी, उस उदात्त कार्य की थोड़ी देर खुलकर चर्चा करना संभव होने से मन पुन: चेतना और उत्साह से भर जाता। सोया हुआ तेज पुन: जाग उठता। जो अपमान सहा था, वह सम्मान प्रतीत होता। भोगी हुई यातनाएँ अकिंचन लगतीं। पुन: यह निश्चय दृढ़ होता कि भविष्य में जो यातनाएँ भुगतनी हैं वे भी कर्तव्य ही हैं। ये चंद घडिय़ाँ उस कोल्हू के कठोर अभिशाप में वरदान समान ही थीं।
उस समय मैंने देखा कि उधर आए हुए राजबंदियों में प्राय: मेरे जैसे ही पच्चीस के आस-पास की आयु के थे। उनकी शिक्षा अधूरी थी। राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि आवश्यक विषयों का उन्हें अत्यंत कम ज्ञान हुआ था और यह स्वाभाविक ही था। तथापि मुझे कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इस कारण उनके उत्कृष्ट स्वदेश-प्रेम अथवा स्वार्थ-त्याग में रत्ती भर भी कमी आई है। इतना ही नहीं, यह देखकर कि अपनी इस आयु में वे मात्र जन्मजात परोपकारी बुद्धि तथा उदार भावना से प्रेरित होकर इस उद्ïदेश्य से इतने भारी कष्ट उठा रहे हैं, मेरा मन उनके प्रति आदर से भर जाता। न्यूनता बस इतनी ही थी कि जिस कार्य को उन्होंने इतने स्वाभाविक धैर्य से स्वीकार किया था, उस कार्य तथा उनकी उन उदार भावनाओं को अत्यंत आवश्यक शिक्षा, ज्ञान तथा विचारों का साथ मिलता तो सोने में सुगंध हो जाती और उस महत्कार्य को संपन्न करने के लिए वे पहले से अधिक सक्षम होते। अत: वे उसके लिए यत्नशील बने, एतदर्थ मैं उन्हें उन कमियों का एहसास दिलाकर उनमें वैसी इच्छा उत्पन्न करने का प्रयास करता। मुझे जब से कोल्हू के काम में लगाया गया तभी से उन प्रयत्नों का श्रीगणेश हुआ था। कई लोगों को, जो वहाँ आए हुए थे, ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अपना जीवन अकारथ गया। उन्हें उस उदासीनता तथा हतबलता के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मैं उन्हें इतिहास के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता। उन लोगों की शंकाओं के निवारण का प्रयास करता, जिन्हें इसका बोध नहीं हुआ था कि कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है। जो केवल समाज के राजनीतिक बवंडर के साथ इसमें फँस गए थे, उन्हें यह युक्तिपूर्वक समझाकर कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, वह नैतिक दृष्टि से कर्तव्य था अथवा अकर्तव्य, मैं इस प्रयास में रहता कि उनकी पूर्वकालीन क्षणिक उत्तेजना एक निश्चित निश्चय में परिणत हो, जो पूरे जीवन टिक सके। दिन भर अत्यंत कष्टप्रद, गंदगी से भरपूर, अपमानजनक उस कोल्हू के काम से थके-माँदे वे राजबंदी उस हौज पर घड़ी भर को गुपचुप इकट्ïठा होते और इस तरह के उदात्त संवाद करते राष्ट्रीय सुख-सपने सँजोते जब तन्मय हो जाते तब उनके मनोधैर्य की धार, जो दिन भर की यातनाओं के आघात सहते-सहते भोथरी हो जाती थी, पुन: पैनी हो जाती। उनके मुख पर नवतेज दमकता और उठते समय हर्ष तथा प्रेमपूर्वक एक-दूसरे से विदा लेकर वे भारतीय नवयुवक अपनी-अपनी चाली में बंद होने चले जाते।
अंदमान में संगठन और प्रचार
प्रकरण-१२
कोल्हू पर काम करते-करते मैं केवल राजबंदियों की स्थिति ही आजमा सका, ऐसा नहीं। थोड़ा-बहुत, कुल मिलाकर अंदमान की सारी स्थिति का आकलन मुझे होने लगा। बाहर के जिन लोगों के मन में हजार आपत्तियों के बाद भी मेरे प्रति जो आदर- भाव तथा प्रेम था, वे हाथ पर हाथ धरे न बैठते, मेरे साथ कुछ-न-कुछ संबंध जोडऩे का प्रयास करते रहे। इस अवस्था से मुझे दिखाई दिया कि प्रयास करने से यहाँ भी कुछ कार्यों में सफलता मिल सकती है, अत: थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो, इस कारावास से ही प्रारंभ करें।
अंदमान में संगठन
कार्य का प्रसार करना संभव है और यदि संभव है तो कम ही सही, पर संगठन करना हमारा कर्तव्य है। कारावास की यातनाएँ भोगना तथा एकांत बंदीवासजन्य कर्मशून्यता का असह्यï भार उठाकर निष्क्रिय खड़े रहने का एक कर्तव्य तो हम कर ही रहे थे। उसके साथ-साथ यदि कार्य प्रचार का और इस द्वीपांतर में जहाँ-जहाँ निर्वासित होंगे वहाँ-वहाँ भी जातीय चैतन्य का संचार करने का सक्रिय कार्य भी थोड़ा-बहुत कर सकें, तो उसके द्वारा मातृभूमि की दोहरी सेवा करने का पुण्य क्यों न सिद्ध किया जाए। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर अंदमान से प्रचार कार्य प्रारंभ करने का निश्चय किया।
राजबंदियों का शिक्षण
सर्वप्रथम राजबंदियों का शिक्षण कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया। इस एक पखवाड़े में ही बंदियों में से जो लोग बवंडर में ऊपरी तौर पर आने के कारण इस आंदोलन के सर्वथा अनुकूल नहीं थे, प्रथमत: उनके गले में यह बात उतारकर इस आंदोलन का अंतरंग विवेचन किया। उन्हें अपना बनाने के लिए दिए गए कोल्हू का कठोर काम करते-करते ही उन राजबंदियों में से दो युवकों को संगठन के कार्य में सम्मिलित होने के लिए शपथबद्ध कराने का खलबली मचानेवाला कार्य किया।
अंदमान के संगठन के प्रयत्नों का आरंभ यही से है। इसका संपूर्ण वर्णन करना संभव नहीं कि उसका कार्य विकास आगे चलकर किस तरह हुआ। अंशत: जो बताना संभव है, वह आगे क्रमश: बताऊँगा।
चौदह दिनों के पश्चात्ï मुझे कोल्हू से हटाया गया और रस्सी बटने का काम दिया गया। यह काम कारागृह के अन्य शारीरिक कार्यों से अधिक सहज था और इसीलिए वह मिलना अहोभाग्य समझा जाता। कुछ दिनों के अभ्यास से रस्सा बटने का काम आने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ, अल्प मात्रा में ही क्यों न हो, शारीरिक यातनाओं के चंगुल से तो मुक्ति मिली। इसी समय मुझे जिस सात नंबर की चाली में बंद रखा गया था उसमें निरुपाय हो चार राजबंदियों को रहने की अनुमति दी गई। हाँ, इसलिए कि अन्य कोई चारा नहीं था, क्योंकि अंतत: यह उनकी नीति तो थी कि यथासंभव मेरा और अन्य राजबंदियों का संपर्क न हो। परंतु सातवें विभाग में उन बंदियों को रखना अनिवार्य ही होता है, जिन्हें संपूर्ण बंदीगृह में बाँटकर भी स्थान नहीं मिलता। कभी-कभी तो प्रत्यक्ष बारी ने और एक दो-बार सुपङ्क्षरटेंडेंट ने भी मुझसे स्पष्ट ही कहा, ‘‘आपके विभाग में जो राजबंदी होते हैं, उन्हें यदि ढील देंगे तो आपको भी शिक्षित राजबंदी की संगत का लाभ प्राप्त होगा।’’ कोई भी नया राजबंदी आने से उसे प्राय: उन राजबंदियों की संगत में रखा जाता जो पालतू बन गए हैं। तथापि किसी भी राजबंदी को सतत एक ही विभाग में और एक ही संघ में रखना सुरक्षित न समझते हुए एक महीने के पश्चात्ï उसके रहने की कोठरियाँ बदल दी जाती थीं।
बंदीगृह में उत्सव
यह बदली का दिवस माना जाता था, क्योंकि उस बदली के बहाने कोठरी से बाहर निकलने पर लगभग आधा दिन तो उस धाँधली में निकल ही जाता। दूसरी बात, इस कारण जेल का चक्कर लगाना पड़ता। एक विभाग से दूसरी ओर जाते-जाते और उस योग से प्राय: राजबंदियों से दृष्टि-भेंट ही क्यों न हो, हो तो जाती। अवसर मिला तो जाते-जाते दो-चार बातें भी संभव होतीं और अंतिम आनंद का कारण यह कि राजबंदियों से परिचय तथा संपत्ति का लाभ उस बदली के अवसर द्वारा प्राप्त होता। यद्यपि मुझे यथासंभव सात नंबर के कक्ष में ही बंद रखा गया था और प्राय: अन्य राजबंदी मेरे पास नहीं भेजे जाते थे, तथापि मैं भी इसे उत्सव का दिवस ही समझता, क्योंकि उस दिन बदली के बहाने इस विभाग से उस विभाग में आते-जाते दूर से मेरे ज्येष्ठ बंधु से दृष्टि-भेंट हो जाती। कभी-कभी पूर्व साँठगाँठ में कदाचित्ï सफलता मिली तो गुपचुप बातें करना भी संभव होता।
एक महीने-दो महीने के स्थान परिवर्तन के कारण नए तथा अन्य राजबंदियों से जिस तरह बात करने का अवसर प्राप्त होता, उसी तरह आपसी बातचीत की और दो सुविधाएँ इस कारागृह में प्राप्ïत होतीं। वे थीं—रहने की कोठरी के ऊपर की खिडक़ी और बिलकुल भूमि से लगी हुई जाली। कारागृह के सातों विभाग फूल की पंखुडिय़ों की तरह एक केंद्र से निकलकर फैले हुए होने के कारण प्रत्येक विभाग का आँगन अगले विभाग की पीठ से सटा हुआ था। अत: प्रत्येक विभाग की इमारत से पिछवाड़े के विभाग से और आँगन से सामने के विभाग में खिडक़ी पर चढ़े हुए मनुष्य से बात करना संभव होता, परंतु यह कार्य बहुत संकट का था।
(प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित वीर सावरकर की आत्मकथा ‘मेरा आजीवन कारावास’ से साभार)