RNI NO - 62112/95
ISSN - 2455-1171
मंदिर की देहरी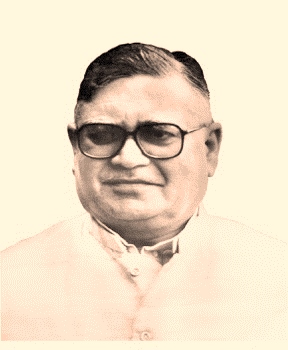
दंडवत् देते-देते महादे की छाती छिल आई थी, लेकिन उसके जीवन का यह क्रम था, जिसे वह किसी प्रकार तोड़ना नहीं चाहता था। आज बीस वर्षों से लगातार हर चैत और कार्तिक में पड़नेवाले छठ व्रत के समय वह देव के मेले में आता, भोर का तारा आकाश में देखकर वह सूर्यकुंड में स्नान कर गीली धोती पहने कुंड की सीढि़यों से ही दंडवत् देना शुरू करता और सूर्य मंदिर की देहरी पर जाकर, भीड़ से अलग हटकर आधा घंटे के करीब आँखें बंद किए ध्यानमग्न भगवान् भास्कर को समर्पित वाक्य गुनगुनाता रहता और फिर हर मूर्ति, सीढ़ी, दरवाजे को मस्तक नवाता, हर घड़ी-घंटे को बजाकर फिर किसी कुएँ पर जाकर स्नान करता। पिछले बीस वर्षों से उसके जीवन के इन क्रमों में कभी कोई व्यवधान नहीं आया था और उसका मानना था कि बीस साल की उम्र से, जब से उसने छठ के समय से भगवान् भास्कर को दंडवत् देना शुरू किया, सूर्यकुंड में स्नान और सूर्य-मंदिर में दर्शन प्रारंभ किया, तभी से उसके जीवन का स्वर्णिम-विहान शुरू हुआ। बुधनी-सी पत्नी मिली, दो बैलों की खेती शुरू हो गई, सोने-सा लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम पंडितजी के अनुसार उसने भास्कर रखा। दूसरे किसानों के खेतों में जहाँ पानी नहीं निकलता था, उसके खेतों में तीन पोरसे में ही लबालब पानी निकल आया और सालों भर फसल लहलहाने लगी। वह सोचता था कि यह सब सूर्य भगवान् की ही कृपा है। भास्कर जब बड़ा हुआ और उसने बगल के कस्बे के स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की तो महादे ने उसकी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए पटना में नाम लिखवाया। गाँव के दूसरे बाबू भइयों के लड़कों से भास्कर के ‘जिट’ में कोई कमी न आए, इसलिए उसने गाँव के महाजन से कर्ज लेकर घड़ी, साइकिल और ट्रांजिस्टर खरीदकर दिया, टेरेलिन की कमीज और बुश्शर्ट सिलवाई और बेटे को दो सौ रुपए महीने का खर्च भी भेजना शुरू किया। उसके शरीर में बाप का एक ऐसा दिल था, जो धड़क-धड़ककर कह रहा था कि इस शरीर का खून और मांस बेचकर भी वह भास्कर को पढ़ाता रहेगा और बड़े बाबुओं के लड़कों की पंक्ति में उसे बैठाएगा और एक बार किसी ऊँची कुरसी पर, जिस पर जज, कलक्टर, एस.डी.ओ. या प्रखंड का बी.डी.ओ. बैठता है या पुलिस का बड़ा हाकिम बैठता है, बैठा देखेगा और तब भगवान् को लाख-लाख धन्यवाद देकर अपनी आँखें मूँद लेगा। शहर से जब बेटे की पहली चिट्ठी आई तो वह फूला नहीं समाया। अपने फेंटे में बाँधकर वह हफ्तों इधर-उधर घूमता रहा, जिस-तिस से उसे पढ़वाता रहा और जैसा कि बेटे ने लिखा था, एक और बुश्शर्ट तथा पैंट बनवाने के लिए, उसने गाँव के महाजन से, जिससे पहले ही पाँच सौ रुपए कर्ज ले चुका था, दो सौ रुपए और लेकर तुरंत ही मनीऑर्डर किया। कार्तिक में छठ के समय उसने दंडवत् देते समय भगवान् को फिर लाख-लाख धन्यवाद दिया और अगहन-पूस में भगवान् ने उस पर अपना आशीर्वाद और उड़ेला, इस रूप में कि जिन खेतों में पिछली बार उसे डेढ़ सौ मन धान हुआ था, इस बार पूरे तीन सौ मन पैदावार हुई, क्योंकि उसने इस बार उन्नत किस्म का बीज ब्लॉक से लिया था तथा कृषि पदाधिकारी ने फर्टिलाइजर वालों को कहकर उसके खेतों को नुमायशी खेत बनवा दिया था, उसमें मुफ्त में पूरी खाद डलवा दी थी। और भगवान् भी जब देते हैं तो छप्पर फाड़कर—इस बार गल्ले का भाव भी आसमान को छू रहा था। पिछले साल चावल का भाव साठ-सत्तर रुपए मन तक चला गया था तो किसानों के चेहरों पर नई रौनक आ गई थी, लेकिन इस बार तो शुरू में ही नया चावल पचहत्तर-अस्सी रुपए मन बिक रहा था। महादे ने मन-ही-मन हिसाब लगाया—एक सौ मन खेहन-बिहन के लिए रखकर बाकी धान या चावल बेच देने पर महाजन का कर्ज लौटे जा रहा था, भास्कर का साल भर का खर्च पूरा हो जा रहा था तथा दो बैलों का और लेना आवश्यक था, वह समस्या भी हल हो रही थी। r सबके बावजूद शहर और गाँव दो इकाई हैं। शहर जहाँ चकाचौंध है, रेशमी डोरे हैं, फूल हैं, पार्क हैं, चमचमाती सड़कें हैं, सिर उठाए बड़े-बड़े मकान एवं भवन हैं, होटल हैं, बार हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, सजी-सँवरी मृदुभाषियाँ हैं, चमचमाती कारें हैं और मोहक वातावरण है, वहीं आज भी भारत के गाँव किसी टूटे हुए जीर्ण-शीर्ण मंदिर के भग्नावशेष की तरह मेंड़ों, खपरैलों, घास-फूँस की झोंपडि़यों, कीच-कादों-कोहवर-कोयल-कौआ-खैनी-बीड़ी-अँगोछा-अँगिया-करती-बिछुआ-हँसुली और चोपे हुए तेलों की धार के बीच मोटी माँग से होकर गुजरती पाव भर सिंदूरी रेखा के समान ही बेतरतीब हैं। शहर, जो किसी नागिन की लट और साँप की फु फकार के जीवित प्रतिबिंब हैं और भारत के गाँव परंपरा-बोधों के अंदर जकड़े आर्थिक टूटन और कसमसाहट में साँस लेते सत्य-ज्ञान। पहले की पीड़ा अशेष कामना है और दूसरे का दर्द अगाध विश्वास। शहर अमलतास का गदराया गुच्छा है तो देहात सेमल का फूल, जो मुरझाकर बिखर रहा है। एक की अन्विति रंग-रूपों और मधु-सपनों का अनगिनत ज्वार है तो दूसरे की व्याप्ति क्षीर-सागर से प्राप्त विष का पान। आज भारत नदी के इन दोनों किनारों के बीच से अपनी नाव खे रहा है और प्रयास कर रहा है समन्वय या संतुलन का, परंतु विषमता की खाई इतनी बड़ी है जो सुलझाने की जिज्ञासा में समस्याओं को और उलझा देती है। इसलिए गाँव का आदमी जब पहली बार शहर में पाँव रखता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मोटर का हॉर्न सुनकर वह चौंक जाता है, किसी आदमी ने डाँट दिया तो बेहोश होने लगता है तथा किसी शो-केस में सजाई गई औरत के बुत को असली समझकर आँखें लड़ाने की कोशिश करने लगता है और यह सोचता है कि कैसी बेशरम औरत है, जो पलक भी नहीं झपझपाती। लेकिन वही आदमी शहर में चाहे कोई काम करने आए या पढ़ने आए, जब अपने गाँव में कुछ दिनों के बाद वापस आता है तो शहर उसके ऊपर इस प्रकार सवार हो जाता है कि हर गाँववाला उसे ‘मुच्छड़’ लगने लगता है तथा गाँव का यह माहौल भयानक, बीभत्स, पिछड़ा, दकियानूस एवं असांस्कृतिक। r पटना से छह महीने बाद भास्कर जब अपने गाँव कंचनपुर पहुँचा तो यह कहना कठिन था कि उसके लिए गाँव बदल गया था या गाँव के लिए वह बदल गया था। पैंट और बुश्शर्ट उसके शरीर पर वैसे ही चिपक गए थे जैसे गोंद के दोनों हिस्सों पर पानी लग जाने से टिकटें चिपक जाती हैं। गाँव के हर गली-कूचे को देखकर उसे उबकाई आती; बराबर भिन्नाता—कितने गंदे और बदतमीज और गए-गुजरे हैं ये लोग कि न रहना आता है, न पहनना और न उठना-बैठना। ‘‘बप्पा, बैलों को जहाँ बाँधते हो, वहीं चारपाई भी क्यों डाल देते हो? और जिस हाथ से उन्हें सानी देते हो उसी हाथ से खैनी भी खाते हो। छिह-छिह!’’ जब-तब भास्कर अपने बाप को झिड़क देता। और महादे की समझ में बात नहीं आती कि इसमें भला क्या बुरा हो गया? आखिर वर्षों से यही क्रम तो चला आ रहा है और भास्कर को भी तो उसने ऐसे में ही बड़ा किया है। एक दिन भास्कर ने अपने थाल की रोटी माँ के सामने उठाकर फेंक दी और माँ के ऊपर बरसा, ‘‘जिस हाथ से उपले थापती हो, गोबर निकालती हो, उसी हाथ से आटा भी गूँधती हो! रोटी में गोबर की गंध है, मैं ऐसी रोटी नहीं खाता। मेरा तो जी नहीं करता है कि इस गंदगी भरे घर में एक मिनट भी रहूँ।’’ और बुधनी अपने बेटे को फटी आँखों देखती रह गई। पैदा हुआ उसी दिन से इसी तरह से खिला-पिलाकर बड़ा किया, पता नहीं आज इसे हो क्या गया है? r आश्विन के बाद कार्तिक आया और छठ-पूजा धूम फिर शुरू हुई। देव मेले की तैयारी में सारा इलाका लग गया। आस-पास के गाँवों से ही नहीं, दूर-दराज से बैलगाडि़यों में, ट्रैक्टरों पर, बसों में, टैक्सियों में भर-भरकर ‘परबइता’ आने लगे। ‘उपास’ के दिन भारी रेला-पेला, लाखों की भीड़, तिल रखने को जगह नहीं, सिर पर ‘दउरी’ और ‘सूप’ लिये अर्ग दिलवाने जा रहे मर्द और नई साड़ी पहने, नाक तक सिंदूर लगाए, छठ मैया के गीत गाती औरतें। इन्हीं लाखों की भीड़ में एक महादे भी है—पस्त-त्रस्त-हारा-थका-चूर-चूर महादे, जिसने विगत इक्कीस-बाईस सालों की तरह आज भी दंडवत् दिया है, व्रत रखा है, सूर्य-मंदिर की देहरी पर जाकर माथा नवाया है, लेकिन प्रार्थना कुछ और ही की है। उसकी आँखों में न रोशनी है, न हृदय में किसी प्रकार का उत्साह, न भावनाओं का ज्वार, न किसी प्रकार की लालसा। मंदिर के कोने में ‘गुलायची’ के पेड़ की जड़ के पास बैठा हुआ मंदिर के स्वर्ण-कलश की ओर निहार रहा है और बार-बार सोचता है कि ‘सूर्यकुंड’ में अगर डूबने भर पानी होता तो वह अपनी इहलीला आज ही समाप्त कर देता। पैंतालीस-पचास साल का महादे सहसा महसूस करता है कि वह सत्तर-अस्सी साल का बूढ़ा हो गया है। उसकी कमर झुक गई है, आँखों की रोशनी चली गई है और वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। उसकी गीली धोती, जिसे पहनकर उसने दंडवत् दी है, बालुओं, कीचड़ों और खुरदरी सड़क की गिट्टियों में मिलकर रीठ आई है और वह गीली धोती बदन से सटकर ‘लीज-लीज’ हो गई है। भगवान् ने उसकी सारी बातें अब तक मानीं, उसे अच्छी पत्नी दी, शादी के दो साल के अंदर बच्चा दिया, हल-बैल दिए, खेती-गृहस्थी दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया और जब भी महादे ने जिस चीज की कामना की, वह उसे मिली। लेकिन आज भगवान् से उसने कुछ और ही माँगा है। क्या भगवान् आज उसे निराश कर देंगे? r भास्कर के शहरी-जीवन का यह चौथा वर्ष था और उसके कॉलेज की पढ़ाई का भी चौथा साल। इस बार दशहरे की छुट्टियों में भास्कर जब घर आया तो वह बिल्कुल बदला हुआ भास्कर था। माथे पर झूलते हुए लंबे-लंबे बाल, जैसे शादी-ब्याह में महादे ने नचनियों के सिर पर देखे थे, पिता के सामने ही सिगरेट पीकर ‘फक-फक’ धुएँ के छल्ले छोड़ना, जैसे बड़े-बड़े साहबों के मुँह से महादे ने देखा था। रात में बक्से से बोतल निकालकर गटागट कुछ पी जाना और फिर अनाप-शनाप बकना। और बात यहीं रुकती तो भी गनीमत थी, लेकिन उसने अपने माँ-बाप से इस बार एक हजार रुपयों की फरमाइश की थी और जब महादे ने यह कहा कि इतना रुपया एक साथ वह कहाँ से लाएगा, इस बार तो पैदावार की हालत भी खराब है, तो वह गरजा था—‘‘मैं यह सबकुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ, तुम लोगों ने मेरा एडमीशन पटना में क्यों कराया था जब पूरे पैसे नहीं दे सकते? पैदा ही क्यों किया था, जब सँभालने की ताकत नहीं थी? पढ़ाने का मंसूबा क्यों बाँधा था जब गाँठ में कूवत नहीं थी? ‘‘बूढ़े, सुन लो आँख खोलकर, मैं एक हजार रुपए लिये घर से नहीं जाऊँगा। और परसों तक मुझे यह पैसा चाहिए—चाहे तुम बैल बेचो, खेत बेचो, मकान बेचो या अपने आपको बेचो!’’ यह बोतल का लाल रंग बेटे के मुँह से बोल रहा था, जिस बेटे के लिए महादे ने भगवान् से वर्षों मिन्नतें माँगी थीं, एक शाम खाकर, पैसे जुगाड़ कर भेजता रहा था, महाजन के सामने गिड़गिड़ाकर, चिरौरी-विनती करेकर्ज लेकर भी कभी दो सौ, कभी तीन सौ रुपए महीने भेजता रहा था, खद के शरीर पर कभी ‘मिरजई’ नहीं हो सकी थी, लेकिन बेटे को टेरेलिन की बुश्शर्ट और पैंट बनवाता रहा था, बेटे के लिए बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची कुरसियों केख्वाब देखे थे—वही इकलौता बेटा किसी मुगल के समान उसके कलेजे पर सवार था—‘एक हजार रुपया चाहिए परसों तक, नहीं तो घर-मकान में आग लगा दूँगा!’ माँ से यह अपमान कि बेटा अपने बाप को इस प्रकार बूढ़ा कहे सहा न गया और वह बीच में ही बोल पड़ी, ‘‘भास्कर, जरा अपने बाप का तो खयाल किया कर, शरीर चिंता से टूट रहा है, किस-किस प्रकार से तुझे रुपया भेजा जाता है और तुझे इस प्रकार बोलते शरम नहीं आती।’’ बुधनी के मुँह से यह शब्द निकलना था कि भास्कर ने अपने पाँव से चप्पल निकाली और अपनी माँ पर चला दी, ‘‘चुप रह, बुढि़या! मैं एक भी बात तुम लोगों की नहीं सुन सकता।’’ और उसके बाद घर में महाभारत छिड़ गया था। महादे को लगा था कि वह अपने बेटे का खून ले लेगा, ढलती उमर थी, लेकिन देहात का खाया-कमाया शरीर था। उसने भास्कर को पटककर उसका गला दबोचा, ‘‘हरामजादे, आज मैं तेरा खून कर दूँगा। जिस माँ की कोख से पैदा हुआ, उसी से इस तरह बातें करता है।’’ महादे के दिल में चार साल से बसा गुस्सा एक साथ बाहर आ गया था। भास्कर की आँखें निकलने लगीं और वह ‘औ-औ’ करने लगा। बोतल का लाल रंग उड़ता नजर आया। बुधनी लपकी, उसने भरपूर ताकत से महादे की बाँह को झकझोरा, ‘‘भास्कर के बप्पा, ऐसा न करो, तुम्हें मेरी कसम है। जिस समय इसे पेट में लेकर नौ महीने बिताए थे, मैंने सारा दरद सहा था। इसकी बातें भी इसी प्रकार सह लूँगी। छोड़ दो, भास्कर के बप्पा, छोड़ दो।’’ बुढि़या का करुण विलाप महादे को कँपा गया और उसका हाथ ढीला हो गया, लेकिन उसका दिल ढीला न हो सका। वह चिल्लाया, ‘‘कमीने, निकल जा अभी इसी समय इस घर से, नहीं तो तेरी हड्डी-पसली एक कर दूँगा।’’ बाहर दरवाजे की ओर उसने इशारा किया और ऐसी परिस्थिति में भास्कर के लिए चारा ही क्या था। वह घर से बाहर हो गया, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद महादे के मकान के पास पूरा गाँव जमा था। विचित्र भाग-दौड़ मची थी। किसी के हाथ में बाल्टी थी, किसी के हाथ में लोटा, तो कोई डंडे से खपरैल, छप्पर को पीटे चला जा रहा था—पश्चिम की ओर से मकान में आग लगी थी। चार कमरों केघर में दो कमरे बिल्कुल स्वाहा हो गए थे, दो को बचाने का प्रयास चल रहा था। भाग-दौड़ में दो बैल और एक बछिया झुलस गए थे, चावल की कोठी से बदबू फूट रही थी और मकान के सामने खड़ा महादे अपलक नयनों से इस ‘स्वाहा’ को देख रहा था। बार-बार उसका जी करता कि वह चिल्लाकर कहे कि छोड़ दो, मत बुझाओ इस आग को—लेकिन उसके मुँह से बोली नहीं निकलती थी। आग जब शांत हुई तो लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया, ‘‘कुछ पता चला, किसने आग लगाई, कैसे आग लगी?’’ लोग पूछ रहे थे। ‘‘कान खोलकर सुन लो, मैंने स्वयं इन्हीं हाथों से अपने घर में आग लगाई थी!’’ चुप्पी तोड़ता हुआ महादे गरजा, ‘‘मैं पूछता हूँ, तुम सब क्यों आए आग बुझाने? मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था।’’ और भीड़ धीरे-धीरे छँट गई। कोई बोल रहा था, ‘‘भले का जमाना नहीं है, जिसकेलिए चोरी की, वही कहे चोर।’’ तो कोई यह कहता हुआ जा रहा था, ‘‘महादे का दिमाग खराब हो गया है!’’ दूसरे दिन गाँववालों को यह भी पता चला कि आग की लपटों में बुधनी भी फँस गई थी, किसी प्रकार बाहर निकली और चार बैलों में से दो बैल झुलसकर मर गए। महादे का कहीं पता नहीं था, चार दिन बाद ही छठ का व्रत था, शायद वह देव की ओर चला गया था। देव का सूर्य-मंदिर जिसके निर्माण, जिसके काल, जिसकी तिथि के संबंध में कितनी किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, आसमान की ओर सिर उठाए खड़ा था। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि बावन पोरसे के इस मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया। तिथि, काल, निर्माण—कोई भी हो, बिहार में कला और शिल्प की दृष्टि से यह सूर्य-मंदिर अद्वितीय है। यों तो हर रविवार को यहाँ हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन सूर्य-पूजा यानी ‘छठ-व्रत’ जिसकी बिहार में सबसे अधिक महत्ता है, उस समय दर्शनार्थियों की संख्या लाखों में हो जाती है। पूरे इलाके में इस मंदिर की बड़ी प्रसिद्धि है और दुखी मनुष्य भगवान् की देहरी पर बड़ी आशा लेकर आता है। महादे हिला, जैसे कोई शव या प्रेत-छाया हिले। बढ़ी दाढ़ी, खिचड़ी बने बाल, कादो-कीचड़ से सना पूरा शरीर तथा शरीर से तिलचट्टे के समान सटी धोती। वह मंदिर की देहरी तक बहुत मुश्किल से डगमगाता हुआ पहुँचा और दंडवत् की मुद्रा में गिर पड़ा और उसके मुँह से अस्पष्ट शब्द निकले—‘‘हे भगवान्! अगले जीवन में निरवंश रखना, लेकिन ऐसा बेटा मत देना।’’ लोगों की भीड़ आती रही; जाती रही, लेकिन महादे वैसे ही पड़ा रहा। अंत में कुछ लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की; लेकिन वह इसके पहले ही उठ चुका था। महादे उठ गया, लेकिन छोड़ गया सदा के लिए एक सवाल—शिक्षा और संस्कृति की धरती और प्रबुद्ध केंद्र क्या कटे या टूटे अभिषेक की सृष्टि तो नहीं कर रहे हैं, जहाँ एक नहीं, कई भास्कर रोज-ब-रोज कितने महादेवों का खून पी रहे हैं और छोड़ रहे हैं—आस्थाहीनता का ऐसा प्रश्न, जिसका उत्तर ढूँढ़े नहीं मिलता।
शंकरदयाल सिंह |
जुलाई 2024 |


.png)











