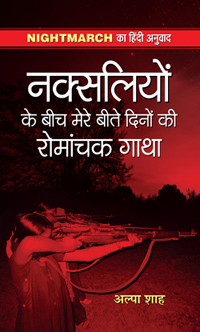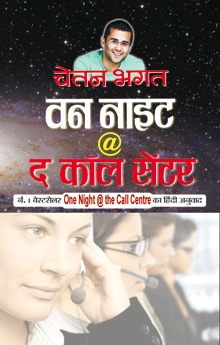राष्ट्रीय विचारों के प्रखर लेखक, चिंतक, टी.वी. डिबेट्स का एक प्रमुख चेहरा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद् दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष। संप्रति दिल्ली विश्वविद्यालय के पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज में व्याख्याता।
आपातकाल के तुरंत बाद की बात है, मैं रामजस कॉलेज का विद्यार्थी था, सूर्यकांत बालीजी वहाँ संस्कृत के प्राध्यापक थे, मैं हिंदी ऑनर्स का छात्र था, इस कारण मेरा उनसे सीधा-सीधा संबंध का कोई कारण नहीं था, परंतु बालीजी विद्यार्थी परिषद् का कार्य देख रहे थे, वे कॉलेज परिसर में ही कई बार विद्यार्थियों के साथ बैठक करते थे, इस नाते मेरा उनसे संबंध बना। बालीजी जितने तर्कशील थे, उससे कहीं अधिक भावुक थे। उनकी पसंद-नापसंद बिल्कुल स्पष्ट होती थी।
राष्ट्र-हित और विद्यार्थी परिषद् के लिए जो उचित होता था, उसमें वे कतई समझौता नहीं करते थे, इस कारण उनकी कई लोगों से असहमति संबंधों के भविष्य तक पहुँच जाती थी। वे इस सीमा तक स्पष्ट वक्ता थे कि उन्हें कई बार इस कारण नुकसान भी उठाना पड़ा, किंतु जिसका वे सम्मान करते थे, उसका अतिशय मुक्त हृदय से सम्मान करते थे, उसमें फिर पद और आयु बिल्कुल नहीं आड़े आते थे, इसलिए चालीस-पचास वर्षों से पहले के संबंध आज भी बिल्कुल तरोताजा बने हुए थे। मैं स्वयं ही उनसे आयु में बहुत छोटा हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे मित्र कहकर ही संबोधित करते रहे। एम.ए. करने के पश्चात् मैं भी अध्यापन के क्षेत्र में आ गया तो फिर तो मैं उनका एकदम अंतरंग हो गया।
अध्यापन के क्षेत्र में आने के पश्चात् मैं न जाने कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षक राजनीति में आ गया। मैं और बालीजी दोनों ही वामपंथियों की देश-विरोधी और शिक्षा-विरोधी राजनीति के मुखर विरोधी थे, हम घंटों-घंटों तक बहस करते थे और शिक्षक राजनीति में वामपंथियों के प्रभाव को लेकर चिंता साझा करते थे। बहुत बार कुछ न कर पाने की झुँझलाहट भी हो जाती थी। इसी बीच बालीजी ने व्यक्तिगत बहसों से बाहर निकलकर नवभारत टाइम्स में लेखन आरंभ कर दिया। उनके लेखन से प्रभावित होकर ही नवभारत टाइम्स के तत्कालीन संपादक राजेंद्र माथुर ने उन्हें अपनी संपादकीय ‘टीम’ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। बालीजी अध्यापन कर्म से अवकाश लेकर सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में चले गए। राजेंद्र माथुर की टीम में बालीजी ही उनके सबसे विश्वस्त और प्रिय साथी थे। बालीजी जो लिखना चाहते थे, माथुर साहब ने उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया। बालीजी सामान्यतया देश की राजनीति पर ही लिखते थे, लेकिन माथुर साहब से उनकी बातचीत में भारतीय इतिहास, संस्कृति, ज्ञान-परंपरा और विरासत बार-बार उद्धृत होती थी। माथुर साहब ने बालीजी के ज्ञान और समझ को नवभारत टाइम्स के पाठकों तक पहुँचाने के लिए उन्हें एक स्तंभ लिखने के लिए प्रेरित किया। ‘भारत के मील के पत्थर’ नामक यह स्तंभ इतना लोकप्रिय हो गया कि पाठक रविवार की प्रतीक्षा करते थे, अखबार के दफ्तर में पाठकों के हजारों पत्र आने लगे। इसी स्तंभ से बालीजी पाठकों के प्रिय लेखक हो गए। पत्रकारीय शैली और भाषा में भारत के अतीत का यह ऐसा स्तंभ था, जिसे नवभारत टाइम्स का सामान्य पाठक भी हाथोहाथ लेता था। कालांतर में ‘भारत के मील के पत्थर’ के ये लेख ‘भारत गाथा’ नाम से पुस्तकाकार रूप में आए तो यह पुस्तक बालीजी की पहचान की प्रतीक बन गई। तत्कालीन सरसंघचालक कुप.सी. सुदर्शनजी ने ‘भारत गाथा’ का लोकार्पण
किया था।
सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण के पश्चात् बालीजी की
‘भारत की राजनीति को समझने की शर्तें’ जैसी पुस्तक आई, जो सचमुच भारतीय राजनीति के सूक्ष्मतम रहस्यों को खोलती है। बालीजी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश तो किया, राजनीति पर उन्होंने सैकड़ों लेख भी लिखे, लेिकन उनका मन रमता था भारत के अतीत की उस ज्ञान-संपदा में, जिसमें अवगाहन किए बिना भारत को जाना-समझा ही नहीं जा सकता था, सो उन्होंने ‘महाभारत : पुनर्पाठ’ और ‘महाभारत का धर्म संकट’ जैसी पुस्तकों की रचना की। दोनों पुस्तकें महाभारत के युद्ध एवं नीति को समझने की एकदम नवीन दृष्टि देती हैं—महाभारत का युद्ध क्या वास्तव में
उत्तराधिकार का युद्ध था या फिर इससे इतर इसका कोई और गहन कारण था, जिससे यह युद्ध टाला नहीं जा सका।
‘महाभारत’ जैसा आर्ष ग्रंथ केवल एक युद्ध का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है, जिसमें भारत के उस गौरवशाली इतिहास का सत्य खुलासा हुआ है, जिसमें पारिवारिक संबंधों से ऊपर, बहुत ऊपर ‘न्याय’ और ‘धर्म’ है—यही भारत का सार्वकालिक-सार्वभौमिक सत्य है।
लेकिन बालीजी ने केवल लेख ही नहीं लिखे, विवेचन-विश्लेषण ही नहीं किया, उन्होंने औपनिषदिक पृष्ठभूमि पर ‘दीर्घतमा’ और ‘तुम कब आओगे श्यावा’ जैसी औपन्यासिक कृतियों का भी सृजन किया। ‘दीर्घतमा’ और ‘श्यावा’ दोनों ही मंत्र रचयिता ऋषि हैं, उनको आधार बनाकर उपन्यास लिखना सरल काम नहीं था, लेकिन बालीजी के सृजनशील व्यक्तित्व ने उन्हें जीवंत पात्र के रूप में ऐसे गढ़ दिया, जैसे वे आज ही के पात्र हों। ‘गार्गी’ को केंद्र में रखकर वे एक और उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन संभवत: यह उपन्यास अधूरा ही रह गया।
यह पुस्तक इस प्रश्न को उठाने का साहस करती है कि ‘ब्राह्मण ग्रंथ’ परंपरा के प्रवर्तक वे ऋषि हैं, जिन्हें आज भी भाषा में दलित कहा जाएगा। ऋषि महिदास एेतरेय ऐसे ही ऋषि थे। ‘उपनिषद् के प्रख्यात दलित प्रवक्ता—सत्यकाम जाबाल’ भारत के अतीत के ऐसे रहस्य का खुलासा करता है, जिसके आगे आज के जातिवादी नितांत निरुत्तर हो जाएँगे। ‘वाल्मीकि, वेद व्यास एवं सूतजी’ भारतीय मनीषा के ऐसे उज्ज्वल रत्न हैं, जिन्हें निर्विवाद रूप से समूचे भारत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है—शायद ही इनके संबंध में किसी को कोई प्रश्न उठाने का साहस हो।
भारतीय समाज में जाति-व्यवस्था पर बालीजी का नितांत मौलिक विमर्श था। ‘भारत का दलित विमर्श’ उनकी ऐसी पुस्तक है, जो जाति-जाति रटने वालों की आँख खोल दे। आज जो लोग दलित-विमर्श के नाम पर एकाकी विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका ‘उत्तर पक्ष’ प्रस्तुत करने वाली यह पुस्तक एक ऐसा महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप है, जो इस विषय को नए सिरे से सोचने को विवश कर देती है।
भारतीय राजनीति को बालीजी कितनी सूक्ष्म दृष्टि से देखते थे, इसका प्रमाण उनकी पुस्तक ‘भारत की राजनीति के महाप्रश्न’ है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की राजनीति की दिशा और दशा का एक तरह से यह श्वेत-पत्र है, जो ऐसे यक्ष-प्रश्नों से टकराती है, जिसके विषय में सामान्यत: चर्चा तक नहीं होती। स्वातंत्र्योत्तर भारत की
राजनीति के उतार-चढ़ावों के कई कुहासों को खोलती यह पुस्तक उनकी राजनीतिक पैनी नजर का बेबाक बयान करती है। ऐसे ही ‘भारत के व्यक्तित्व की पहचान’ उनके ‘भारत-बोध’ एवं भारतीयता को सही संदर्भों में समझने का मौलिक प्रयास है। बालीजी भारत के अतीत को ईरान की सीमा तक देखते थे और इस पूरे उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एकता के ऐसे रहस्यों को खोलते दिखाई देते हैं, जिन्हें अब विस्मृत सा कर दिया गया है।
बालीजी को ज्ञान-संपदा विरासत में मिली थी, उनके पूज्य पिता स्व. पं. चंद्रकांत बालीजी इतिहास, ज्योतिष एवं संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान् थे। पितामह पं. चूड़ामणिजी भी अपने समय के संस्कृत साहित्य के सुविख्यात व्यक्तित्व थे। भारत विभाजन के समय ‘मुल्तान’ से विस्थापित होकर भारत आए इस परिवार ने भी वे सभी यंत्रणाएँ झेलीं, जो हजारों-लाखों परिवारों ने उस समय झेली थीं। अपने ही देश के दो टुकड़े हो गए और लाखों लोगों ने उस विभाजन के परिणामस्वरूप जो कष्ट, यंत्रणा और पीड़ा झेली थी, वह पीड़ा इस परिवार ने भी झेली, लेकिन बालीजी के परिवार ने जिस साहस और धैर्य से परिस्थितियों की चुनौती को स्वीकार किया, उसने बालीजी के व्यक्तित्व-निर्माण में बहुत ही महती भूमिका अपनाई। बालीजी ने जिस प्रकार हर चुनौती का सामना किया, उनके व्यक्तित्व में जो संकल्पशीलता थी, उसमें वह संघर्ष बहुत बड़ा कारण था, जिसमें उनका बचपन बीता था।
बालीजी स्पष्ट वक्ता होने की विशिष्टता उनके इसी संघर्ष का परिणाम था, उनका पारदर्शी व्यक्तित्व ही वह वजह थी, जिसके कारण वे जिस क्षेत्र में गए, वहाँ उन्हें अप्रतिम प्रतिष्ठा एवं सम्मान मिला। बालीजी के तेजस्वी व्यक्तित्व एवं उनके शब्द रूप साहित्य की स्मृति उनकी मित्रमंडली में स्थायी रहेगी। हम सब उनकी ओजस्वी वाणी की अनुपस्थिति को कैसे स्वीकारेंगे—पता नहीं?
४१, जगदंबा अपार्टमेंट्स
सेक्टर-१३, रोहिणी
नई दिल्ली-११००८५
दूरभाष : ९८१०३६४०९६