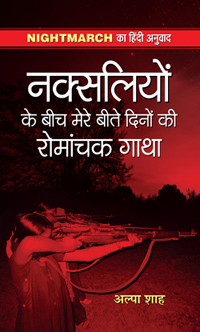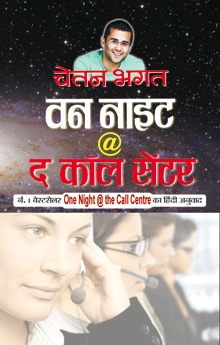अपना-अपना नजरिया है। कुछ हैं, जो जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। वाहन के नाम पर उनके पास एक स्कूटर है। उसे वर्तमान की तुलना में ‘खटारा’ कहना अधिक उचित है। उन्हें अपनों से शिकायत है। यह पत्नी के माता-पिता का कर्तव्य था कि हर साल, दो साल में नया मॉडल दे देते। उन्हें दु:ख है कि लड़की वालों ने यह कर्तव्य नहीं निभाया। विंटेज या पुरानी गाड़ियों की तो एक रैली भी होती है। सजी-सजाई चार पहिए के वाहन के साथ उसके मुसकराते स्वामियों के चित्र भी अखबारों में छपते हैं। इतना ही नहीं, झंडा या झंडी लहराकर मंत्री या मुख्यमंत्री भी इस प्रदर्शन का उद्घाटन करते हैं।
हमारे नायक के भाग्य में तो यह भी नहीं है। उनके दो-पहिया वाहन की तो कोई नुमाइश भी नहीं है, उलटे लोग यह प्रश्न करते हैं कि “भाई जी! यह किस जमाने का है? क्या गजब है कि अाजतक चलता भी है?” यह सुन-सुनकर उनके कान पक गए हैं। लिहाजा, उन्होंने उसे कवर चढ़ाकर सुरक्षित रख छोड़ा है। दिक्कत यह है कि उसका कोई खरीदार भी नहीं है। उन्होंने कई कबाड़ियों को इसलिए उसे बेचने का प्रस्ताव दिया है, पर वहाँ भी उत्तर में सिर्फ इनकार है। नतीजतन, वह अपनी पत्नी से बिगड़ते रहते हैं, कहते दाल में नमक नहीं होने पर, कभी सब्जी में। इनसानी बरदाश्त की भी सीमा है। वह भी उन्हें खरी-खोटी सुनाने से क्यों चूके? उसका सीधा जवाब होता है—“आपके मुँह के स्वाद में कुछ गड़बड़ है?” उनका चुप होना आवश्यक है, वरना उनका छोटा पुत्र अपनी माँ के कैंप का है। “माँ सच कहती है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा”, कहकर वह उन्हें चुप करा देता है।
इस देश में भी मौसम, भाषा और व्यक्तियों की ही नहीं, सोच की भी विविधता है। कुछ हैं, जो अपने प्राध्यापन के काम को कर्तव्य की तरह निभाते हैं। कुछ इसे, अपनी योग्यता का अपमान मानते हैं। उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा की नौकरी थी। वह आज भी दु:खी हैं कि परीक्षा के ‘चांस’ में सफल न हो सके। विवशता में ‘बैचलर ऑफ एजुकेशन’ की डिग्री लेकर प्राध्यापक बन बैठे। अब वह अपना, निजी बदला, शिक्षण संस्थाओं से ले रहे हैं। यो छात्रों में वह लोकप्रिय हैं। क्लास में नई फिल्मों से लेकर जोक्स सुनाने तक का उनमें हुनर है। छात्र भी सुखी हैं, वह भी। साहित्य की कक्षा में वह फिल्मों की पटकथा सुनाते हैं और जोक्स की विविधता। उनका विश्वास है कि साहित्य खुद पढ़ने का विषय है, पढ़ाने का नहीं। यों वह परीक्षा के संभावित प्रश्नों की कुंजी छात्रों को अवश्य सुझाते हैं, जिससे उनका परिणाम सकारात्मक आए। वह सफल हैं। उनकी क्लास का रिजल्ट शत-प्रतिशत रहता है।
भारत में हर नागरिक को सरकार में संपर्क रखना-ही-रखना। अधिकांश का मत है कि सरकार एक कामचोर, निकम्मी और भ्रष्ट संस्था है। बिना लेन-देन और सतत संपर्क के वहाँ कुछ भी होना असंभव है। अवकाश प्राप्त सरकारी सेवक इस धारणा की पुष्टि करते हैं। सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। कुछ का प्रमोशन नहीं हो पाया, कुछ की अधिकारी से नहीं पटी। बहरहाल, सेवानिवृत्त कर्मचारी या अधिकारी सरकार से सब असंतुष्ट हैं। कर्मचारी अफसरों के भ्रष्टाचार को दोष देते हैं, अधिकारी कर्मचारी को। सरकार को करप्ट और अक्षमता की छवि बनाने में दोनों का बराबर का योगदान है। लोगों का स्वाभाविक विचार है कि इसने तो अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में खपा दिया, अगर उसका यह मत है तो जरूर सच होगा।
हम भी अपने मोहल्ले के मोहन बाबू के संवादों में इसी भ्रम में रहे। उनका घर और समृद्ध जीवन-शैली सब सरकार की इनायत थी। वह रिटायर तो केवल सैक्शन अधिकारी के पद से हुए थे, पर रहन-सहन किसी उच्चाधिकारी से कम नहीं था। मोहल्ले के पार्क में वह रोज सुबह सैर करने जाते। वहीं वह हमारे ऐसे सरकारी कार्य-पद्धति से अनजान व्यक्तियों को बैंच के आसन से प्रवचन देते, आप लोग भाग्यशाली हैं कि सरकार की सेवा में नहीं हैं, वरना वहाँ पेट भरने के लिए लोग, खाना नहीं, बस सिर्फ पैसा खाते हैं। हमने तो अखबार में पढ़ा था कि कुछ सियासी महापुरुष जैसे कभी चारा चबाते थे। वैसे ही पैसा खाना उन्हें जीवंत और स्वस्थ रखता है। यों वहाँ एक कल्याणकारी शासन होने के नाते डॉक्टरों की भी पूरी फौज है, जो केंद्रीय कर्मियों की सेहत की देख-भाल करती है, बीमार पड़ने पर दवा देती है। आप सबको आश्चर्य होगा। यहाँ भी घोटाला है। कुछ कर्मचारी दवा दुकानदारों को बेच देते हैं, कई डॉक्टर टेस्ट लिखने का जाँच के संस्थानों से ‘कमीशन’ खाते हैं। वह भी ऐसा-वैसा नहीं, कम-से-कम बीस प्रतिशत का। सरकार के हर विभाग में धाँधली है, ठेका देने से लेकर बिल बनाने और उसके भुगतान तक। कभी भारत सोने की चिड़िया रहा होगा, अब तो शासकीय विभाग भ्रष्टाचार के गिद्ध हैं। जीते-जी इनसान को नोच-नोचकर मृत करने में उनका सानी नहीं है।”
मोहन बाबू के प्रवचन रोचक हैं और उनके करप्ट आचारण की स्वीकारोक्ति। आलोचना व्यक्ति की हो या संस्था की, हमेशा रुचिकर लगती है। ऐसे भी, वर्तमान समय में सामाजिक मेल-जोल का चलन घटा है। अब ‘लैपटॉप’ है, ‘स्मार्ट फोन’ है। सब उसी के प्रयोग में उलझे हैं। फेसबुक पर कोई अपनी काल्पनिक प्रेम-कहानियाँ लिख रहा है तो कोई अपनी दिनचर्या। किसी के पास फुरसत ही नहीं है, जीवन की वास्तवितकता के सच को समझने या जाँचने की।
सबकी अपनी-अपनी कल्पना की कारगुजारियाँ हैं। वह उन्हीं में गुम है। ‘सब चलता है’ के युग में सबसे अधिक असर जीवन-मूल्यों पर पड़ा है। पारंपरिक संबंध, रिश्ते-नाते जैसे शहरों में गौरैया की तरह गुम हैं। कितना भी खोज लीजिए, कहीं नजर ही नहीं आते हैं। भाई भाई का शत्रु है, दोनों मिलके माता-पिता से दुश्मनी में साथ हैं। कल टैं बोलने वाले हों तो आज ही क्यों न विदा हों? जो बड़ा घर बूढ़े घेरे है, उसका स्वामित्व बेटे को मिले। जीवन-बीमा भी होगा ही, उसकी राशि उड़ाएँ-खाएँ।
सबसे अधिक दुर्दशा नैतिक मूल्यों की है। उन्हें कोसने वाले के लाखों ‘समर्थक’ (फाॅलोअर) हैं। उनकी लोकप्रियता का इकलौता कारण उनके नैतिक रिश्तों का उपहास है। कुछ विवाह की संस्था के विरुद्ध और ‘लिव-इन’ यानी बिना किसी बंधन के, साथ-साथ रहने के पक्षधर हैं तो कुछ माता-पिता के पारंपरिक सम्मान के दुश्मन। परिहास की इस पहेली से यह बूझना कठिन है कि ऐसे चाहते क्या हैं?
इनका आदर्श समाज क्या केवल अराजक विद्रोहियों की जमात है? एक पुरातन और प्रचलित पारिवारिक इमारत को ध्वंस करना ही क्या इनका लक्ष्य है? क्या इन्हें स्वयं यह ज्ञान है कि यह विनाश के वकील उसके स्थान पर रचना क्या चाहते हैं? क्या इन्हें खँडहरों से प्रेम है? या इनके पास कोई वैकल्पिक योजना है? ऐसे प्रश्न अधिकतर अनुत्तरित हैं?
बहुतों के लिए इनका औचित्य भी नहीं है। यह समय ही बदलाव का है, परिवर्तन का है। अस्थायी संक्रमणकाल के भ्रामक ढाँचे से कुछ स्थायी सामाजिक संरचना उभरेगी। यों भी कहीं-कहीं इस बदलाव का विरोध भी है। वैसे भी यह परिवर्तन का समय है। पुरानी के साथ नई व्यवस्था का सहअस्तित्व है। कौन कहे, कब तक यह विचित्र स्थिति रहे?
देशों में भी देखा जाए तो अजब हालात विद्यमान हैं। कहीं प्रजातंत्र है, कहीं शाही एकतंत्र। यों अपने को प्रजातांत्रिक कहना एक नया ‘फैशन’ है। चीन का तानाशाह भी अपने विरोधियों के विनाश में सक्षम है। विरोध के स्वर प्रजातंत्र में भी उभरते हैं, पर यह व्यक्तिगत कम, नीतिगत अधिक होते हैं। ज्यादातर इनका हिंसक होना भी आवश्यक नहीं है। बेतहाशा मूल्यवृद्धि अथवा शिक्षित बेरोजगारी ऐसे ही सार्वजनिक मुद्दे हैं। इन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने को आंदोलन होते हैं, जुलूस निकलते हैं, कभी दुकानें लुटती हैं, कहीं बाजार। विद्वानों का यह कथन प्रासंगिक है और उचित भी कि भीड़ पर नियंत्रण कठिन है। वह कब तक अहिंसक रहें, इसका अनुमान भी मुश्किल है? ऐसे यह आम धारणा है कि प्रजातंत्र में परंपरा चली आ रही है आंदोलनों के अहिंसक होने की। विशेषकर भारत ऐसे शांति प्रिय देश में।
भारतीय इनसान आमतौर पर अहिंसक हैं। पर उनमें भी अपराधियों के ऐसे अपवाद हैं, जो बाहुबल, हिंसा और अपहरण, हत्या, चोरी, डकैती जैसे गुनाहों से अपना काम चलाते हैं। प्रजातंत्र में छवि या ‘इमेज’ का कितना प्रभाव है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इनमें से भी कुछ सफल राजनेता बनते हैं, इसके वाबजूद कि वह अपने अतीत को झुठालते भी नहीं हैं। उल्टे, इस क्रांतिकारी व्यक्तिगत प्रगति को प्रजातंत्र में उपलब्ध अवसर की क्रांतिकारी समानता का गुण गाते हैं।
देखने में आया है कि बहुधा आदमी व्यक्तिगत सुविधा-सुभीते का जीवन बसर करने का पक्षधर है। हमारे एक मित्र हैं। वह सबको बताते हैं कि देश में संस्कार, परिवार, कार्यकुशल सरकार, सत्याचार जैसे गुणों का बहुत महत्त्व है। इससे जीवन सुखी रहता है। उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। यह उनके व्यक्तित्व का प्रशंसनीय पक्ष है। वह अपनी जिंदगी को सरल व सहज बनाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए उनकी मान्यता है कि विश्व और अपने देश में भी, हर संस्था या व्यक्ति का आदर्श होना नामुमकिन है। आदर्श अर्थात् ऐसी पर्वत की चोटी है, जहाँ बिना समतल भूमि और घाटी के जीवन संभव नहीं है। इस कारण हर चोटी की ऊँचाई के साथ घाटी और समतल भूमि की ‘खोट’ जुड़ी है, यदि कोई इसे खोट माने-तो-माने। उन्होंने दूसरों के समान अपने जीवन की इस खोट को ‘सब चलता है’ का जीवन-दर्शन बना लिया है।
यदि कहीं भ्रष्टाचार है तो रहे। वह जानते हैं कि उसे मिटाना कुछ का मिशन हो सकता है और होना भी चाहिए, पर उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। वह चुपचाप संबद्ध कार्यालय जाकर घूस का पावन कर्तव्य निभाते हैं। उन्हें भरोसा है कि जीवन का उत्सव या सुख इसी फलसफे से मुमकिन है। सामान्य व्यक्ति को जो व्यवस्था है, उससे समझौता करना आनंद का जनक है। सुधार, बदलाव और परिवर्तन महापुरुषों का दायित्व है। उनके पावन कर्म का शाब्दिक अनुकरण ही उचित है। यह जरूरी नहीं कि वह उनके उदाहरण को अपनाकर कोई भी असुविधा झेले।
जब कोई कहता है कि देश का विकास आवश्यक है तो वह जोर-जोर से सिर हिलाकर उसका समर्थन करते हैं। उन बाधाओं को भी गिनाते हैं, जो राजमार्ग के गड्ढों सा प्रगति के रथ को अवरुद्ध कर रहे हैं। सरकार कल्याणकारी होने का कर्तव्य निभा रही, गरीबों को फ्री राशन देकर। पर इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। कहीं राशन वितरित करने वाले कोटाधारी उसे बेच देते हैं, कहीं राशन इतना घटिया देते हैं कि वह खाने योग्य न हो। जो ऐसी गलती करे, वह अपनी जान से खेले।
ऐसे सरकार ने मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रखी है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। कौन कहे वह परिचित हो कोटाधारियों की हरकतों से? उसे आभास है फ्री राशन की गुणवत्ता का? लिहाजा उसने पाँच लाख तक फ्री इलाज की व्यवस्था पहले ही कर दी है। इससे रोगियों को कम, अस्पतालों को अधिक लाभ है। डॉक्टरों की एक ही रुचि है, कैसे जल्दी-से-जल्दी आयुष्मान कार्ड के अधिकतम खर्च की सीमा पार की जाए? इसमें कमाई की कमाई है और मुफ्त सेवा करने की कीर्ति भी। आपसी चर्चा में चिकित्सक एक-दूसरे को अपनी-अपनी जुगत बताते हैं, जो अधिकतर सरकार को चूना लगाने की विधियाँ हैं। उन्हें आयुष्मान कार्ड का विचार तो पसंद है, पर उन्होंने फ्री इलाज अपने सगों तक का नहीं किया है तो इन अजनबियों का क्यों करें?
फ्री राशन की या आयुष्मान कार्ड की योजना चलाने वाली खुर्राट एजेंसियाँ हैं, जो बिना पैसा लिये अपने बाप तक को ठेंगा दिखाएँ? उन्हें विश्वास है कि पवित्र इनसानी जन्म ही दूसरों से वसूली करने की नियत से मिला है। यदि वह इस जन्मजात दायित्व से चूके तो मृत्यु के बाद स्वर्ग के न होकर नर्क के पात्र होंगे। ऐसे धार्मिक निष्ठावान लगन से अपना इहलोक और परलोक सुधारने में लगे हैं। क्या मजाल कि मामूली चूक भी हो जाए?
एक भलेमानुस ने वसूली बगैर कुछ फ्री राशन या आष्युमान कार्ड बना दिए, अपना कर्तव्य निभाने के इरादे से। वसूली-उसूल के उसके साथियों ने चंदे से सुपारी देकर उस भ्रष्ट की हत्या करवा दी। सिद्धांत तो सिद्धांत है। जो उससे डिगेगा, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, वरना आज एक है, कल दस भी हो सकते हैं। ऐसों का जड़ से विनाश आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। वसूली के उसूल का उल्लंघन करने वाला अभियुक्त सजा का सुपात्र है। कहीं कर्तव्य-पालन का ईमानदार कैंसर फैला तो हजारों जानें जाने का खतरा है?
‘सब चलता है’ के नजरिए वाले भ्रष्टचार के भुक्तभोगी है। पर वह विकसित भारत की राह में रोड़े बनने के इच्छुक नहीं है। यदि उनके चंदे या घूस के योगदान से, कुछ का जीवन-स्तर सुधर रहा है तो सुधरे। उन्हें क्यों एतराज हो? उन्हें आशा है कि एक बार विकसित भारत बना तो इस प्रकार की कुरीतियों का स्वयं अंत होगा। तब तक ‘सब चलता है’ के दृष्टिकोण से उनका जीवन सुभीते से चल रहा है। उन्हें क्यों शिकायत या असंतोष हो? कुछ को शक है, ‘सब चलता है’ का फलसफा क्या भारत को विकसित कर पाएगा?
१/५, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ-२२६००१
दूरभाष : ९४१५३४८४३८