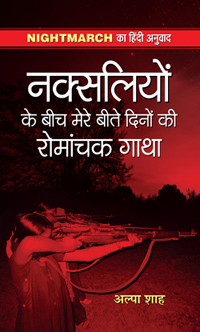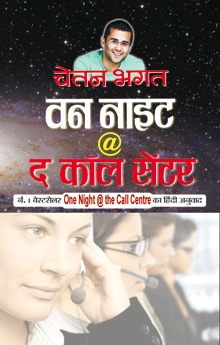RNI NO - 62112/95
ISSN - 2455-1171
ब्रह्मांड बनाम राजदंड हमारी सभ्यता के चेहरे की एक खास पहचान
भारतीय संस्कृति के अध्येता और संस्कृत भाषा के विद्वान् श्री सूर्यकांत बाली ने भारत के प्रसिद्ध हिंदी दैनिक पत्र ‘नवभारत टाइम्स’ के सहायक संपादक बनने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। राजनीतिक लेखन पर केंद्रित दो पुस्तकों ‘भारत की राजनीति के महाप्रश्न’ तथा ‘भारत के व्यक्तित्व की पहचान’ के अलावा श्री बाली की भारतीय पुराविद्या पर तीन पुस्तकें ‘कंट्रीब्यूशन ऑफ भट्टोजी दीक्षित टु संस्कृत ग्रामर’, ‘हिस्टॉरिकल ऐंड क्रिटिकल स्टडीज इन द अथर्ववेद’ और महाभारत पर केंद्रित पुस्तक ‘महाभारत : पुनर्पाठ’ प्रकाशित हुई। श्री बाली ने वैदिक कथारूपों को हिंदी में पहली बार दो उपन्यासों के रूप में प्रस्तुत किया—‘तुम कब आओगे श्यावा’ तथा ‘दीर्घतमा’। अपनी पुस्तक ‘महाभारत का धर्मसंकट’ के माध्यम से श्री बाली का यह मंतव्य बना कि यदि भारत को अपने व्यक्तित्व की ऊँचाई को समझना है तो उसे ‘धर्म’ के स्वरूप और तत्त्व पर स्वयं को केंद्रित करना ही होगा, और धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब नहीं, धर्म का मतलब है धर्म। स्मृतिशेष : ७ अप्रैल, २०२५।
उदाहरण कोई बहुत उम्दा नहीं हैं, पर उनके जरिए राजनीति के जिस सामाजिक सत्य की प्रतिष्ठा हुई, यानी पुन: प्रतिष्ठा हुई, वह भारत के चेहरे की वह पहचान है, जिस पर दो-एक बार हम पहले भी रोशनी डाल चुके हैं और फिर से इसलिए डाल रहे हैं, क्योंकि वह पहचान ही ऐसी है कि जिस पर बार-बार रोशनी डाली जानी चाहिए। पर उससे पहले दो बातें। जिन उदाहरणों का जिक्र आज हम करनेवाले हैं, वे सभी उस युग के माने जाने चाहिए, जिसे हम आज की भाषा में सतयुग अर्थात् सत्ययुग कहते हैं, पर हमारे इतिहास में जो ‘कृतयुग’ के नाम से दर्ज है। हम यह माने बैठे हैं कि सत्ययुग यानी कृतयुग में सभी तरफ अच्छाई ही अच्छाई थी, न्याय ही न्याय था, धर्म ही धर्म था और पाप का नामोनिशान नहीं था। त्रेता में जाकर थोड़ा पाप, थोड़ा अधर्म, थोड़ा असत्य शुरू हुआ, द्वापर में और बढ़ा तो कलियुग में सब ओर पाप और अधर्म ही छा गया। यह धारणा लुभावनी होने पर भी अतार्किक है, इसका पता उन कुछ लापरवाह और कुछ दुष्ट राजाओं ने दिया है, जिनके नमूने हम बस अभी पेश करने जा रहे हैं। सिद्ध यह होता है कि किसी भी युग में धर्म-अधर्म दोनों रहते हैं, पर व्यक्तियों और संस्थाओं की मर्यादाएँ इस बात से तय होती हैं कि हम इस ढंग के हालात से कैसे सुलटते हैं। दूसरी बात, भारतवर्ष को सिर्फ मूर्खताओं और झगड़ालुओं का देश माननेवालों को यह बात कहने में भरसक लुत्फ आ सकता है कि यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं और तमाम जातियाँ ब्राह्मणों के अन्याय से पीडि़त रही हैं। जो नमूने हम पेश करने जा रहे हैं, उनमें भी ब्राह्मणों ने ही क्षत्रिय राजाओं को लताड़ा (बशर्ते कि हम मान लें कि समाज तब इस तरह की जातिवादी दीवारों में बँट चुका था, जो कि हमारे हिसाब से कतई नहीं बँटा था।) पर घटना का आकलन अगर हम उसके पूरे संदर्भ में और स्थापित की गई मर्यादा और आदर्श के परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो बात कुछ और ही उभरती नजर आएगी। तो नमूने पेश किए जाएँ। ये नमूने उन राजाओं के नहीं हैं, जिन्होंने कोई बड़ा काम करके बड़ा नाम कमाया, बल्कि ऐसे लापरवाह या दुष्ट राजाओं के हैं, जिन्होंने राजा बनने के बाद या तो अपने पद से न्याय नहीं किया या उसका दुरुपयोग किया। पहला उदाहरण वेन का लिया जाए। वेन का समय पता नहीं। उसे अंग देश का राजा पुराणों में कहा गया है। उसके पुत्र का नाम पृथु था और अयोध्या का एक राजा पृथु मनु से छठी पीढ़ी से माना जाता है, तो इसलिए पृथु के पिता अनेना को वेन का पर्यायवाची मानने का एक लोभ कुछ लोगों को होता रहता है। खैर, पृथु एक महान् सम्राट् था, इस पर अगली गाथा में। पर वेन का क्या है? राजा बनने के बाद वह दंभ और अहंकार से भर गया। किसी के नाम चार कुकृत्य लिखे हों, तो बातचीत में पाँच और जुड़ जाते हैं। पुराण ग्रंथ वेन के कुकृत्यों से भरे पड़े हैं। राजा बनते ही उसने यज्ञ-याग बंद करवा दिए। वह खुद को ईश्वर का रूप मानने की हद तक दंभी हो गया। प्रजा पर अत्याचार ढानेवाले इस राजा को ऋषि लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मिलकर इसका वध कर दिया। वेन के दो पुत्र थे—पृथु और निषाद। पुराण कहते हैं कि निषाद ने जिस समुदाय का शासन किया, वे ही आगे चलकर निषाद (धीवर) कहलाए, जबकि पृथु ने वेन का उत्तराधिकार पाकर राजशासन के नए-नए मानदंड कायम किए। दूसरा नमूना पुरूरवा का है, जो मनु से तीसरी पीढ़ी का था और प्रतिष्ठान का राजा था। वह वही सम्राट् पुरूरवा है, जिसकी उर्वशी अप्सरा के साथ प्रेम-कथा पर कविकुलगुरु कालिदास ने ‘विक्रमोर्वशीय’ नामक सुंदर नाटक लिखा है। पुरूरवा अच्छा और नेक राजा था। पर उर्वशी के सौंदर्य पर मोहित होकर उसने उससे विवाह करने की ठान ली। उर्वशी कुछ शर्तों पर विवाह को राजी हो गई और एक शर्त यह थी कि कोई भी शर्त टूट जाने पर वह पुरूरवा को छोड़कर चली जाएगी। वही हुआ। पुरूरवा ने लापरवाही में शर्त तोड़ी और उर्वशी उसे छोड़कर चली गई। अब पुरूरवा उसके पीछे पागल होकर दर-दर, गाँव-गाँव, जंगल-जगंल भटकने लगा। पेड़ों से बातें करने लगा और उसका सारा राजपाट चौपट और राजकोष खाली हो गया। दरिद्र राजा ने अब जबरदस्ती प्रजा से पैसा उगाहना शुरू किया। यह बात भारतीय स्मृति में इस कदर दर्ज है कि चाणक्य तक ने अपने अर्थशास्त्र में, यानी चौथी सदी ई.पू. में, साफ-साफ लिखा है, कि राजा पुरूरवा ने प्रजा पर अत्याचार कर पैसा इकट्ठा किया। कालिदास ने बेशक अपने नाटक में पुरूरवा-उर्वशी का सुखांत वर्णन कर इस लापरवाह और बाद में अन्यायी और अनाचारी हो गए राजा की तसवीर कुछ उजली करने की कोशिश की है, पर सचाई यह है कि ऋषियों ने प्रजा की तरफ पहले लापरवाह और फिर अनाचारी हो गए इस कामांध पुरूरवा को गद्दी से उतार दिया और उसके बेटे आयु को राजा बनाया। वैसे तो निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए दो उदाहरण ही काफी हैं, पर नहुष का उदाहरण भी ले लेना चाहिए। पुरूरवा के बेटे आयु ने तो अच्छे राजा के रूप में नाम कमाया, पर उसका पुत्र नहुष अपने पिता से एकदम उलट, दुष्ट और धूर्त साबित हुआ। नहुष इतना दंभी था कि उसने खुद को इंद्र कहना शुरू कर दिया और ऋषियों को मजबूर करने लगा कि वे उसकी पालकी ढोएँ। वे बेचारे ढोते और नहुष मजे से सवारी करता। इस पूरे प्रसंग की रंग-बिरंगी कथाएँ अनेक पुराणों में मिलती हैं। ‘भागवत’, ‘देवी भागवत’ और ‘विष्णुपुराण’ के अनुसार नहुष ने एक बार पालकी में बैठे-बैठे ही एक ऋषि को लात मारकर अपनी धीमी चाल तेज करने को कहा, तो ऋषियों ने उसे पालकी से खींचकर जमीन पर दे मारा और उसके पुत्र ययाति को राजा बना दिया। तीन नमूनों में तीन बातें समान हैं। एक कि राजा दुष्ट थे, दो कि ऋषियों (आज की भाषा में बुद्धिजीवियों) ने उनका नाश कर दिया और तीन कि उनके बाद उनके पुत्रों को राजा बनाया। किसी ऋषि ने राजा को महज इसलिए नहीं मारा कि वह क्षत्रिय था और ब्राह्मण होने के नाते उन्हें उसका वध करना ही चाहिए था। अगर ऐसा होता तो फिर वे उसी के पुत्र को राजा न बनाते, बनाते तो उसे कठपुतली जरूर बनाकर रखते और अपनी उँगलियों पर नचाते। पर ऐसा नहीं कर, उसके पुत्र को राजा बनाकर वे ऋषि लोग अपने काम में जुट गए। सवाल है, ऋषियों ने ऐसा क्यों किया? क्यों राजाओं को, भले ही वे दुष्ट हो गए थे, मारकर हिंसा का पाप कमाया? जवाब में हमें फिर उस आद्य वसिष्ठ का उदाहरण याद करने का मन कर रहा है, जिन्होंने हिमालय का अपना आश्रम छोड़ा और कोसल देश की राजधानी अयोध्या में आकर इसलिए रहने लगे कि ताकि मनु द्वारा शुरू की गई राजा की संस्था अन्यायी और प्रजाविमुख होने लगे तो उसे ब्रह्मबल से रास्ते पर लाया जा सके। आद्य वसिष्ठ कितने दूरदर्शी थे, यह इसी से साबित हो जाता है कि उनका डर हिमालय से नीचे उतरने के बाद कुछ दशकों के भीतर ही सही साबित हुआ और राजा लोग प्रजा विमुख ही नहीं, प्रजा पर अत्याचार करनेवाले भी होने लगे। आद्य वसिष्ठ ने जिस जरूरत को समझा, वैसा आचरण किया और उसी का ही तो नतीजा था कि ऋषियों में वह नैतिक साहस पैदा हो सका कि उन्होंने दुष्ट राजाओं से सीधा संपर्क कर उनका नाश किया और धर्म-परायण राजाओं को प्रजा पर शासन करने का भार सौंपा। इस संदर्भ में देखेंगे तो हमें भगवान् ऋषभदेव और उनके पुत्र जड़ भरत के दार्शनिक होने का महत्त्व समझ में आ सकता है कि राजा अपने लिए नहीं, प्रजा के हित के लिए है और ऐसा राजा फिर दार्शनिक के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। सत्ता और शक्ति के शिखर पर पहुँचकर उससे पैदा हो सकनेवाले दंभ और लापरवाही से दूर रहना आसान नहीं, अगर वह ऐसा कर पाए तो यह एक ऐसी दृष्टि है, जो राजा को असामान्य बना देती है। अगर राजदंड ही निष्ठुर हो जाए, तो फिर उसका एक ही इलाज है—ब्रह्मबल, जिसके बराबर इस दुनिया में शायद दूसरा कोई बल नहीं। हो तो हमें जरूर बताइए। भारत की सभ्यता के विकास में ये तमाम उदाहरण बड़े महत्त्व के हैं। इसलिए कि इनमें से सचाई यह झाँक रही है कि इस देश की राजनीतिक और सामाजिक सोच क्या है और उसे वैसा बनाने में किन घटनाओं और व्यक्तियों ने क्या योगदान किया। भारत के स्वभाव में राजा सिर्फ इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि उसे प्रजा को हर तरह से प्रसन्न रखना है—राजा प्रकृतिरंजनात्। पर राजा से भी कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण वे हैं, जिन पर समाज की मर्यादाएँ स्थापित करने का दायित्व है। एक वेन, एक पुरूरवा, एक नहुष लापरवाह या अनाचारी हो सकता है, पर अगर देश की बुद्धि अपने नैतिक बल से युक्त रही तो फिर कैसे राजनीति मर्यादा से विमुख हो सकती है और कैसे कोई भी तूफान इस तरह की बड़ी सभ्यताओं को खत्म कर सकता है? करीब ७००० वर्ष पूर्व—गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने रचा था ऋग्वेद का पहला मंत्र अगर शरीर की तरह हमारे मन के भी रोम होते तो विश्वामित्र का नाम सुनते ही हमारे शरीर ही नहीं, मन को भी रोमांच हो आता। कोई अचानक विश्वामित्र का नाम ले ले तो बरबस याद आ जाता है, वह महापुरुष जिसने राम और लक्ष्मण को ऐसी शानदार शस्त्रविद्या दी कि न केवल दोनों भाइयों ने मारीच-सुबाहु जैसे दुर्दम्य राक्षसों का वध कर दिया बल्कि यह विश्वामित्र की दी हुई अस्त्र विद्या का ही प्रताप था कि सीता-स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष हाथोंहाथ आनन-फानन उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। रोमांच उस विश्वामित्र-कथा को सुनकर भी हो आता है, जिसमें विश्वामित्र की अभूतपूर्व तपस्या का वर्णन मिलता है कि तपोलीन मुनिवर अचानक मेनका अप्सरा के मोह में फँसकर कामलीन हो गए, जिससे एक कन्या शकुंतला का जन्म हुआ, जिसका पुरुवंशी राजा दुष्यंत से विवाह हुआ और जिन शकुंतला-दुष्यंत के पुत्र इतिहास-प्रसिद्ध भरत हुए, जिनके वंश में आगे चलकर कौरव-पांडव हुए। इतना भर तो ठीक है। पर हमारे समाज के कथानायक विश्वामित्र के साथ दो बड़े भारी अन्याय हुए हैं, इतने भारी कि उनके बोझ तले विश्वामित्र का इस देश की सभ्यता को किया गया एक अभूतपूर्व विलक्षण योगदान, यानी उनके द्वारा की गई गायत्री मंत्र की रचना को ही हम लोग भुला बैठे। एक अन्याय पुराणों ने किया है तो दूसरा अन्याय हमारे इतिहास और विचार को विकृत करने में खासी रुचि लेनेवाले पश्चिमी विद्वानों ने किया है। विश्वामित्र का वसिष्ठों से दो बार संघर्ष हुआ। एक संघर्ष अयोध्या के राजा सत्यव्रत त्रिशंकु के और उसके पुत्र हरिश्चंद्र के समय हुआ और दूसरा संघर्ष तब हुआ, जब पुरुवंशी सुदास के विरुद्ध दस राजाओं ने एक महासंघ बनाकर (दाशराज) युद्ध किया और सुदास से हारे। पहला संघर्ष विश्वामित्र ने देवराज वसिष्ठ से ब्राह्मणत्व पाने के लिए किया था और वह एक तरह से तप-संघर्ष था, जिसमें वसिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्राह्मण मानने से इनकार कर दिया। पर विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र बनाकर एक ऐसा नया अद्भुत कर्म कर दिया था कि वे पूरे देश में ब्राह्मण स्वीकार कर लिये गए और अंतत: वसिष्ठ को भी उन्हें ब्राह्मण मानना पड़ा। यह घटना मनु से करीब ग्यारह सौ वर्ष बाद की है। दूसरा संघर्ष विश्वामित्र ने शक्ति वसिष्ठ से उसकी कामधेनु गाय लेने के लिए किया, पर गाय लेने में सफल नहीं हुए। दाशराज युद्ध के समय की यह घटना राम से करीब डेढ़ सौ वर्ष बाद की है। यानी दो संघर्ष हुए और दोनों संघर्षों में तेरह सौ से ज्यादा वर्षों का अंतर है, पर पुराणों ने दोनों को मिलाकर एक कर दिया और ऐसा एक किया कि देश इस बात को भुला ही बैठा कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना कर एक नई बौद्धिक क्रांति देश में ला दी थी। दूसरा अन्याय पश्चिमी विद्वानों ने किया, जो आर्यों को एक नस्ल मानने और उनके बाहर कहीं से भारत आने के दो झूठ की तरह एक तीसरे झूठ को प्रतिष्ठित करने में लगे थे कि इस देश में ब्राह्मण और क्षत्रिय हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। वसिष्ठ (ब्राह्मण) और विश्वामित्र (क्षत्रिय) के संघर्ष को वे इसका सबसे पुराना उदाहरण बनाकर परोसते रहे और झूठ के दबाव में हमारे विद्वान् याद ही नहीं कर पाए कि विश्वामित्र ने आखिर इस देश को दिया क्या! थोड़ा आगे बढ़ें, इससे पहले फुटनोट के तौर पर दो बातें जान लेने में कोई हर्ज नहीं। विश्वामित्र-मेनका का प्रसंग पुराणों के जरिए हमारे जहन में आज तक बसा है। हालाँकि इतिहास के क्रम में उसे फिट करने में कई दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें भुला दें तो यह प्रसंग पहले यानी गायत्री मंत्र बनानेवाले विश्वामित्र का हो सकता है, जो उनके जीवन के उत्तरार्ध में कहीं घटा होगा और जिन विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को शिक्षा दी थी, वे उस विश्वामित्र के पूर्ववर्ती होंगे जिन्होंने शक्ति वसिष्ठ से कामधेनु के लिए संघर्ष किया। जाहिर है कि जिस तरह वसिष्ठों की एक कुल परंपरा है, जिसमें सभी को वसिष्ठ कहा जाता है। वैसे ही विश्वामित्रों की भी एक पूरी वंश परंपरा है जहाँ सभी को विश्वामित्र कहा जाता है। दोनों ही सप्तर्षियों में गिने जाते हैं, पर दोनों के कालक्रम में फर्क यह है कि जहाँ वसिष्ठों की नामावली मनु के एकदम बाद हुए राजा इक्ष्वाकु के समय से ही, यानी आज से आठ हजार साल पहले से मिलना शुरू हो जाती है वहाँ विश्वामित्र के कुल का प्रारंभ उससे ग्यारह सौ वर्ष बाद यानी आज से करीब सात हजार साल पहले होता है। और अगर युगों का एक साधारण, लगभग, अनुमान लगाना हो तो कह सकते हैं कि वसिष्ठों का उदय कृतयुग अर्थात् सत्ययुग के शुरू में हुआ तो विश्वामित्रों के उदय के साथ ही त्रेतायुग की भी शुरुआत होती है, जब इस देश के महामंत्र गायत्री मंत्र की रचना हुई। इस पृष्ठभूमि के बाद अब आराम से आगे बढ़ा जा सकता है। प्रथम विश्वामित्र की कथा वास्तव में संघर्ष के महत्त्व की, संकल्प की, अदम्यता की, इच्छाशक्ति के प्राबल्य की और मन की अपराजेयता की वह कथा है, जिसमें आग से तपकर निखरे सोने की तरह विश्वामित्र ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए घोर मानसिक और बौद्धिक तप किया और विजय पाई। इन महान् विश्वामित्र का असली पहला नाम विश्वरथ था। वे राजा कुशिक के पुत्र थे और पिता के बाद खुद कान्यकुब्ज के शासक बने। कुछ विवरणों के मुताबिक वे कुशिक के पौत्र व गाथिन के पुत्र थे। जब विश्वरथ कान्यकुब्ज (आज के कन्नौज) पर शासन कर रहे थे, तब अयोध्या में सत्यव्रत का राज चल रहा था, जिसे हम त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। बस इसमें मजेदार बात यह है कि विश्वरथ और सत्यव्रत त्रिशंकु गहरे दोस्त थे और अपनी-अपनी तरह के जबरदस्त झक्की भी थे। विश्वरथ की राजकाज में कोई खास रुचि थी नहीं और हर वक्त बौद्धिकता में लीन रहनेवाले विश्वरथ की महत्त्वाकांक्षा एक ही थी कि उन्हें ब्राह्मण मान लिया जाए। पर वक्त के सर्वाधिक पूजनीय ऋषि कुल के प्रमुख देवराज वसिष्ठ को यह बात स्वीकार नहीं थी। तर्क यह था कि पहले तपस्या करके दिखाओ तो ब्राह्मण मानने की बात उठे। उधर सत्यव्रत त्रिशंकु की झक यह थी कि उसके कुलगुरु देवराज वसिष्ठ कुछ ऐसा यज्ञ करें कि वह (त्रिशंकु) सीधा अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग पहुँच जाए। देवराज वसिष्ठ ने मना कर दिया। यानी विश्वरथ और त्रिशंकु दोनों मन मसोसकर रह गए और दोनों का कारण एक ही था—देवराज वसिष्ठ। त्रिशंकु तो कुछ कर नहीं पाया, पर विश्वरथ ने ठान ली कि यह राजकाज क्या होता है? तप करेंगे और ऐसा तप करेंगे कि वसिष्ठ को आखिर उन्हें ब्राह्मण मानना ही पड़ेगा। तय करते ही विश्वरथ ने राजपाट त्याग दिया और ऐसा त्यागा कि उनके बाद कान्यकुब्ज का कोई उस समय का राजवंश ही नहीं मिलता। वे अपने परिवार को लेकर आज के गुजरात-सौराष्ट्र इलाके में, जिसे उन दिनों सागरानूप कहा जाता था, चले गए। वहाँ लंबी तपस्या करने के बाद भी जब वसिष्ठ ने उन्हें ब्राह्मण नहीं माना तो विश्वरथ ने, जो अब तक विश्वामित्र हो चुके थे, कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर रूषुंग तीर्थ पर तपस्या का एक दूसरा दौर चलाया। वसिष्ठ को उससे भी संतोष शायद नहीं हुआ। विश्वामित्र भला कहाँ माननेवाले थे? वे राजस्थान के अजमेर (अजयमेरु) इलाके में पुष्कर तीर्थ पर सविता (सूर्य) की उपासना में लग गए और वहीं उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की—ॐ भूभुर्व: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न: प्रचोदयात् अर्थात् हम सूर्य के परम तेज पर ध्यान लगाते हैं, जो हमें बुद्धि प्रदान करे। इस मंत्र रचना के समय तक वसिष्ठ ने विश्वामित्र को राजर्षि तो मान लिया था, पर चौबीस अक्षरोंवाले इस गायत्री मंत्र का असर इतना विलक्षण था कि जब जनसामान्य में इस मंत्र का चलन हो गया तो बरबस वसिष्ठ को उन्हें ब्राह्मण मानना पड़ा। ऐसी क्या बात थी इस मंत्र में? थी, तभी तो यह मंत्र हिमालय से समुद्र तक और सिंधु सेज्ञ् ब्रह्मपुत्र तक सारे भारत के लोगों का अपना एक स्वाभाविक मंत्र बन गया है जैसा कि कोई दूसरा मंत्र नहीं बन पाया है। मनु ने आज से आठ हजार साल पहले यज्ञ संस्था की शुरुआत की। उनके साथ ही गद्य में लिखे जानेवाले यजुष मत्रों की रचना शुरू हुई जो यजुर्वेद में संकलित हैं। पर मनु के करीब ग्यारह सौ वर्ष बाद यानी आज से करीब सात हजार वर्ष पहले त्रेतायुग के आरंभ के आस-पास विश्वामित्र ने पहली बार एक ऐसा मंत्र रचा जो कविता में, ऋचा में, छंद में था, जिसमें चौबीस अक्षर थे, जिसमें गेयता थी और जो यज्ञ के लिए नहीं, बल्कि सूर्य से बुद्धि की तीव्रता की प्रार्थना के लिए रचा गया था। वह गेय यानी गाने लायक था, इसलिए उसे गायत्री कहा गया और गाने लायक होने के कारण वह लोगों की जुबान पर सहसा चढ़ गया और आज तक चढ़ा हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के ६२वें सूक्त (३.६२) में संकलित हैं। तो कैसे मालूम पड़ा कि यह पहली ऋचा है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है? ऋग्वेद के करीब दस हजार मंत्रों का संकलन करीब एक हजार सूक्तों में है। इन सूक्तों की रचना जिन ऋषियों द्वारा की गई है, शोधकर्ताओं ने गहरा अनुसंधान करके उनका कालक्रम तय किया है और उस शृंखला में हमारे महानायक विश्वामित्र का नाम सर्वप्राचीन है, जिनका पहला मंत्र गायत्री है। वैसे तो वसिष्ठों का उदय विश्वामित्रों से एक हजार साल पहले हो चुका था, पर वसिष्ठों ने यानी वसिष्ठ कुल के मैत्रावरुण वसिष्ठ ने पहला सूक्त विश्वामित्र के भी करीब तेरह सौ साल बाद अर्थात् दाशराज युद्ध के बाद रचा (ऋग्वेद ७.२२)। ऋग्वेद की पोथी खोलेंगे तो उसमें आगे पहला मंत्र कोई और ही नजर आएगा। पर याद रहना चाहिए कि वेदों में मंत्रों का संकलन कालक्रमानुसार नहीं है। क्रम किस आधार पर तय हुआ, वेदव्यास के मन में इस क्रम को बनाने का क्या कारण था, इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। पर आज लोगों ने रिसर्च कर डाली है और उसी रिसर्च ने विश्वामित्र को ढूँढ़ निकाला है, जिसने हम भारतवासियों को ऋग्वेद का पहला गायत्री मंत्र दिया। तो धन्य कौन हुआ—विश्वामित्र या हम या हमारा भारत देश? जवाब है—सभी। (प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक ‘भारत गाथा’ से साभार)
|
मई |