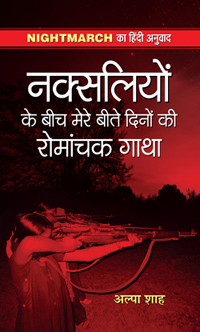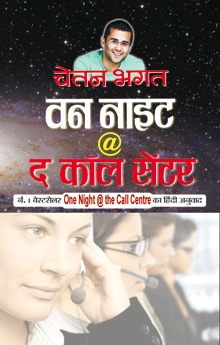RNI NO - 62112/95
ISSN - 2455-1171
मंदिरों का शहर है मदुरै
चितरंजन भारती मदुरै का नाम काफी समय से सुनता आया था। द्रविड़ संस्कृति का केंद्र मदुरै भारतीय इतिहास में अपनी विशिष्ट अहमियत रखता है। वह इस मायने में कि अतीत में इसने अनेक राजवंशों का उत्थान-पतन झेला है। ११वीं शती तक यहाँ पांड्य राजवंश का शासन रहा। बाद में चोल वंश का शासन आरंभ हुआ। फिर यह विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। विजयनगर का पराभव बहमनी शासन में हुआ। यह वह समय था, जब दिल्ली में मुगल सम्राट् अकबर का अभ्युदय हो रहा था। इसी समय ‘नायक’ वंशावली के साथ तेलुगु मूल के राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने आधुनिक तमिलनाडु के वृहत् क्षेत्र में शासन किया। यह अलग बात है कि एकाधिक बार राजधानी को मदुरै से हटाकर तिरूचिरापल्ली भी ले जाया गया। चूँकि उस वक्त तक फ्रांसीसी और ब्रिटिशों ने इस इलाके में प्रविष्ट नहीं हुए थे, मुख्य रूप से डच और पुर्तगाल द्वारा यहाँ से व्यापार किया जाता था। मदुरै स्थित अमेरिकन कॉलेज में उसके केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ, तमिलनाडु के संयुक्त तत्त्वावधान में ‘राष्ट्रीय एकता में भारतीय भाषाओं का योगदान’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हेतु जब मुझे आमंत्रित किया गया, तो स्वयं को रोक नहीं पाया। हिंदी एवं तमिल भाषा की विदुषी डॉ. भवानी अश्विनी कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष, अमेरिकन कॉलेज, मदुरै के आवास पर हम १० अक्तूबर को सपरिवार पहुँच गए। हालाँकि हमारे लिए होटल आवंटित थे। फिर भी हमने उन्हीं के आवास पर रुकना पसंद किया, ताकि तमिल संस्कृति को बेहतर समझ सकें। सुबह में जब हम ट्रेन से उतरे, तो स्टेशन की साफ-सफाई से चकित थे। अब स्टेशन है, तो उसका विशाल प्रांगण होगा ही, जिसे कई खंडों में बाँट दिया गया था। वहीं एक गणेश मंदिर था, जिसके बाहर पुजारी खड़े थे। शुभ की आकांक्षा रखे यात्री भक्तगण आते और प्रणाम करते। निःस्पृह भाव से पुजारी उन्हें भस्म-कुंकुम का तिलक लगाते। महिलाएँ आमतौर पर वहीं गजरा बेचने बैठी महिला से गजरा खरीदतीं और गणेश को अर्पित कराने के बाद ही अपने बालों में लगातीं। पुजारी उन्हें भस्म-कुंकुम देता, जिसे स्वयं लगातीं। यह तिलक भी किसी के लिए लंबवत् होता, तो किसी के लिए टीके के रूप में सजता। जैसी जिसकी श्रद्धा। चढ़ावे और दान के लिए कोई आग्रह नहीं, दुराग्रह तो छोड़ ही दें। स्टेशन परिसर में नीम के पेड़ ही पेड़ हैं, जिन्हें देख मैं चकित था। वैसे ये नीम के पेड़ पूरे शहर में हैं, हर कहीं, हर जगह दिखे। दूसरे फलदार पेड़ भी हैं और इमारती लकड़ियों के भी हैं। मगर यहाँ जैसे नीम का साम्राज्य है। हमारे एक मित्र ने जानकारी दी कि नीम के पेड़ पूरे तमिलनाडु में मिलेंगे। यहाँ इस पेड़ को वही दर्जा है, जो उत्तर भारत में पीपल को दिया जाता है। वैगेई नदी के तट पर हजारों वर्ष के प्राचीन शहर को कमल की आकृति में बसाया गया है। इसलिए इसे ‘लोटस सिटी’ भी कहा जाता है। अमेरिकन कॉलेज का विशाल परिसर जैसे पुराने दिनों को अभी भी स्वयं में समेटे हुए है। किन्हीं पार्कों के समूहों में रचा-बसा है यह कॉलेज। लाल रंगवाले बजरी से बने और रँगे सैकड़ों वर्ष पूर्व १८५१ ई. में निर्मित भवनों को देखकर ही इसकी भव्यता का अहसास होता है। हालाँकि कुछ अन्य नए भवन भी निर्मित किए जा रहे हैं। गूगल समूह के सी.ई.ओ. सुंदर पिचाई यहीं के छात्र रह चुके हैं। वैसे अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों ने भी यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। साफ-सफाई का सुंदर प्रबंध है। पार्किंग में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की भरमार को देखकर ही इस कॉलेज की विशिष्टता का अनुमान हो गया था। मुख्य फाटक पर ही चुस्त-दुरुस्त गार्डों की तत्परता और सजगता देखते बनती थी। स्पष्ट है, आरंभ ही अनुशासन से है, तो आगे भी उसका बने रहना ही है। छात्र-छात्राओं के झुंड-के-झुंड आ-जा रहे थे। मगर कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शोरगुल नहीं। ठीक सुबह दस बजे तक आयोजन हॉल का दर्शक दीर्घा भर चुका था। नियत समय पर दि अमेरिकन कॉलेज, मदुरै के प्राचार्य डॉ. दवमणि क्रिस्टोबर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी ने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि डॉ. पी. राधिका, कुलपति, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, चेन्नै एवं मुख्य अतिथि डॉ शैलेंद्रनाथ मिश्र, हिंदी विभागाध्यक्ष, श्रीलाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोंडा, उ.प्र. ने उनका साथ दिया। तत्पश्चात् मेरे द्वारा संगोष्ठी विषय ‘राष्ट्रीय एकता में भारतीय भाषाओं का योगदान’ पर बीज वक्तव्य दिया गया। इस कड़ी को क्रमशः डॉ. एम. ब्यूला रूबी कमलम, प्राध्यापक, अमेरिकन कॉलेज, डॉ. एम. शाहुल हमीद, हिंदी विभागाध्यक्ष, अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं डॉ. एस. मंजुनाथ, हिंदी विभागाध्यक्ष, कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज, बैंगलुरु ने आगे बढ़ाया। कार्यक्रम के बीच डॉ. राजलक्ष्मी कृष्णन, हिंदीसेवी, चेन्नै की पुस्तक ‘उत्कृष्ट तमिल साहित्य और संस्कृति’ एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा की पत्रिका ‘समन्वय दक्षिण’ के ‘सुब्रह्मण्यम भारती विशेषांक’ का लोकार्पण हुआ। ‘राष्ट्रीय एकता में भारतीय भाषाओं का योगदान’ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन ‘गंगा-कावेरी व्याख्यान माला’ के अंतर्गत किया गया था। सो इस अवसर पर ‘गंगा-कावेरी व्याख्यान माला’ के आयोजकों को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ, तमिलनाडु द्वारा सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में ‘राष्ट्रीय एकता में भारतीय भाषाओं का योगदान’ विषयक सत्र की अध्यक्षता डॉ. बीना शर्मा, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा किया गया। इस विषय पर तमिलनाडु-केरल के छह विद्वानों द्वारा परचे पढ़े गए। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. जयशंकर तिवारी, हिंदी विभागाध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोंडा उपस्थित रहकर विशद् जानकारी दी। ‘राष्ट्रीय एकता में भारतीय संतों का योगदान’ अगले सत्र का विषय था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. राजलक्ष्मी कृष्णन, हिंदीसेवी, चेन्नै ने की। यहाँ भी छह पर्चे पढ़े गए। जबकि मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉ. जयशंकर बाबू, हिंदी विभागाध्यक्ष, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी ने विषय को उत्तर-दक्षिण एकता के रूप में देखने का आग्रह किया। कार्यक्रम में रोचकता बनी रहे, इसका भी जैसे ध्यान रखा गया था। इसलिए अगले सत्र का विषय था, ‘राष्ट्रीय एकता में फिल्मों का योगदान’। विषय के अनुरूप श्रोताओं ने इसमें अपनी रुचि प्रदर्शित की। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. शशिप्रभा जैन, हिंदी विभागाध्यक्ष, अविनाश्विलिंगम विश्वविद्यालय, कोयंबतूर ने की। जबकि मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. आर. जयचंद्रन, निदेशक, स्कूल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम थे। संध्या समय कार्यक्रम के अंत में डॉ. ज्ञानचंद मर्मज्ञ, बैंगलुरु की अध्यक्षता में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन डॉ. सतीश कुमार ने किया। अगले दिन कार्यक्रम का आरंभ सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ, क्योंकि अब सभी एक-दूसरे से सुपरिचित थे। ‘राष्ट्रीय एकता में भारतीय कवियों का योगदान’ सत्र की अध्यक्षता डॉ. राजरत्नम्, हिंदी विभागाध्यक्ष, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवारूर, तमिलनाडु ने किया। इस विषय पर तमिलनाडु-केरल के छह विद्वानों द्वारा परचे पढ़े गए। जबकि मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. बी.एल. आच्छा, वरिष्ठ साहित्यकार, चेन्नै ने रोचक मगर सारगर्भित जानकारी दी। इसी क्रम में अगला सत्र आरंभ हुआ, जिसका विषय था ‘राष्ट्रीय एकता में भारतीय गौरव ग्रंथों का योगदान’। इसकी अध्यक्षता डॉ. जी. रविशंकर, भाषाविज्ञान प्राध्यापक, पांडिचेरी सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी स्टडीज, पांडिचेरी ने की। यहाँ भी छह परचे पढ़े गए। मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. सलीम बैग, हिंदी विभागाध्यक्ष, गांधीधाम विश्वविद्यालय, दिंडीगल, तमिलनाडु ने अपने वक्तव्य में महत्त्वपूर्ण जानकारी दी। ‘राष्ट्रीय एकता में क्रांतिकारियों का योगदान’, यह एक लीक से हटकर विषय था, सो स्वाभाविक ही मत-वैभिन्न्य देखने को मिले। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. लता चौहान, हिंदी विभागाध्यक्ष, बैंगलुरु ने की। जबकि मुख्य वक्ता के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. वी.एच. विट्ठादेव उपस्थित थे। उन्होंने विषय की बारिकियों में जाकर इस विषय की गंभीरता से सबको अवगत कराया। विद्वत्ता हमेशा सीमाहीन और गरिमामयी होती है। और इसको जैसे डॉ. गंगाधर वानोडे, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हैदराबाद, डॉ. विजय भास्कर नायडू, हिंदी विभागाध्यक्ष, जानकी अम्माल महाविद्यालय, शिवकाशी, तमिलनाडु, डॉ. जगन्नाथ रेड्डी, हिंदी विभागाध्यक्ष, अण्णमलै विश्वविद्यालय, चितंबरम्, तमिलनाडु, डॉ. पी. बालमुरूगन, वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोयंबतूर ने अपने वक्तव्यों से सिद्ध किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉ. ए. भवानी, हिंदी प्राध्यापक, अमेरिकन कॉलेज, मदुरै द्वारा किया गया। इतिहासकारों के मतानुसार प्राचीन काल में यानी ई.पू. ० में मदुरै राज्य का रोम एवं यूनानी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन आख्यानों के अनुसार पांड्य राजा मलयध्वज की पुत्री मीनाक्षी के साथ विवाह के लिए आदिदेव शिव सुंदरेश्वर के रूप में यहाँ आए थे। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने यहाँ आकर अमृत वर्षा की थी। मदुराई नाम ‘मधुरा’ शब्द से निकला, जिसका अर्थ है—मिठास। मान्यता है कि यह मिठास शिव द्वारा किए गए अमृत-वर्षा से उत्पन्न हुई। इस प्रकार इस शहर का नामकरण ‘मदुरै’ हो गया। दक्षिण भारत में सौंदर्य-प्रसाधन के रूप में हल्दी का उपयोग सभी अविवाहित-विवाहित महिलाएँ करती हैं। ऐसी मान्यता है कि आदिदेव गौरवर्णी थे, जबकि पार्वती द्रविड़, श्यामा-सुंदरी थीं। उनके सौंदर्य के निखार के लिए उनपर हल्दी का उबटन लगाया गया था। अब काले और पीले रंग का सामंजस्य होगा, तो प्रकाश में वह हरे रंग का दिखता है। और इस प्रकार पार्वती के सौंदर्य में निखार लाया गया। इसलिए यहाँ मीनाक्षी देवी हरे रूप में दिखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित पार्वती का विग्रह एमराल्ड अर्थात् पन्ना पत्थर (रत्न) से निर्मित है, जो हरे रंग का ही होता है। महिला हो अथवा पुरुष, प्रतीक स्वरूप चंदन के साथ हल्दी का तिलक लगाना इसलिए यहाँ सामान्य बात है। वैसे तिलक तो कमल के डंठल से निर्मित कुंकुम का भी लगाया जाता है। शिव-पार्वती का धूमधाम से विवाह हुआ था। इस परंपरा का निर्वाह यहाँ के मीनाक्षी मंदिर में प्रतिवर्ष किया जाता है। मीनाक्षी मंदिर मूलतः मीनाक्षी यानी देवी पार्वती एवं भगवान् शिव को समर्पित है। शिव यहाँ सुंदरेश्वर स्वरूप में विराजमान हैं। मदुरै शहर का प्रमुख आकर्षण है—द्रविड़ शैली का विशाल मीनाक्षी मंदिर। इस मंदिर को देवी पार्वती के के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। अन्य प्रमुख स्थानों में कांचीपुरम् का कामाक्षी मंदिर एवं वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का स्थापत्य और वास्तु आश्चर्यचकित करनेवाला है, इसलिए इसकी गणना विश्व के सात आश्चर्यों में की जाती है। इसी से इस विश्व धरोहर की महत्ता का आकलन किया जा सकता है। इस इमारत समूह में १२ गोपुरम् हैं, जिनके कठोर प्रश्तरों पर की गई महीन शिल्पकारी कर उन्हें रंग-रोगन लगाकर चित्रकारी की गई है। इसका विशद् वर्णन तमिल के पुरातन संगम साहित्य में है और इसी से इसकी पुरातनता का अंदाज लगाया जा सकता है। हालाँकि वर्तमान में जो निर्माण दिखता है, वह १७वीं शताब्दी का बताया जाता है। मंदिर का गर्भगृह ३५०० वर्ष पुराना है। जबकि बाहरी दीवारें और अन्य बाह्य निर्माण, अर्थात् गोपुरम् और चहारदीवारी आदि का अनुमान है कि वे १५००-२००० वर्ष पुराने हैं। यह सभी लगभग ४५ एकड़ में है, जिसकी लंबाई २५४ मीटर और चौड़ाई २३७ मीटर है। अब मंदिर है, तो जल-स्रोत रहेगा ही। मंदिर परिसर के अंदर एक १६५ फीट लंबा और १२० फीट चौड़ा सरोवर है, जिसका नाम ‘पोत्र करै कूलम’ है। तमिल धारणा के अनुसार साहित्य परखने का उत्तम स्थल है। प्राचीन समय में लेखक अपनी पांडुलिपियाँ लाते और इस सरोवर में इस धारणा के अनुसार डाल देते थे कि यदि वह उत्तम साहित्य होगा, तो तैरता रहेगा। निम्न साहित्य होगा, तो डूब जाएगा। मंदिर परिसर में सहस्र स्तंभ मंडपम् यानी हजार खंभों वाला विशाल मंडप है। सभी खंभे विशाल पत्थरों पर तराशे हुए हैं, जिनमें फूल-पत्ती से लेकर देवी-देवता उत्कीर्ण हैं। इस मंडप के बाहर पश्चिम की ओर संगीतमय स्तंभ है। इन स्तंभों की रचना विस्मयकारी इस रूप में है कि प्रत्येक स्तंभ पर थाप देने पर भिन्न-भिन्न स्वर निकलते हैं। ठीक ही मदुरै मंदिर शिव-पार्वती को समर्पित है। लेकिन तमिलों के मुख्य आराध्य सौंदर्य, शक्ति, श्रम के साधक कार्तिकेय ही हैं। पौराणिक कथानुसार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने पर खिन्न कार्तिक का प्रश्न है—क्या श्रम तुच्छ है? मगर शिव-पार्वती वचनबद्ध हैं। तत्काल कोई जवाब नहीं सूझता। यह महत्त्वपूर्ण ही नहीं, अनुत्तरित प्रश्न है कि श्रम श्रेष्ठ है या बुद्धि? हमारी वर्ण-व्यवस्था भी संभवतः इसी बुद्धि पर टिकी है। दूर क्यों जाएँ, हमारे नेता तिलक ने बुद्धि को श्रेष्ठ मानते गणेश-पूजन को ही राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया। अंततः फल तो गणेश को ही मिलता है। ऋद्धि-सिद्धि के साथ गणेश का विवाह हो चुका है। अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर वह अपने वाहन मयूर से दक्षिण की ओर प्रयाण कर देते हैं। दक्षिण यानी द्रविड़ प्रदेश में उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ श्रम की महिमा थी। यहाँ की पथरीली मिट्टी म& |
मई |