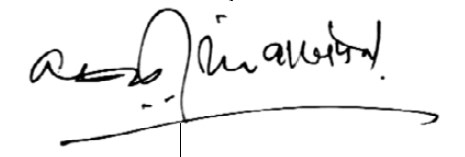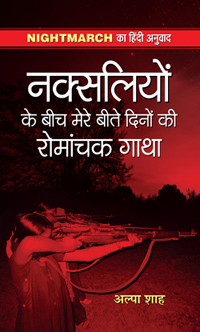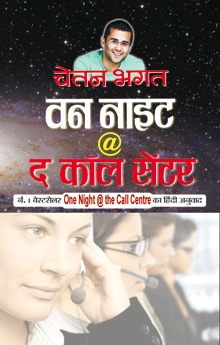RNI NO - 62112/95
ISSN - 2455-1171
पसीने के दस्तावेजकिसी कवि ने कहा था—ये ताज अजंता बोकारो...हैं दस्तावेज पसीने के! पूरे विश्व में जितनी भी विशालकाय इमारतें हैं, मीनाक्षी मंदिर या ताजमहल जैसे वास्तुकला के प्रतिमान हैं या पुल या बाँध या कारखाने आदि हैं, सब पसीने के ही दस्तावेज हैं। ये सब लाखों श्रमिकों के अनथक परिश्रम का ही परिणाम हैं। जब लाखों पर्यटक किसी किले या मंदिर या अन्य अनूठी इमारत को देखते हैं, तो क्या उनमें से एक प्रतिशत के भी मन में इन्हें बनानेवाले श्रमिकों के योगदान की ओर ध्यान जाता होगा। हमारा रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह श्रमिकों के श्रम पर ही निर्भर है, चाहे वह श्रम खेतों में किया गया हो या मंडियों में सूर्योदय के पहले ही सब्जी-फल ढोने में। यह ठीक है कि मशीनों की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन श्रमिकों के बिना जीवन संभव नहीं। महाप्राण निराला की कालजयी कविता के अंश याद आते हैं, जो एक महिला श्रमिक पर रची गई थी— वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर ... ... ... चढ़ रही थी धूप गरमियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू रुई ज्यों जलती हुई भू गर्द चिनगीं छा गई प्रायः हुई दुपहर वह तोड़ती पत्थर बहुत सारे कानून बने, श्रम कल्याण के प्रावधान किए गए, किंतु श्रमिकों के जीवन में बहुत अधिक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ पाया। सबसे बड़ा संकट यही है कि अधिकांश श्रमिक गैर-संगठित क्षेत्र में हैं। जो संगठित क्षेत्र में हैं, वहाँ तो ट्रेड यूनियन आदि के कारण बहुत से सकारात्मक बदलाव संभव हो गए, किंतु गैर-संगठित क्षेत्रों में जीवन की अनिश्चितता, असुरक्षा, शोषण, उत्पीड़न का सिलसिला बना रहा। न उनके काम के घंटों का कोई हिसाब है, न किसी प्रकार की सुविधाओं का, यहाँ तक कि महिला श्रमिक यदि अपने बच्चे को पोलियो से बचाव के लिए टीकाकरण केंद्र गई, तो उसके आधे दिन का पैसा काट लिया गया। गैर-संगठित क्षेत्रों के श्रमिक महानगरों तथा नगरों में बहुत गंदी बस्तियों में रहने को विवश होते हैं। कोरोना के दौरान हजारों श्रमिक जिस प्रकार सैकड़ों मील दूर अपने गाँवों में लौटने को विवश हुए, वह भी एक समाज के रूप में भारत के लिए बहुत दुःखद अध्याय रहा। अशिक्षा अभी भी शोषण-उत्पीड़न का कारण बनी हुई है। बालश्रम तो देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। कौन नहीं जानता कि एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो वह उच्च-से-उच्च पद को सुशोभित कर सकता है, किंतु अभी भी लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। कहीं भी राष्ट्रीय राजमार्ग के होटल, ढाबों में देखिए तो बच्चे ही चाय लाते, बरतन धोते मिल जाएँगे। जोखिम भरे व्यवसायों में प्रतिबंध के बावजूद हजारों बच्चे काम करके अपने परिवारों का भरण-पोषण करने को अभिशप्त हैं। बालश्रमिकों के पुनर्वास की योजनाएँ जिस गति से चलती हैं, उस गति से तो भारत को बालश्रम से मुक्ति पाने में न जाने कितने दशक लग जाएँगे। बालश्रम से मुक्ति तो तभी संभव है, जब पूरी संवेदनशीलता से सरकारें विशेष अभियान चलाएँ। बच्चे तो किसी भी देश की बहमूल्य पूँजी हैं, देश का भविष्य हैं। यदि बच्चे किताब-कॉपी या खेल-खिलौनों से वंचित होकर श्रमिक बनकर शोषण-उत्पीड़न के शिकार होते हैं तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। यह भी कटु सत्य है कि बालश्रमिक ढाबे, होटल-मालिकों या छोटे उद्योग चलाने वालों को बहुत सुविधाजनक लगते हैं, क्योंकि वे चुपचाप डाँट-मार भी सह लेते हैं और किसी प्रकार की माँग भी नहीं रखते तथा उन्हें मजदूरी भी कम देनी पड़ती है। अब जबकि स्वाधीनता के सौ वर्ष तक हमने विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है, तो हमें बालश्रम से मुक्ति पानी ही होगी और यह कार्य कोई एक-दो वर्षों में हो पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए भी एक नई सोच के साथ योजनाएँ बनानी होंगी कि वे भी शोषण, दमन, उत्पीड़न आदि से मुक्त होकर सम्मान एवं सुरक्षा का जीवन बिता सकें। इस संदर्भ में कवियों, लेखकों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। हिंदी की मुख्यधारा के साहित्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा बालश्रमिकों के शोषण, उत्पीड़न, दमन व नारकीय जीवन की पीड़ाओं को कितना स्थान मिला है, यह विचारणीय है। चित्रा मुद्गल के लोकप्रिय उपन्यास ‘आवाँ’ में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दशा, ट्रेड यूनियनों और आपसी टकराव से उपजी विकृतियों आदि का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और बालश्रमिकों के पुनर्वास के लिए अभी अनेक कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों आदि की आवश्यकता होगी। विकासशील देश का मीडिया टेलीविजन तो अब घर-घर पहुँच गया है। स्वाभाविक है कि उसकी पहुँच करोड़ों लोगों तक है और इस कारण राष्ट्र-निर्माण में उसका योगदान कितना हो सकता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर एक विकासशील देश में, जहाँ करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे हों, करोड़ों लोग निरक्षर हों, जहाँ तरह-तरह की समस्याएँ हों, चुनौतियाँ हों, वहाँ मीडिया का स्वरूप कैसा हो, यह भी बताना कठिन नहीं है। यदि दूरदर्शन तथा संसद् टी.वी. को लगभग ९०० चैनलों की भीड़ से अलग कर दें, जिनका लक्ष्य ‘जन-सेवा प्रसारण’ है, तो हमें चैनलों की पत्रकारिता का गंभीर आकलन करने की आवश्यकता है। आइए, पहले अपनी महान् सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं। भारत जैसे विराट्, विशाल उपमहाद्वीप में जहाँ इतनी विविधता है, सैकड़ों भाषाएँ हैं, हजारों बोलियाँ हैं, जहाँ कण-कण में संगीत है, लाखों लोकगीत हैं, लोकनाट्य हैं, लोक-उत्सव हैं, मेले हैं, सैकड़ों कलारूप हैं, विविध लोक त्योहार हैं, वहाँ के चैनल इस धरोहर को संरक्षित करने में, उसका प्रसार करने में अपना दायित्व कितना निभा रहे हैं, इसकी पड़ताल करते हैं! आपको ऐसे कितने टी.वी. चैनलों की जानकारी है, जहाँ आप भारत के महान् शास्त्रीय गायकों के गायन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं? आपको ऐसे कितने टी.वी. चैनलों की जानकारी है, जहाँ आप सुगम संगीत, यानी गैर-फिल्मी गीत-गजलों की प्रस्तुति देख-सुन सकते हैं! किस टी.वी. चैनल से आप कविताएँ, कहानियाँ आदि सुन सकते हैं? एकाध अपवाद को छोड़कर उत्तर अत्यंत निराशाजनक ही मिलेगा। सैकड़ों चैनलों में साहित्य, संगीत, कला को स्थान न हो तो यह दुःखद ही नहीं, निजी चैनलों के लिए शर्म की बात है। कुछ चैनलों पर कविता के नाम पर जो कुछ प्रसारित होता है, वह मनोरंजन भले ही कराता है, पर वह साहित्य से कोसों दूर है। संस्कृति से हटकर अब सामाजिक क्षेत्र की ओर ध्यान दें तो देश की ज्वलंत समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में चैनलों के कार्यक्रमों को परखते हैं—अापने कितने टी.वी. चैनलों पर बालश्रम पर चर्चा देखी है, जिसका संबंध करोड़ों बच्चों के बहुमूल्य जीवन से है। कितने टी.वी. चैनलों से आपने महिला सुरक्षा पर चर्चा सुनी है कि ‘यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते’ वाले देश में बच्चियाँ तक असुरक्षित क्यों हैं? जब कोई गंभीर अपराध घट जाता है, तब भले ही कुछ बहस हो जाए, जो प्रायः राजनीतिक कटुता से भरी होती है। आपने कितने टी.वी. चैनलों से किसानों की स्थितियों पर कोई बहस या चर्चा सुनी है कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो? आपने कितने टी.वी. चैनलों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई चर्चा सुनी है? भारत में लगभग डेढ़ लाख लोग हर वर्ष सड़कों पर दम तोड़ देते हैं, जीवनभर को अपाहिज हो जाते हैं, अरबों रुपयों की देश की क्षति होती है। सही व्यवस्थाएँ करके इन मौतों को कम किया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में हर वर्ष जितने लोग हमारे देश में मरते हैं, उतनी तो दर्जनभर छोटे देशों की आबादी भी नहीं है। आपने कभी किसी टी.वी. चैनल से राजनीति में अपराधियों के वर्चस्व पर या चुनाव सुधारों पर कोई सार्थक चर्चा सुनी है? आपने कभी टी.वी. चैनलों से शिक्षा के क्षेत्र में या न्याय-व्यवस्था के क्षेत्र में जरूरी सुधारों पर सार्थक गंभीर चर्चा सुनी है? ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हिंदी का टी.वी. मीडिया टी.आर.पी. की होड़ में या सनसनी के उद्देश्य से कितने बचकाने या हास्यास्पद कार्यक्रम करता है कि अफसोस के साथ-साथ चिंता भी होती है। वह क्रिकेट मैच के परिणाम पर एक दर्जन ज्योतिषी बुला लेता है और भारत की जीत के सपने बेचता है, किंतु मैच में भारत न केवल हारता है वरन् बुरी तरह हारता है। कितनी बार चैनलों ने झूठ परोसा है, घृणा परोसी है, अदालतों से फटकार सुनी है, क्षमा माँगी है किंतु उनके रवैये में कोई सुधार नजर नहीं आता। एक दुर्दांत अपराधी को गुजरात से प्रयागराज लाए जाने की पल-पल की यात्रा को ऐसे दिखाया गया, जैसे अब इतने बड़े देश में कुछ और बताने को रहा ही नहीं। सनसनी और सिर्फ सनसनी! गंभीर विषयों पर कभी कोई चर्चा नहीं। देश के प्रति, समाज के प्रति कभी कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं। समाज के वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति कोई मानवीय संवेदना नहीं। ऐसा दायित्वविहीन मीडिया भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे बन पाएगा? यह हम सबके लिए विचारणीय होना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि जब कभी किसी चैनल ने सकारात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है, कोई गंभीर प्रश्न सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है तो उसके बहुत सुखद परिणाम निकले हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब ‘जेसिका लाल केस’ में सभी आरोपी बरी कर दिए गए थे तो एक चैनल ने इस केस के विरुद्ध अभियान चलाया था और फिर दोषियों को उच्च न्यायालय से सजा मिली थी। यदि इतने सारे टी.वी. चैनल देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य एवं दायित्व समझकर एक-एक समस्या पर गंभीर चर्चाएँ आयोजित करें, सरकार एवं आमजन के बीच संवाद का सार्थक माध्यम बनें तो समाज का कायाकल्प हो सकता है। सिर्फ बेकार के विषयों पर ऐसी बहसें कराना, जहाँ बात गाली-गलौज और मारपीट तक पहुँच जाए, तो उससे देश और युवा पीढ़ी को क्या हासिल होगा?
(लक्ष्मी शंकर वाजपेयी) |
मई |