RNI NO - 62112/95
ISSN - 2455-1171
महामारी में चुनाव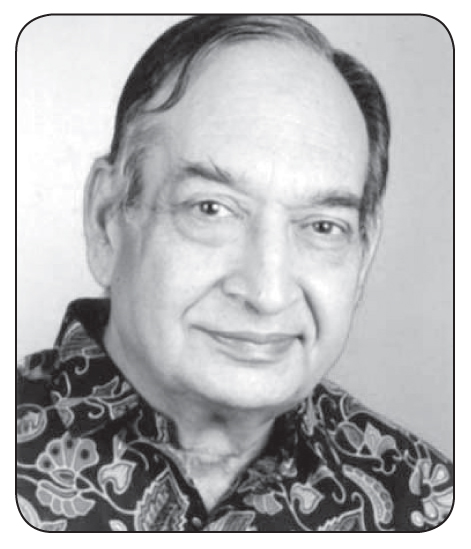
अपनी-अपनी अनिवार्यता है। प्रसिद्ध विद्वान् पी. लाल का मानना है, कि गतिशील और जीवंत प्रजातंत्र में चुनाव होने ही होने वरना महामारी के दौरान चुनाव करवाने को सोचता ही कौन? वह भी तब, जबकि सब जानते हैं कि इस लाइलाज महामारी में बिना मास्क और उचित दूरी के संक्रमण होने की सर्वाधिक संभावना है? तभी तो देश के नेता भीड़ जुटाने की स्वयं की क्षमता को अपनी ‘शान’ समझते हैं? यों इनमें एक समान गुण हैं, जो इन्हें नेतृत्व के देवत्व से जमीनी इनसान के समकक्ष बनाता है। यह सब बेहद बड़बोले हैं। इन्हें पाँच सौ की भीड़ कभी पाँच हजार की लगती है, कभी पचास हजार की। पी. लाल के अनुसार इस बड़बोलेपन ने देश को बचाया है। नहीं तो चुनावी संक्रमण इतना व्यापक होता कि महामारी अब तक पता नहीं कितनी जनसंख्या को चपेट में ले चुकी होती? पी. कुमार का मत है कि ‘महामारी का मानसिक प्रभाव, शारीरिक से कहीं अधिक है। तभी तो जाने-माने शास्त्रीय गायक जब ‘ओम’ का आलाप लगाते हैं तो उनके मुँह से ऑक्सीजन निकलता है। जब अयोध्या में कोई भक्त जय सियाराम का उद्घोष करता है तो कुछ-कुछ ‘रैमडेसिविर’ का स्वर सुनाई पड़ता है।’ हम पी. लाल की राय से अधिकतर सहमत हैं। सिर्फ हमारा विचार है कि यदि चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिए गए होते तो बेहतर रहता। हमारी प्रजातांत्रिक प्रतिबद्धता से पूरा विश्व परिचित है। महामारी के महाकाल में चुनाव करवाना कौन देश की ऐसी प्राथमिकता थी कि इसके बगैर गुजारा नहीं होता या मुल्क की नाक कट जाती? जब चुनाव की पराजय से नेता की नाक सही सलामत है तो उनके न होने से देश की नाक को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे पी. लाल मानें न मानें, हमें कभी कभी गंभीर संदेह होता है कि हमारे नेताओं की नाक शरीर का स्थाई अंग न होकर, निकाली-लगाई, जा सकती हैं। अन्यथा तो अबतक वह इतनी कट-छँट गई होती कि उसके दो छिद्रों के अलावा शायद ही कोई अन्य अवशेष बचता! संभव है कि ऐसे महानुभाव नासिकाओं का कोई भंडार घर पर रखते हैं और वक्त-जरूरत घिसी-पिटी नाक को नई से बदल लेते हैं। तभी तो वह दावा करने में समर्थ हैं कि चुनावी जीत-हार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में उनका वक्तव्य भी है, ‘प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में यही तो फायदा है कि एकतंत्र से उलट, जनतंत्र में जीत-हार लगी रहती है। जनता सत्ता से नाखुश हुई तो विरोधियों को अवसर देने से क्यों चूके? इसीलिए जनतंत्र हमेशा जनमत के सहारे है।’ कुछ नेता चुनावी मौकों पर जनता को जनार्दन निरूपित करने से भी बाज नहीं आते हैं। यह उनकी विनम्र स्वीकारोक्ति है। इन्होंने इसी जनता को चुनाव के पहले ‘कचरा’ माना है। घर के सामने यही उस के दर्शनार्थ आते तो वह कभी मीटिंग में व्यस्त रहते, कभी पद की जुगाड़ में। अब इन्हीं नेताओं को इसी कचरे में कन्हैया नजर आते हैं। अब वह दर्शन देते नहीं, दर्शन करने पैदल निकलते हैं। लोकतंत्र की यही खूबी है। इसके चलते कब कोई बिना सीढ़ी अहम के आसमान पर चढ़े, कब जमीन पर टपके, कहना कठिन क्या, असंभव है। राजनेता शायद संसार का सबसे आशावादी व्यक्ति है। वह अभी हाल ही में हारा है और आज फिर से अपने हवाई किले बनाने में लग गया है। कैसे और क्या किया जाए कि जीते नेता की छवि धूमिल हो? कैसे जनता का विश्वास उस पर से हटे? कौन सा दुष्प्रचार का उसकी छवि पर असर होगा? कैसे सिद्ध किया जाए कि वह न व्यवहार से प्रजातांत्रिक है न अपने सोच से? हार के बाद पहले सप्ताह से पराजित दल इस जुगाड़ में भिड़ता है कि विजयी पार्टी को कैसे पछाड़ा जाए? क्या राज्य में हालात इतने बदतर हैं कि राष्ट्रपति शासन की कोई गुंजाइश है? कैसे हालिया विजय को पराजय में तब्दील किया जाए? ऐसे नेता भूलता है कि चुनाव के तत्काल बाद इस प्रकार के प्रयास व्यावहारिक नहीं हैं। जाने क्यों, चुनाव के समय उसके दल ने ऐसा माहौल बनाया था कि विजय उनके ही दल की होगी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक ने, वहाँ प्रचार करने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। सबने मिल-जुलकर स्वयं को आश्वस्त कर लिया कि जीत तो उनकी ही होनी है। दुर्भाग्य से जनता ने अपने वोट से उनका सारा आत्मविश्वास ध्वस्त कर दिया। अब परिवर्तन के लिए पूरे पाँच वर्ष का समय है। तब तक न जाने कितने राज्यों मे चुनाव हों और केंद्र में भी। क्या सत्ता दल को चिंता है कि इस पराजय का उसके भविष्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा? कहीं राज्य का यह नेता इतना महत्त्वपूर्ण बनकर न उभरे कि विपक्ष के नेतृत्व की कमान कहीं वह ही न सँभाल ले? मुमकिन है कि वह इस आकलन से राज्य के नेतृत्व के पंख वह अभी से काटने की कोशिश में लग गए हैं? किसी भी सत्तादल के लिए विपक्षी एकता एक खतरनाक संभावना है, विशेषकर, महामारी की परिस्थिति में जब शासक दल से जनता कोई खास प्रसन्न नहीं है, उलटे नाराज है। क्या यह महामारी की दूसरी और घातक लहर आने के पूर्व दवा या जरूरी ऑक्सीजन की उपलब्धि की योजना नहीं बना सकते थे? क्या तब अपनी पीठ ठोकना इतना महत्त्वपूर्ण था कि यह यही करते रहे और संसार भर को उपलब्ध संसाधन सप्लाई कर वाहवाही लूटते रहे? पी. लाल का कहना है कि इसमें ऐसे महानुभावों को क्या दोष देना? यह केवल इनसानी प्रवृत्ति है। हाँ, इससे इतना जरूर साबित होता है कि यह टैगोर या महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष नहीं हैं। इन्हें अपनी महानता का आभास ही नहीं है, वह इसे दूसरों पर लादने से भी नहीं हिचकते हैं। कौन कहे, गांधी-टैगोर को भी यह अहसास रहा होगा पर उन्होंने हमेशा एक सामान्य इनसान के समान व्यवहार किया। क्या पता, उनके व्यक्तित्व को यही महान बनाता है। यों उनका कृतित्व भी उनकी महानता का साक्षी है। पूरा देश उनकी महानता से परिचित है। उसे जताने की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है। विद्वान् जन्मजात शंकालु होते हैं महामारी को लेकर कुछ विद्वान् अपनी विचारधारा व व्यक्तिगत निष्ठा के कारण अधिक ही शंकालु हो गए हैं। फिलहाल वह इस विषय पर लेख आदि नहीं लिख रहे हैं, पर अपने मौखिक प्रचार में लगे हैं। शिष्यों को समझा रहे हैं कि महामारी-काल में चुनाव कोई दुघर्टना नहीं है, न यह प्रजातंत्र के प्रति अतिशय लगाव का द्योतक है। उलटे, यह जान-बूझकर उठाया गया, एक सोचा-विचार कदम है। रैली, भाषण, मीटिंग आदि होंगी। इसमें कितने ऐसे होंगे जो मॉस्क पहनेंगे या एक-दूसरे से समुचित दूरी बनाएँगे? संक्रमण फैलाने का यह सबसे बड़ा अवसर होगा। संक्रमण के पश्चात दो ही विकल्प संभव है, या तो व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाएँ मिलें या वह चल बसे। महामारी के दौरान ऑक्सीजन व दवाओं का अभाव एक ऐसा तथ्य है, जो जगजाहिर है। महामारी-निरोधक, एक साधन, सब का वैक्सीनेशन है। इधर तो उसका भी अभाव महसूस हो रहा है। लोग जाते हैं, कतारों में लगते हैं और टीका न उपलब्ध होने से लौट जाते हैं। संक्रमण की संभावना और बढ़ जाती है। शंकालु विद्वानों का निष्कर्ष है कि कहीं यह सब शासकीय हरकतें जनसंख्या-नियंत्रण का माध्यम तो नहीं है? सरकारी इरादों को भाँप पाना कोई आसान है क्या? लाशों पर जीमना गिद्धों का स्वभाव है, चीलें यों ही मँडराती हैं, कौए काँव-काँव की कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके मन में क्या है सब जानते हैं। पर इंसानी गिरगिट कब रंग बदल ले किसे पता है? ऐसे निर्णय अधिकतर लिखित नहीं होते हैं। कौन फाइल पर यह तथ्य दर्ज कर अपनी खुद की फाँसी का फंदा तैयार करेगा? इससे शंकालु बुद्धिजीवी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उसने एक तो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार में ऐसे काम के निर्णय फाइलों पर नहीं लिये जाते हैं। लिहाजा, इस विषय में साक्ष्य खोजना संभव नहीं हैं। ऐसी घातक हरकतें किस कोड या इशारे से संपन्न होती हैं, इससें शंकालु ज्ञानी भी अपरिचित है। बस उसने अपनी ‘शंका’ जता दी, वह भी शिष्यों से। उन्होंने इसे प्रचारित कर दिया तो इसमें उसका क्या कुसूर? यदि इस विषय में उसे अपने विचार व्यक्त करने होते तो वह लेख लिखना या टी.वी. की तमाम चर्चाओं में भाग लेता। सच्चाई तो यह है कि वह सोचने में भी असमर्थ है कि जनता की चुनी हुई सरकार ऐसी जन-विरोधी इरादे रख सकती है? शंकालु विद्वान् ने यह भी साफ कर दिया कि उसने सरकार पर घटिया आरोप नहीं लगाए हैं। सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार में उसकी भूमिका कतई नहीं है। बुद्धिजीवी पत्रकारों से ‘ऑफ दि रिकॉर्ड’ यह भी कहता है कि उसने भी चुनाव संबंधी इस तरह की अफवाहें सुनी हैं, पर यह कतई विश्वास योग्य नहीं है। दरअसल, बुद्धिजीवी चिंतित हैं। सरकार के रावण से अधिक सिर है, कौन कहे सैकडों हों? हजारों-लाखों हाथ हैं। जाने कब शंकालु विद्वान् पर देश-द्रोह की कौन सी धारा लगा दे, जेल में ठूसने के लिए। वह जेल जाने से डरता है। टॉयलेट में बिना चुना हुआ अखबार पढ़े, उसे कब्ज होने का गंभीर खतरा है। जेल के डॉक्टरों का क्या भरोसा? वह गलत इलाज ही कर दें। तब उसे कौन बचाने आएगा? फिर भी पत्रकारों को सामने पाकर वह खासा मुखर हैं। ‘देखिए, यह हमारा निजी विचार नहीं है पर इतना जरूर है कि गाँव-गाँव में चुनाव कराकर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई समझदारी का प्रदर्शन किया है? जो महामारी अभी शहरों तक सीमित थी, उसे गाँव-गाँव भेजने से फायदा क्या है? वहाँ कौन इसका निदान करेगा, बिना ऑक्सीजन और दवाओं के? वहाँ तो अस्पताल भी नहीं है। किसान अन्नदाता है। उन्होंने सिर्फ देश का पेट भरा है। यह कोई ऐसा अपराध है, जिसके लिए शासक उन्हें मृत्युदंड देने पर उतारू है? हमसे कई विचारक इस प्रकार की चर्चा करते हैं। क्या हम चुप बैठें? हम उन्हें आप तक प्रेषित कर मन का बोझ हलका कर रहे हैं। हम ऊपरवाले से मनाते हैं कि ऐसा न हो। यही आशा हमें आप से भी है। आप भी सोचिए कि इस गलत निर्णय का निराकरण कैसे हो? इसी में हमारा, आपका, अन्नदाताओं, सबका कल्याण है। हम नास्तिक हैं। फिर भी प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है।’ दुखद है कि देश में कुत्सित राजनीति ने ऐसे पाँव पसारे हैं कि उसने जन-कल्याण को भी नहीं बख्शा है। इधर जानें जा रही हैं, उधर सरकार की टाँग-खिंचाई हो रही है। क्या किसी को अनुमान तक था कि महामारी की दूसरी लहर ऐसी घातक और भयावह होगी? सोशल मीडिया पर समर्पित बुद्धिजीवियों के बिना सिर-पैर के ऐसे प्रचार से क्या प्राण-रक्षा की संभावना है? ऐसा लगता है कि ऊपरवाले ने उनसे कानाफूसी कर दूसरी लहर की सूचना दी हो। तब से उन्होंने विषेशज्ञों की कई काल्पनिक कमेटियाँ बनाकर दूसरी लहर के आक्रमण की चेतावनी दी है। सबका लक्ष्य प्रधानमंत्री का दफ्तर है जहाँ इन्हें जान-बूझकर दफन कर दिया गया? इतना ही नहीं वह यह आरोप भी लगा रहे हैं कि जब इस आपदा की आशंका थी तो दूसरों की सहायता द्वारा विश्वप्रिय बनने की क्या आवश्यकता थी? दुघर्टना के बाद सभी चौकन्ने होते हैं, विशेषकर बुद्धि के कीड़े जिन्हें बुद्धिजीवी भी कहते हैं। वह भूलते हैं कि आज संसार हमारी मदद के लिए इसी कारण आगे आया है। पिछले शासकों ने देश की स्वास्थ्य-प्रणाली के लिया क्या किया कि अब हाय-तौबा मचाने में जुटे हैं? रही-सही कसर उन चरित्रहीन इंसानी गिद्धों ने पूरी कर दी है जिन्हें हर आपदा पैसा कमाने का अवसर है। ऑक्सीजन है, दवा है पर जमाखोरों और कालाबाजारियों ने उस पर कब्जा जमा रखा है। इसी प्रवृत्ति के इनसानी शैतान अस्पतालों में भी हैं। वंशवादी वारिश की जनसेवा के नाम पर सिर्फ उपलब्धि है, उससे कायाकल्प की क्या उम्मीद है? पर किसी भी बहाने सत्ता हथियाने की कोशिशों में अनुचित क्या है? जनता समझे न समझे, वह खुद को सत्ता परिवार का पुश्तैनी आका समझता है। कुरसी की संभावना से वह भी प्रफुल्लित हैं। उनके साथी भी इसी विचार के हैं। कौन कहे, अंधे के हाथ बटेर लग ही जाए? ऐसों को महामारी और संक्रमण से क्या लेना-देना? उनके अंतर में सिर्फ सत्ता का आकर्षण है? सत्ता हथिया कर, वह राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का, एक और अध्याय, लिखने को प्रस्तुत ही नहीं, कटिबद्ध भी हैं। इतने वर्षों के सत्ताहीन समय की वसूली भी तो करनी है। |
अप्रैल 2024 |













